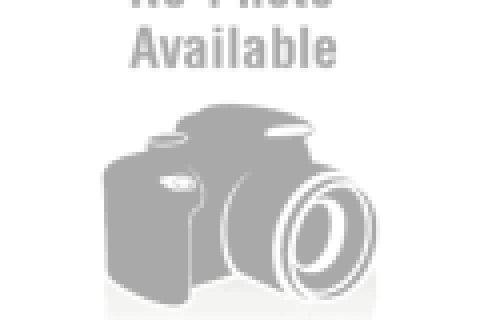परिचय
जन्म : 13 नवंबर 1917, श्योपुर, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)
भाषा : हिंदी
विधाएँ : कहानी, कविता, निबंध, आलोचना, इतिहास
मुख्य कृतियाँ
कविता संग्रह : चाँद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल
कहानी संग्रह : काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी
आलोचना : कामायनी : एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्यशास्त्र, समीक्षा की समस्याएँ, एक साहित्यिक की डायरी
इतिहास : भारत : इतिहास और संस्कृति
रचनावली : मुक्तिबोध रचनावली (छह खंड)
निधन : 11 सितंबर 1964, दिल्ली
विशेष
गजानन माधव ‘मुक्तिबोध’ (१३ नवंबर १९१७ – ११ सितंबर १९६४) आप के पिता का नाम माधवराव और माता का नाम पार्वती बाई था। पिता थानेदार रहकर उज्जैन में इन्स्पेक्टर पद से रिटायर हुए । पूजापाठ के प्रति आस्तिक विचार, निर्भीक, न्यायनिष्ठ और घोर रिश्वत-विरोधी होने के कारण जब रिटायर हुए तब खाली हाथ थे। मुक्तिबोध की प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई। 1938 में बी० ए० पास करने के पश्चात आप उज्जैन के मॉर्डन स्कूल में अध्यापक हो गए । मुक्तिबोध ने 1939 में शांता जी से माता-पिता की इच्छाओं के विरूद्ध विवाह कर लिया, किंतु जल्द ही पत्नी के साथ उनका वैचारिक मतभेद हो गये । पत्नी को मुक्तिबोध के कवि-व्यक्तित्व की अपेक्षा सम्पन्नता और सुविधापूर्ण जीवन में अधिक रुचि थी ।
मुक्तिबोध तारसप्तक के पहले कवि थे। मनुष्य की अस्मिता, आत्मसंघर्ष और प्रखर राजनैतिक चेतना से समृद्ध उनकी कविता पहली बार ‘तार सप्तक’ के माध्यम से सामने आई, लेकिन उनका कोई स्वतंत्र काव्य-संग्रह उनके जीवनकाल में प्रकाशित नहीं हो पाया। मृत्यु के पहले श्रीकांत वर्मा ने उनकी केवल ‘एक साहित्यिक की डायरी’ प्रकाशित की थी, जिसका दूसरा संस्करण भारतीय ज्ञानपीठ से उनकी मृत्यु के दो महीने बाद प्रकाशित हुआ। ज्ञानपीठ ने ही ‘चाँद का मुँह टेढ़ा है’ प्रकाशित किया था। इसी वर्ष नवंबर १९६४ में नागपुर के विश्वभारती प्रकाशन ने मुक्तिबोध द्वारा १९६३ में ही तैयार कर दिये गये निबंधों के संकलन नयी कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध’ को प्रकाशित किया था। परवर्ती वर्षो में भारतीय ज्ञानपीठ से मुक्तिबोध के अन्य संकलन ‘काठ का सपना’, तथा ‘विपात्र’ (लघु उपन्यास) प्रकाशित हुए। पहले कविता संकलन के १५ वर्ष बाद, १९८० में उनकी कविताओं का दूसरा संकलन ‘भूरी भूर खाक धूल’ प्रकाशित हुआ और १९८५ में ‘राजकमल’ से पेपरबैक में छ: खंडों में ‘मुक्तिबोध रचनावली’ प्रकाशित हुई,
इसके बाद मुक्तिबोध पर शोध और किताबों की भी झड़ी लग गयी। १९७५ में प्रकाशित अशोक चक्रधर का शोध ग्रंथ ‘मुक्तिबोध की काव्यप्रक्रिया’ इन पुस्तकों में प्रमुख था। उन्हें उम्र जरूर कम मिली, पर कविता, कहानी और आलोचना में उन्होंने युग बदल देनेवाला काम किया। प्रस्तुत हैं कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ और चर्चित कविता”अँधेरे में” [ लम्बी कविता] सहित अन्य रचनाएँ
रचनाएँ
पक्षी और दीमक – कहानी
बाहर चिलचिलाती हुई दोपहर है लेकिन इस कमरे में ठंडा मद्धिम उजाला है। यह उजाला इस बंद खिड़की की दरारों से आता है। यह एक चौड़ी मुँडेरवाली बड़ी खिड़की है, जिसके बाहर की तरफ, दीवार से लग कर, काँटेदार बेंत की हरी-घनी झाड़ियाँ हैं। इनके ऊपर एक जंगली बेल चढ़ कर फैल गई है और उसने आसमानी रंग के गिलास जैसे अपने फूल प्रदर्शित कर रखे हैं। दूर से देखने वालों को लगेगा कि वे उस बेल के फूल नहीं, वरन बेंत की झाड़ियों के अपने फूल हैं।
किंतु इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि उस लता ने अपनी घुमावदार चाल से न केवल बेंत की डालों को, उनके काँटों से बचते हुए, जकड़ रखा है, वरन उसके कंटक-रोमोंवाले पत्तों के एक-एक हरे फीते को समेट कर, कस कर, उनकी एक रस्सी-सी बना डाली है; और उस पूरी झाड़ी पर अपने फूल बिखराते-छिटकाते हुए, उन सौंदर्य-प्रतीकों को सूरज और चाँद के सामने कर दिया है।
लेकिन, इस खिड़की को मुझे अकसर बंद रखना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के इस इलाके में, मौसम-बेमौसम आँधीनुमा हवाएँ चलती हैं। उन्होंने मेरी खिड़की के बंद पल्लों को ढीला कर डाला है। खिड़की बंद रखने का एक कारण यह भी है कि बाहर दीवार से लग कर खड़ी हुई हरी-घनी झाड़ियों के भीतर जो छिपे हुए, गहरे, हरे-साँवले अंतराल हैं, उनमें पक्षी रहते हैं और अंडे देते हैं। वहाँ से कभी-कभी उनकी आवाजें, रात-बिरात, एकाएक सुनाई देती हैं। वे तीव्र भय की रोमांचक चीत्कारें हैं क्योंकि वहाँ अपने शिकार की खोज में एक भुजंग आता रहता है। वह, शायद उन तरफ की तमाम झाड़ियों के भीतर रेंगता फिरता है।
एक रात, इसी खिड़की में से एक भुजंग मेरे कमरे में भी आया। वह लगभग तीन-फीट लंबा अजगर था। खूब खा-पी कर के, सुस्त हो कर, वह खिड़की के पास, मेरी साइकिल पर लेटा हुआ था। उसका मुँह ‘कैरियर’ पर, जिस्म की लपेट में, छिपा हुआ था और पूँछ चमकदार ‘हैंडिल’ से लिपटी हुई थी। ‘कैरियर’ से ले कर ‘हैंडिल’ तक की सारी लंबाई को उसने अपने देह-वलयों से कस लिया था। उसकी वह काली-लंबी-चिकनी देह आतंक उत्पन्न करती थी।
हमने बड़ी मुश्किल से उसके मुँह को शिनाख्त किया। और फिर एकाएक ‘फिनाइल’ से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर डाला। रोमांचपूर्ण थे हमारे वे व्याकुल आक्रमण! गहरे भय की सनसनी में अपनी कायरता का बोध करते हुए, हम लोग, निर्दयतापूर्वक, उसकी छटपटाती देह को लाठियों से मारे जा रहे थे।
उसे मरा हुआ जान, हम उसका अग्नि-संस्कार करने गए। मिट्टी के तेल की पीली-गेरूई ऊँची लपक उठाते हुए, कंडों की आग में पड़ा हुआ वह ढीला नाग-शरीर, अपनी बची-खुची चेतना समेट कर, इतनी जोर-से ऊपर उछला कि घेरा डाल कर खड़े हुए हम लोग हैरत में आ कर, एक कदम पीछे हट गए। उसके बाद रात-भर, साँप की ही चर्चा होती रही।
इसी खिड़की से लगभग छह गज दूर, बेंत की झाड़ियों के उस पार, एक तालाब है… बड़ा भारी तालाब, आसमान का लंबा-चौड़ा आईना, जो थरथराते हुए मुस्कराता है। और उसकी थरथराहट पर किरनें नाचती रहती हैं।
मेरे कमरे में जो प्रकाश आता है, वह इन लहरों पर नाचती हुई किरनों का उछल कर आया हुआ प्रकाश है। खिड़की की लंबी दरारों में से गुजर कर वह प्रकाश, सामने की दीवार पर चौड़ी मुँडेर के नीचे सुंदर झलमलाती हुई आकृतियाँ बनाता है।
मेरी दृष्टि उस प्रकाश-कंप की ओर लगी हुई है। एक क्षण में उसकी अनगिनत लहरें नाचे जा रही हैं, नाचे जा रही हैं। कितना उद्दाम, कितना तीव्र वेग है उन झिलमिलाती लहरों में। मैं मुग्ध हूँ कि बाहर के लहराते तालाब ने किरनों की सहायता से अपने कंपों की प्रतिच्छवि मेरी दीवार पर आँक दी है।
काश, ऐसी भी कोई मशीन होती जो दूसरों के हृदयकंपनों को, उनकी मानसिक हलचलों को, मेरे मन के परदे पर चित्र रूप में उपस्थित कर सकती।
उदाहरणत: मेरे सामने इसी पलंग पर, वह जो नारी-मूर्ति बैठी है, उसके व्यक्तित्व के रहस्य को मैं जानना चाहता हूँ, वैसे, उसके बारे में जितनी गहरी जानकारी मुझे है, शायद और किसी को नहीं।
इस धुँधले अँधेरे कमरे में वह मुझे सुंदर दिखाई दे रही है। दीवार पर गिरे हुए प्रत्यावर्तित प्रकाश का पुन: प्रत्यावर्तित प्रकाश, नीली चूडियोंवाले हाथों में थमे हुए उपन्यास के पन्नों पर, ध्यानमग्न कपोलों पर और आसमानी आँचल पर फैला हुआ है। यद्यपि इस समय हम दोनों अलग-अलग दुनिया में (वह उपन्यास के जगत में और मैं अपने खयालों के रास्तों पर) घूम रहे हैं, फिर भी इस अकेले धुँधुले कमरे में गहन साहचर्य के संबंध-सूत्र तड़प रहे हैं और महसूस किए जा रहे हैं।
बावजूद इसके, यह कहना ही होगा कि मुझे इसमें ‘रोमांस’ नहीं दीखता। मेरे सिर का दाहिना हिस्सा सफेद हो चुका है। अब तो मैं केवल आश्रय का अभिलाषी हूँ, ऊष्मापूर्ण आश्रय का…
फिर भी मुझे शंका है। यौवन के मोह-स्वप्न उद्दाम आत्मविश्वास अब मुझमें नहीं हो सकता। एक वयस्क पुरुष का अविवाहिता वयस्का स्त्री से प्रेम भी अजीब होता है। उसमें उद्बुद्ध इच्छा के आग्रह के सा्थ-साथ जो अनुभवपूर्ण ज्ञान का प्रकाश होता है, वह पल-पल पर शंका और संदेह को उत्पन्न करता है।
श्यामला के बारे में मुझे शंका रहती है। वह ठोस बातों की बारीकियों का बड़ा आदर करती है। वह व्यवहार की कसौटी पर मनुष्य को परखती है। वह मुझे अखरता है। उसमें मुझे एक ठंडा पथरीलापन मालूम होता है। गीले-सपनीले रंगों का श्यामला में सचमुच अभाव है।
ठंडा पथरीलापन उचित है, या अनुचित, यह मैं नहीं जानता। किंतु जब औचित्य के सारे प्रमाण, उनका सारा वस्तु-सत्य पॉलिशदार टीन-सा चमचमा उठता है, तो मुझे लगता है – बुरे फँसे इन फालतू की अच्छाइयों में, दूसरी तरफ मुझे अपने भीतर ही कोई गहरी कमी महसूस होती है और खटकने लगती है।
ऐसी स्थिति में मैं ‘हाँ’ और ‘ना’ के बीच में रह कर, खामोश, ‘जी हाँ’ की सूरत पैदा कर देता हूँ। डरता सिर्फ इस बात से हूँ कि कहीं यह ‘जी हाँ’ ‘जी हुजूर’ न बन जाए। मैं अतिशय शांति-प्रिय व्यक्ति हूँ। अपनी शांति भंग न हो, इसका बहुत खयाल रखता हूँ। न झगड़ा करना चाहता हूँ, न मैं किसी झगड़े में फँसना चाहता…
उपन्यास फेंक कर श्यामला ने दोनों हाथ ऊँचे करके जरा-सी अँगड़ाई ली। मैं उसकी रूप-मुद्रा पर फिर से मुग्ध होना ही चाहता था कि उसने एक बेतुका प्रस्ताव सामने रख दिया। कहने लगी, ‘चलो, बाहर घूमने चलें।’
मेरी आँखों के सामने बाहर की चिलचिलाती सफेदी और भयानक गरमी चमक उठी। खस के परदों के पीछे, छत के पंखों के नीचे, अलसाते लोग याद आए। भद्रता की कल्पना और सुविधा के भाव मुझे मना करने लगे। श्यामला के झक्कीपन का एक प्रमाण और मिला।
उसने मुझे एक क्षण आँखों से तौला और फैसले के ढंग से कहा, ‘खैर, मैं तो जाती हूँ। देख कर चली जाऊँगी… बता दूँगी।’
लेकिन चंद मिनटों बाद, मैंने अपने को चुपचाप उसके पीछे चलते हुए पाया। तब दिल में एक अजीब झोल महसूस हो रहा था। दिमाग के भीतर सिकुड़न-सी पड़ गई थी। पतलून भी ढीला-ढाला लग रहा था, कमीज के ‘कॉलर’ भी उल्टे-सीधे रहें होंगे। बाल अन-सँवरे थे ही। पैरों को किसी-न-किसी तरह आगे ढकेले जा रहा था।
लेकिन यह सिर्फ दुपहर के गरम तीरों के कारण था, या श्यामला के कारण, यह कहना मुश्किल है।
उसने पीछे मुड़ कर मेरी तरफ देखा और दिलासा देती हुई आवाज में कहा, ‘स्कूल का मैदान ज्यादा दूर नहीं है।’
वह मेरे आगे-आगे चल रही थी, लेकिन मेरा ध्यान उसके पैरों और तलुओं के पिछले हिस्से की तरफ ही था। उसकी टाँग, जो बिवाइयों-भरी और धूल-भरी थी, आगे बढ़ने में, उचकती हुई चप्पल पर चटचटाती थी। जाहिर था कि ये पैर धूल-भरी सड़कों पर घूमने के आदी हैं।
यह खयाल आते ही, उसी खयाल से लगे हुए न मालूम किन धागों से हो कर, मैं श्यामला से खुद को कुछ कम, कुछ हीन पाने लगा; और इसकी ग्लानि से उबरने के लिए, मैं उस चलती हुई आकृति के साथ, उसके बराबर हो लिया। वह कहने लगी, ‘याद है शाम को बैठक है। अभी चल कर न देखते तो कब देखते। और सबके सामने साबित हो जाता कि तुम खुद कुछ करते नहीं। सिर्फ जबान की कैंची चलती है।’
अब श्यामला को कौन बताए कि न मैं इस भरी दोपहर में स्कूल का मैदान देखने जाता और न शाम को बैठक में ही। संभव था कि ‘कोरम’ पूरा न होने के कारण बैठक ही स्थगित हो जाती। लेकिन श्यामला को यह कौन बताए कि हमारे आलस्य में भी एक छिपी हुई, जानी-अनजानी योजना रहती है। वर्तमान सुचालन का दायित्व जिन पर है, वे खुद संचालन-मंडल की बैठक नहीं होने देना चाहते। अगर श्यामला से कहूँ तो पूछेगी, ‘क्यों!’
फिर मैं जवाब दूँगा। मैं उसकी आँखों से गिरना नहीं चाहता, उसकी नजर में और-और चढ़ना चाहता हूँ। प्रेमी जो हूँ; अपने व्यक्तित्व का सुंदरतम चित्र उपस्थित करने की लालसा भी तो रहती है।
वैसे भी, धूप इतनी तेज थी कि बात करने या बात बढ़ाने की तबीयत नहीं हो रही थी।
मेरी आँखें सामने के पीपल के पेड़ की तरफ गईं, जिसकी एक डाल तालाब के ऊपर, बहुत ऊँचाई पर, दूर तक चली गई थी। उसके सिरे पर एक बड़ा-सा भूरा पक्षी बैठा हुआ था। उसे मैंने चील समझा। लगता था कि वह मछलियों के शिकार की ताक लगाए बैठा है।
लेकिन उसी शाखा की बिलकुल विरुद्ध दिशा में, जो दूसरी डालें ऊँची हो कर तिरछी और बाँकी-टेढ़ी हो गई हैं, उन पर झुंड के झुंड कौवे काँव-काँव कर रहे हैं, मानो वे चील की शिकायत कर रहे हों और उचक-उचक कर, फुदक-फुदक कर, मछली की ताक में बैठे उस पक्षी के विरुद्ध प्रचार किए जा रहे हों कि इतने में मुझे उस मैदानी-आसमानी चमकीले खुले-खुलेपन में एकाएक, सामने दिखाई देता है – साँवले नाटे कद पर भगवे रंग की खद्दर का बंडीनुमा कुरता, लगभग चौरस मोटा चेहरा, जिसके दाहिने गाल पर एक बड़ा-सा मसा है, और उस मसे में बारीक बाल निकले हुए।
जी धँस जाता है उस सूरत को देख कर। वह मेरा नेता है, संस्था का सर्वेसर्वा है। उसकी खयाली तस्वीर देखते ही मुझे अचानक दूसरे नेताओं की और सचिवालय के उस अँधेरे गलियारे की याद आती है, जहाँ मैंने इस नाटे-मोटे भगवे खद्दर-कुरतेवाले को पहले-पहले देखा था।
उन अँधेरे गलियारों में से मैं कई-कई बार गुजरा हुँ और वहाँ किसी मोड़ पर किसी कोने में इकट्ठा हुए, ऐसी ही संस्थाओं के संचालकों के उतरे हुए चेहरों को देखा है। बावजूद श्रेष्ठ पोशाक और ‘अपटूडेट’ भेस के सँवलाया हुआ गर्व, बेबस गंभीरता, अधीर उदासी और थकान उनके व्यक्तित्व पर राख-सी मलती है। क्यों?
इसलिए कि माली साल की आखिरी तारीख को अब सिर्फ दो या तीन दिन बचे हैं। सरकारी ‘ग्रांट’ अभी मंजूर नहीं हो पा रही है, कागजात अभी वित्त-विभाग में ही अटके पड़े हैं। आफिसों के बाहर, गलियारे के दूर किसी कोने में, पेशाबघर के पास, या होटलों के कोनों में क्लर्कों की मुट्ठियाँ गरम की जा रहीं हैं, ताकि ‘ग्रांट’ मंजूर हो और जल्दी मिल जाए।
ऐसी ही किसी जगह पर मैंने इस भगवे-खद्दर कुरतेवाले को जोर-जोर से अंगरेजी बोलते हुए देखा था। और, तभी मैंने उसके तेज मिजाज और फितरती दिमाग का अंदाजा लगाया था।
इधर, भरी दोपहर में श्यामला का पार्श्व-संगीत चल ही रहा है, मैं उसका कोई मतलब नहीं निकाल पाता। लेकिन न मालूम कैसे, मेरा मन उसकी बातों से कुछ संकेत ग्रहण कर, अपने ही रास्ते पर चलता रहता है। इसी बीच उसके एक वाक्य से मैं चौंक पड़ा, ‘इससे अच्छा है कि तुम इस्तीफा दे दो। अगर काम नहीं कर सकते तो गद्दी क्यों अड़ा रखी है।’
इसी बात को कई बार मैंने अपने से भी पूछा था। लेकिन आज उसके मुँह से ठीक उसी बात को सुन कर मुझे धक्का-सा लगा। और मेरा मन कहाँ का कहाँ चला गया।
एक दिन की बात! मेरा सजा हुआ कमरा! चाय की चुस्कियाँ! कहकहे! एक पीले रंग के तिकोने चेहरेवाला मसखरा, ऊलजलूल शख्स! बगैर यह सोचे कि जिसकी वह निंदा कर रहा है, वह मेरा कृपालु मित्र और सहायक है, वह शख्स बात बढ़ाता जा रहा है।
मैं स्तब्ध! किंतु, कान सुन रहे हैं। हारे हुए आदमी-जैसी मेरी सूरत, और मैं!
वह कहता जा रहा है, ‘सूक्ष्मदर्शी यंत्र? सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहाँ हैं?’
‘हैं तो। ये हैं। देखिए।’ क्लर्क कहता है। रजिस्टर बताता है। सब कहते हैं-हैं, हैं। ये हैं। लेकिन, कहाँ हैं? यह तो सब लिखित रूप में हैं, वस्तु-रूप में कहाँ हैं।
वे खरीदे ही नहीं गए! झूठी रसीद लिखने का कमीशन विक्रेता को, शेष रकम जेब में। सरकार से पूरी रकम वसूल!
किसी खास जाँच के एन मौके पर किसी दूसरे शहर की…संस्था से उधार ले कर, सूक्ष्मदर्शी यंत्र हाजिर! सब चीजें मौजूद हैं। आइए, देख जाइए। जी हाँ, ये तो हैं सामने। लेकिन जांच खत्म होने पर सब गायब, सब अंतर्धान। कैसा जादू है। खर्चे का आँकडा खूब फुला कर रखिए। सरकार के पास कागजात भेज दीजिए। खास मौकों पर ऑफिसों के धुँधले गलियारों और होटलों के कोनों में मुट्ठियाँ गरम कीजिए। सरकारी ‘ग्रांट’ मंजूर! और उसका न जाने कितना हिस्सा, बड़े ही तरीके से, संचालकों की जेब में! जी!’
भरी दोपहर में मैं आगे बढ़ा जा रहा हूँ। कानों में ये आवाजों गूँजती जा रही हैं। मैं व्याकुल हो उठता हूँ। श्यामला का पार्श्व-संगीत चल रहा है। मुझे जबरदस्त प्यास लगती है! पानी, पानी!
-कि इतने में एकाकए विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की ऊँचे रोमन स्तंभोंवाली इमारत सामने आ जाती है। तीसरा पहर! हलकी धूप! इमारत की पत्थर-सीढ़ियाँ, लंबी, मोतिया!
सीढ़ियों से लग कर, अभरक-मिली लाल मिट्टी के चमचमाते रास्ते पर सुंदर काली ‘शेवरलेट’।
भगवे खद्दर-कुरते वाले की ‘शेवरलेट’, जिसके जरा पीछे मैं खड़ा हूँ, और देख रहा हूँ – यों ही, कार का नंबर – कि इतने में उसके चिकने काले हिस्से में, जो आईने-सा चमकदार है, सूरत दिखाई देती है।
भयानक है वह सूरत! सारे अनुपात बिगड़ गए हैं। नाक डेढ़ गज लंबी और कितनी मोटी हो गई है। चेहरा बेहद लंबा और सिकुड़ गया है। आँखें खड्डेदार। कान नदारद। भूत-जैसा अप्राकृतिक रूप। मैं अपने चेहरे की उस विद्रूपता को, मुग्धभाव से, कुतूहल से और आश्चर्य से देख रहा हूँ, एकटक।
कि इतने में मैं दो कदम एक ओर हट जाता हूँ; और पाता हूँ कि मोटर के उस काले चमकदार आईने में मेरे गाल, ठुड्डी, नाम, कान सब चौड़े हो गए हैं, एकदम चौड़े। लंबाई लगभग नदारद। मैं देखता ही रहता हूँ, देखता ही रहता हूँ कि इतने में दिल के किसी कोने में कई अँधियारी गटर एकदम फूट निकलती है। वह गटर है आत्मालोचन, दु:ख और ग्लानि की।
और, सहसा मुँह से हाय निकल पड़ती है। उस भगवे खद्दर-कुरते वाले से मेरा छुटकारा कब होगा, कब होगा।
और, तब लगता है कि इस सारे जाल में, बुराई की इस अनेक चक्रोंवाली दैत्याकार मशीन में, न जाने कब से मैं फँसा पड़ा हूँ। पैर भिंच गए हैं, पसलियाँ चूर हो गई हैं, चीख निकल नहीं पाती, आवाज हलक में फँस कर रह गई है।
कि इसी बीच अचानक एक नजारा दिखाई देता है। रोमन स्तंभोंवाली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की ऊँची, लंबी, मोतिया सीढ़ियों पर से उतर रही है एक आत्म-विश्वासपूर्ण गौरवमय नारीमूर्ति।
वह किरणीली मुस्कान मेरी ओर फेंकती-सी दिखाई देती है। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि उसका स्वागत कर सकूँ। मैं बदहवास हो उठता हूँ।
वह धीमे-धीमे मेरे पास आती है। अभ्यर्थनापूर्ण मुस्काराहट के साथ कहती है, ‘पढ़ी है आपने यह पुस्तक।’
काली जिल्द पर सुनहले रोमन अक्षरों में लिखा है, ‘आई विल नाट रेस्ट।’
मैं साफ झूठ बोल जाता हूँ, ‘हाँ पढ़ी है, बहुत पहले।’
लेकिन मुझे महसूस होता है कि मेरे चेहरे पर से तेलिया पसीना निकल रहा है। मैं बार-बार अपना मुँह पोंछता हूँ रूमाल से। बालों के नीचे ललाट-हाँ, ललाट, (यह शब्द मुझे अच्छा लगता है) को रगड़ कर साफ करता हूँ।
और, फिर दूर एक पेड़ के नीचे, इधर आते हुए, भगवे खद्दर-कुरतेवाले की आकृति को देख कर श्यामला से कहता हूँ, ‘अच्छा, मै जरा उधर जा रहा हूँ। फिर भेंट होगी।’ और सभ्यता के तकाजे से मैं उसके लिए नमस्कार के रूप में मुस्कराने की चेष्टा करता हूँ।
पेड़।
अजीब पेड़ है, (यहाँ रूका जा सकता है), बहुत पुराना पेड़ है, जिसकी जड़ें उखड़ कर बीच में से टूट गई हैं और साबित है, उनके आस-पास की मिट्टी खिसक गई है। इसलिए वे उभर कर ऐंठी हुई-सी लगती हैं। पेड़ क्या है, लगभग ठूँठ है। उसकी शाखाएँ काट डाली गई हैं।
लेकिन, कटी हुई बाँहोंवाले उस पेड़ में से नई डालें निकल कर हवा में खेल रही हैं! उन डालों में कोमल-कोमल हरी-हरी पत्तियाँ झालर-सी दिखाई देती हैं। पेड़ के मोटे तने में से जगह-जगह ताजा गोंद निकल रहा है। गोंद की साँवली कत्थई गठानें मजे में देखी जा सकती हैं।
अजीब पेड़ है, अजीब! (शायद, यह अच्छाई का पेड़ है) इसलिए कि एक दिन शाम की मोतिया-गुलाबी आभा में मैंने एक युवक-युवती को इस पेड़ के तले ऊँची उठी हुई, उभरी हुई, जड़ पर आराम से बैठे हुए पाया था। संभवत: वे अपने अत्यंत आत्मीय क्षणों में डूबे हुए थे।
मुझे देख कर युवक ने आदरपूर्वक नमस्कार किया। लड़की ने भी मुझे देखा और झेंप गई। हलके झटके से उसने अपना मुँह दूसरी ओर कर लिया। लेकिन उसकी झेंपती हुई ललाई मेरी नजरों से न बच सकी।
इस प्रेम-मुग्ध को देख कर मैं भी एक विचित्र आनंद में डूब गया। उन्हें निरापद करने के लिए जल्दी-जल्दी पैर बढाता हुआ मैं वहाँ से नौ-दो ग्यारह हो गया।
यह पिछली गर्मियों की मनोहर साँझ की बात है। लेकिन आज इस भरी दोपहरी में श्यामला के साथ पल-भर उस पेड़ के तले बैठने को मेरी भी तबीयत हुई। बहुत ही छोटी और भोली इच्छा है यह।
लेकिन मुझे लगा कि शायद श्यामला मेरे सुझाव को नहीं मानेगी। स्कूल-मैदान पहुँचने की उसे जल्दी जो है। कहने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई।
लेकिन दूसरे क्षण, आप-ही-आप, मेरे पैर उस ओर बढ़ने लगे। और ठीक उसी जगह मैं भी जा कर बैठ गया, जहाँ एक साल पहले वह युग्म बैठा था। देखता क्या हूँ कि श्यामला भी आ कर बैठ गई है।
तब वह कह रही थी, ‘सचमुच बड़ी गरम दोपहर है।’
सामने मैदान-ही-मैदान हैं, भूरे मटमैले! उन पर सिरस और सीसम के छायादार विराम-चिह्र खड़े हैं। मैं लुब्ध और मुग्ध हो कर उनकी घनी-गहरी छायाएँ देखता रहता हूँ…
क्योंकि… क्योंकि मेरा यह पेड़, यह अच्छाई का पेड़ छाया प्रदान नहीं कर सकता, आश्रय प्रदान नहीं कर सकता, (क्योंकि वह जगह-जगह काटा गया है) वह तो कटी शाखाओं की दूरियों और अंतरालों में से केवल तीव्र और कष्टप्रद प्रकाश को ही मार्ग दे सकता है।
लेकिन मैदानों के इस चिलचिलाते अपार विस्तार में एक पेड़ के नीचे, अकेलेपन में, श्यामला के साथ रहने की यह जो मेरी स्थिति है, उसका अचानक मुझे गहरा बोध हुआ। लगा कि श्यामला मेरी है, और वह भी इसी भाँति चिलमिलाते गरम तत्वों से बनी हुई नारी-मूर्ति है। गरम बफती हुई मिट्टी-सा चिलमिलाता हुआ उसमें अपनापन है।
तो क्या आज ही, अगली अनगिनत गरम दोपहरियों के पहले आज ही, अगले कदम उठाए जाने के पहले, इसी समय, हाँ, इसी समय, उसके सामने अपने दिन की गहरी छिपी हुई तहें और सतहें खोल कर रख दूँ… कि जिससे आगे चल कर उसे गलतफहमी में रखने, उसे धोखे में रखने का अपराधी न बनूँ।
कि इतने में मेरी आँखों के सामने, फिर उसी भगवे खद्दर-कुरतेवाले की तस्वीर चमक उठी। मैं व्याकुल हो गया और उससे छुटकारा चाहने लगा।
तो फिर आत्म-स्वीकार कैसे करूँ, कहाँ से शुरू करूँ!
लेकिन क्या वह मेरी बातें समझ सकेगी? किसी तनी हुई रस्सी पर वजन साधते हुए चलने का, ‘हाँ’, और ‘ना’ के बीच में रह कर जिंदगी की उलझनों में फँसने का तजुर्बा उसे कहाँ है!
हटाओ, कौन कहे।
लेकिन यह स्त्री शिक्षिता तो है! बहस भी तो करती है! बहस कर बातों का संबंध न उसके स्वार्थ से होता है, न मेरे। उस समय हम लड़ भी तो सकते हैं। और ऐसी लड़ाइयों में कोई स्वार्थ भी तो नहीं होता। सामने अपने दिल की सतहें खोल देने में न मुझे शर्म रही, न मेरे सामने उसे। लेकिन वैसा करने में तकलीफ तो होती ही है, अजीब और पेचीदा, घूमती-घुमाती तकलीफ!
और उस तकलीफ को टालने के लिए हम झूठ भी तो बोल देते हैं, सरासर झूठ, सफेद झूठ! लेकिन झूठ से सचाई और गहरी हो जाती है, अधिक महत्वपूर्ण और अधिक प्राणवान, मानो वह हमारे लिए और सारी मनुष्यता के लिए विशेष सार रखती हो। ऐसी सतह पर हम भावुक हो जाते हैं। और, यह सतह अपने सारे निजीपन में बिलकुल बेनिजी है। साथ ही, मीठी भी! हाँ, उस स्तर की अपनी विचित्र पीड़ाएँ हैं, भयानक संताप है, और इस अत्यंत आत्मीय किंतु निर्वैयक्तिक स्तर पर हम एक हो जाते हैं, और कभी-कभी ठीक उसी स्तर पर बुरी तरह लड़ भी पड़ते हैं।
श्यामला ने कहा, ‘उस मैदान को समतल करने में कितना खर्च आएगा?’
‘बारह हजार।’
‘उनका अंदाज क्या है?’
‘बीस हजार ।’
‘तो बैठक में जा कर समझा दोगे और यह बता दोगे कि कुल मिला कर बारह हजार से ज्यादा नामुमकिन है?’
‘हाँ, उतना मैं कर दूँगा।’
‘उतना का क्या मतलब?’
अब मैं उसे ‘उतना’ का क्या मतलब बताऊँ! साफ है कि उस भगवे खद्दर- कुरतेवाले से मैं दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। मैं उसके प्रति वफादार रहूँगा क्योंकि मैं उसका आदमी हूँ। भले ही वह बुरा हो, भ्रष्टाचारी हो, किंतु उसी के कारण ही मैं विश्वास-योग्य माना गया हूँ। इसीलिए, मैं कई महत्वपूर्ण कमेटियों का सदस्य हूँ।
मैंने विरोध-भाव से श्यामला की तरफ देखा। वह मेरा रुख देख कर समझ गई। वह कुछ नहीं बोली। लेकिन मानो मैंने उसकी आवाज सुन ली हो।
श्यामला का चेहरा ‘चार जनियों-जैसा’ है। उस पर साँवली मोहक दीप्ति का आकर्षण है। किंतु उसकी आवाज… हाँ… आवाज… वह इतनी सुरीली और मीठी है कि उसे अनसुना करना निहायत मुश्किल है। उस स्वर को सुन कर दुनिया की अच्छी बातें ही याद आ सकती हैं।
पता नहीं किस तरह की परेशान पेचीदगी मेरे चेहरे पर झलक उठी कि जिसे देख कर उसने कहा, ‘कहो, क्या कहना चाहते हो।’
यह वाक्य मेरे लिए निर्णायक बन गया। फिर भी अवरोध शेष था। अपने जीवन का सार-सत्य अपना गुप्त-धन है। उसके गुप्त संधर्ष हैं, उसका अपना एक गुप्त नाटक है। वह प्रकट करते नहीं बनता। फिर भी, शायद है कि उसे प्रकट कर देने ये उसका मूल्य बढ़ जाए, उसका कोई विशेष उपयोग हो सके।
एक था पक्षी। वह नीले आसमान में खूब ऊँचाई पर उड़ता जा रहा था। उसके साथ उसके पिता और मित्र भी थे।
(श्यामला मेरे चेहरे की तरफ आश्चर्य से देखते लगी)
सब बहुत ऊँचाई पर उड़नेवाले पक्षी थे। उनकी निगाहें भी बड़ी तेज थीं। उन्हें दूर दूर की भनक और दूर-दूर की महक भी मिल जाती।
एक दिन वह नौजवान पक्षी जमीन पर चलती हुई एक बैलगाड़ी को देख लेता है। उसमें बड़े-बड़े बोरे भरे हुए हैं। गाड़ीवाला चिल्ला-चिल्ला कर कहता है, ‘दो दीमकें लो, एक पंख दो।’
उस नौजवान पक्षी को दीमकों का शौक था। वैसे तो ऊँचे उड़नेवाले पक्षियों को हवा में ही बहुत-से कीड़े तैरते हुए मिल जाते, जिन्हें खा कर वे अपनी भूख थोड़ी-बहुत शांत कर लेते।
लेकिन दीमकें सिर्फ जमीन पर मिलती थीं। कभी-कभी पेड़ों पर-जमीन से तने पर चढ़ कर, ऊँची डाल तक, वे अपना मटियाला लंबा घर बना लेतीं। लेकिन वैसे कुछ ही पेड़ होते, और वे सब एक जगह न मिलते।
नौजवान पक्षी को लगा – यह बहुत बड़ी सुविधा है कि एक आदमी दीमकों को बोरों में भर कर बेच रहा है।
वह अपनी ऊँचाइयाँ छोड़ कर मँडराता हुआ नीचे उतरता है और पेड़ की एक डाल पर बैठ जाता है।
दोनों का सौदा तय हो जाता है। अपनी चोंच से एक पर को खींच कर तोड़ने में उसे तकलीफ भी होती है; लेकिन उसे वह बरदाश्त कर लेता है। मुँह में बड़े स्वाद के साथ दो दीमकें दबा कर वह पक्षी फुर्र से उड़ जाता है।
(कहते-कहते मैं थक गया शायद साँस लेने के लिए। श्यामला ने पलकें झपकाईं और कहा, ‘हूँ’)
अब उस पक्षी को गाड़ीवाले से दीमकें खरीदने और एक पर देने में बड़ी आसानी मालूम हुई। वह रोज तीसरे पहर नीचे उतरता और गाड़ीवाले को एक पंख दे कर दो दीमकें खरीद लेता।
कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उसके पिता ने देख लिया। उसने समझाने को कोशिश की कि बेटे, दीमकें हमारा स्वाभाविक आहार नहीं हैं, और उसके लिए अपने पंख तो हरगिज नहीं दिए जा सकते।
लेकिन, उस नौजवान पक्षी ने बड़े ही गर्व से अपना मुँह दूसरी ओर कर लिया। उसे जमीन पर उतर कर दीमकें खाने की चट लग गई थी। अब उसे न तो दूसरे कीड़े अच्छे लगते, न फल, न अनाज के दाने। दीमकों का शौक अब उस पर हावी हो गया था।
(श्यामला अपनी फैली हुई आँखों से मुझे देख रही थी, उसकी ऊपर उठी हुई पलकें और भौंएँ बड़ी ही सुंदर दिखाई दे रही थीं।)
लेकिन ऐसा कितने दिनों तक चलता। उसके पंखों की संख्या लगातार घटती चली गई। अब वह, ऊँचाइयों पर, अपना संतुलन साध नहीं सकता था, न बहुत समय तक पंख उसे सहारा दे सकते थे। आकाश-यात्रा के दौरान उसे जल्दी-जल्दी पहाड़ी चट्टानों गुंबदों और बुर्जो पर हाँफते हुए बैठ जाना पड़ता। उसके परिवार वाले तथा मित्र ऊँचाइयों पर तैरते हुए आगे बढ़ जाते। वह बहुत पिछड़ जाता। फिर भी दीमक खाने का उसका शौक कम नहीं हुआ। दीमकों के लिए गाड़ीवाले को वह अपने पंख तोड़-तोड़ कर देता रहा।
(श्यामला गंभीर हो कर सुन रही थी। अबकी बार उसने ‘हूँ’ भी नहीं कहा।)
फिर उसने सोचा कि आसमान में उड़ना ही फिजूल है। वह मूर्खों का काम है। उसकी हालत यह थी कि अब वह आसमान में उड़ ही नहीं सकता था, वह सिर्फ एक पेड़ से उड़ कर दूसरे पेड़ तक पहुँच पाता। धीरे-धीरे उसकी यह शक्ति भी कम होती गई। और एक समय वह आया जब वह बड़ी मुश्किल से, पेड़ की एक डाल से लगी हुई दूसरी डाल पर, चल कर, फुदक कर पहुँचता। लेकिन दीमक खाने का शौक नहीं छूटा।
बीच-बीच में गाड़ीवाला बुत्ता दे जाता। वह कहीं नजर में न आता। पक्षी उसके इंतजार में घुलता रहता।
लेकिन दीमकों का शौक जो उसे था। उसने सोचा, ‘मैं खुद दीमकें ढूँढ़ँगा।’ इसलिए वह पेड़ पर से उतर कर जमीन पर आ गया; और घास के एक लहराते गुच्छे में सिमट कर बैठ गया।
(श्यामला मेरी ओर देखे जा रही थी। उसने अपेक्षापूर्वक कहा ‘हूँ।’)
फिर एक दिन उस पक्षी के जी में न मालूम क्या आया। वह खूब मेहनत से जमीन में से दीमकें चुन-चुन कर, खाने के बजाय उन्हें इकट्टा करने लगा। अब उसके पास दीमकों के ढेर के ढेर हो गए।
फिर एक दिन एकाएक वह गाड़ीवाला दिखाई दिया। पक्षी को बड़ी खुशी हुई। उसने पुकार कर कहा, ‘गाड़ीवाले, ओ गाड़ीवाले! मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था।’
पहचानी आवाज सुन कर गाड़ीवाला रुक गया। तब पक्षी ने कहा, ‘देखो, मैंने कितनी सारी दीमकें जमा कर ली है।’
गाड़ीवाले को पक्षी की बात समझ में नहीं आई। उसने सिर्फ इतना कहा, ‘तो मैं क्या करूँ।’
‘ये मेरी दीमकें ले लो, और मेरे पंख मुझे वापस कर दो।’ पक्षी ने जवाब दिया।
गाड़ीवाला ठठा कर हँस पड़ा। उसने कहा, ‘बेवकूफ, मैं दीमक के बदले पंख लेता हूँ, पंख के बदले दीमक नहीं।
गाड़ीवाले ने ‘पंख’ शब्द पर जोर दिया था।
(श्यामला ध्यान से सुन रही थी। उसने कहा, ‘फिर’)
गाड़ीवाला चला गया। पक्षी छटपटा कर रह गया। एक दिन एक काली बिल्ली आई और अपने मुँह में उसे दबा कर चली गई। तब उस पक्षी का खून टपक-टपक कर जमीन पर बूँदों की लकीर बना रहा था।
(श्यामला ध्यान से मुझे देखे जा रही थी; और उसकी एकटक निगाहों से बचने के लिए मेरी आँखें तालाब की सिहरती-काँपती, चिलकती-चमचमाती लहरों पर टिकी हुई थीं)
कहानी कह चुकने के बाद, मुझे एक जबरदस्त झटका लगा। एक भयानक प्रतिक्रिया – कोलतार-जैसी काली, गंधक-जैसी पीली-नारंगी!
‘नहीं, मुझमें अभी बहुत कुछ शेष है, बहुत कुछ। मैं उस पक्षी-जैसा नहीं मरूँगा। मैं अभी भी उबर सकता हूँ। रोग अभी असाध्य नहीं हुआ है। ठाठ से रहने के चक्कर से बँधे हुए बुराई के चक्कर तोड़े जा सकते हैं। प्राणशक्ति शेष है, शेष ।’
तुरंत ही लगा कि श्यामला के सामने फिजूल अपना रहस्य खोल दिया, व्यर्थ ही आत्म-स्वीकार कर डाला। कोई भी व्यक्ति इतना परम प्रिय नहीं हो सकता कि भीतर का नंगा। बालदार, रीछ उसे बताया जाए। मैं असीम दु:ख के खारे मृत सागर में डूब गया।
श्यामला अपनी जगह से धीरे से उठी, साड़ी का पल्ला ठीक किया, उसकी सलवटें बराबर जमाईं, बालों पर से हाथ फेरा। और फिर (अंगरेजी में) कहा, ‘सुंदर कथा है, बहुत सुंदर!’
फिर वह क्षण-भर खोई-सी खड़ी रही, और फिर बोली, ‘तुमने कहाँ पढ़ी?’
मैं अपने ही शून्य में खोया हुआ था। उसी शून्य के बीच में से मैंने कहा, ‘पता नहीं… किसी ने सुनाई या मैंने कहीं पढ़ी।’
और वह श्यामला अचानक मेरे सामने आ गई, कुछ कहना चाहने लगी, मानो उस कहानी में उसकी किसी बात की ताईद होती हो।
उसके चेहरे पर धूप पड़ी हुई थी। मुखमंडल सुंदर और प्रदीप्त दिखाई दे रहा था।
कि इसी बीच हमारी आँखें सामने के रास्ते पर जम गईं।
घुटनों तक मैली धोती और काली, सफेद या लाल बंडी पहने कुछ देहाती भाई, समूह में चले आ रहे थे। एक के हाथ में एक बड़ा-सा डंडा था, जिसे वह अपने आगे, सामने किए हुए था। उस डंडे पर एक लंबा मरा हुआ साँप झूल रहा था। कला भुजंग, जिसके पेट की हलकी सफेदी भी झलक रही थी।
श्यामला ने देखते ही पूछा, ‘कौन-सा साँप है यह?’ वह ग्रामीण मुख छत्तीसगढ़ी लहजे में चिल्लाया, ‘करेट है बाई, करेट ।’
श्यामला के मुँह से निकल पडा, ‘ओफ्फो! करेट तो बड़ा जहरीला साँप होता है।’
फिर मेरी ओर देख कर कहा, ‘नाग की तो दवा भी निकली है, करेट की तो कोई दवा नहीं है। अच्छा किया, मार डाला। जहाँ साँप देखो, मार डालो, फिर वह पनियल साँप ही क्यों न हो ।’
और फिर न जाने क्यों, मेरे मन में उसका यह वाक्य गूँज उठा, ‘जहाँ साँप देखो, मार डालो।’
और ये शब्द मेरे मन में गूँजते ही चले गए।
कि इसी बीच… रजिस्टर में चढ़े हुए आँकड़ों की एक लंबी मीजान मेरे सामने झूल उठी और गलियारे के अँधेरे कोनों में गरम होनेवाली मुट्ठियों का चोर हाथ ।
श्यामला ने पलट कर कहा, ‘तुम्हारे कमरे में भी तो साँप घुस आया था, कहाँ से आया था वह?’
फिर उसने खुद ही जबाब दे लिया, ‘हाँ, वह पास की खिड़की में से आया होगा।’
खिड़की की बात सुनते ही मेरे सामने, बाहर की काँटेदार झाड़ियाँ, बेंत की झाड़ियाँ आ गईं, जिसे जंगली बेल ने लपेट रखा था । मेरे खुद के तीखे काँटों के बावजूद, क्या श्यामला मुझे इसी तरह लपेट सकेगी। बड़ा ही ‘रोमांटिक’ खयाल है, लेकिन कितना भयानक।
… क्योंकि श्यामला के साथ अगर मुझे जिंदगी बसर करनी है तो न मालूम कितने ही भगवे खद्दर कुरतेवालों से मुझे लड़ना पड़ेगा, जी कड़ा करके लड़ाइयाँ मोल लेनी पड़ेगी और अपनी आमदनी के जरिए खत्म कर देने होंगे। श्यामला का क्या है! वह तो एक गाँधीवादी कार्यकर्ता की लड़की है, आदिवासियों की उस कुल्हाड़ी-जैसी है जो जंगल में अपने बेईमान और बेवफा साथी का सिर धड़ से अलग कर देती है। बारीक बेईमानियों का सूफियाना अंदाज उसमें कहाँ!
किंतु फिर भी आदिवासियों जैसे उस अमिश्रित आदर्शवाद में मुझे आत्मा का गौरव दिखाई देता है, मनुष्य की महिमा दिखाई देती है, पैने तर्क की अपनी अंतिम प्रभावोत्पादक परिणति का उल्लास दिखाई देता है – और ये सब बाते मेरे हृदय का स्पर्श कर जाती हैं। तो, अब मैं इसके लिए क्या करूँ, क्या करूँ!
और अब मुझे सज्जायुक्त भद्रता के मनोहर वातावरण वाला अपना कमरा याद आता है… अपना अकेला धुँधला-धुँधला कमरा। उसके एकांत में प्रत्यावर्तित और पुन: प्रत्यावर्तित प्रकाश कोमल वातावरण में मूल-रश्मियाँ और उनके उद्गम स्त्रोतों पर सोचते रहना, खयालों की लहरों में बहते रहना कितना सरल, सुंदर और भद्रतापूर्ण है। उससे न कभी गरमी लगती है, न पसीना आता है, न कभी कपड़े मैले होते हैं। किंतु प्रकाश के उद्गम के सामने रहना, उसका सामना करना, उसकी चिलचिलाती दोपहर में रास्ता नापते रहना और धूल फाँकते रहना कितना त्रास-दायक है। पसीने से तरबतर कपड़े इस तरह चिपचिपाते हैं और इस कदर गंदे मालूम होते हैं कि लगता है… कि अगर कोई इस हालत में हमें देख ले तो वह बेशक हमें निचले दर्जे का आदमी समझेगा। सजे हुए टेबल पर रखे कीमत फाउंटेनपेन-जैसे नीरव-शब्दांकन-वादी हमारे व्यक्तित्व जो बहुत बड़े ही खुशनुमा मालूम होते हैं – किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण – जब वे आँगन में और घर-बाहर चलती हुई झाड़ू जैसे काम करनेवाले दिखाई दें, तो इस हालत में यदि सड़क-छाप समझे जाएँ तो इसमें आश्चर्य की ही क्या बात है!
लेकिन मैं अब ऐसे कामों की शर्म नहीं करूँगा, क्योंकि जहाँ मेरा हृदय है, वहीं मेरा भाग्य है!
ब्रह्मराक्षस का शिष्य – कहानी
उस महाभव्य भवन की आठवीं मंजिल के जीने से सातवीं मंजिल के जीने की सूनी-सूनी सीढियों पर उतरते हुए, उस विद्यार्थी का चेहरा भीतर से किसी प्रकाश से लाल हो रहा था।
वह चमत्कार उसे प्रभावित नहीं कर रहा था, जो उसने हाल-हाल में देखा। तीन कमरे पार करता हुआ वह विशाल वज्रबाहु हाथ उसकी आँखों के सामने फिर से खिंच जाता। उस हाथ की पवित्रता ही उसके खयाल में जाती किन्तु वह चमत्कार, चमत्कार के रूप में उसे प्रभावित नहीं करता था। उस चमत्कार के पीछे ऐसा कुछ है, जिसमें वह घुल रहा है, लगातार घुलता जा रहा है। वह कुछ क्या एक महापण्डित की जिन्दगी का सत्य नहीं है? नहीं, वही है! वही है!
पाँचवी मंजिल से चौथी मंजिल पर उतरते हुए, ब्रह्मचारी विद्यार्थी, उस प्राचीन भव्य भवन की सूनी-सूनी सीढियों पर यह श्लोक गाने लगता है।
मेघैर्मेदुरमम्बरं वनभवः श्यामास्तमालद्रुमैः – इस भवन से ठीक बारह वर्ष के बाद यह विद्यार्थी बाहर निकला है। उसके गुरू ने जाते समय, राधा-माधव की यमुना-कूल-क्रीडा में घर भूली हुई राधा को बुला रहे नन्द के भाव प्रकट किये हैं। गुरू ने एक साथ श्रृंगार और वात्सल्य का बोध विद्यार्थी को करवाया। विद्याध्ययन के बाद, अब उसे पिता के चरण छूना है। पिताजी! पिताजी! माँ! माँ! यह ध्वनि उसके हृदय से फूट निकली।
किन्तु ज्यों-ज्यों वह छन्द सूने भवन में गूँजता, घूमता गया त्यों-त्यों विद्यार्थी के हृदय में अपने गुरू की तसवीर और भी तीव्रता से चमकने लगी।
भाग्यवान् है वह जिसे ऐसा गुरू मिले!
जब वह चिडियों के घोंसलों और बर्रों के छत्तों-भरे सूने ऊँचे सिंहाद्वार के बाहर निकला तो एकाएक राह से गुजरते हुए लोग भूत भूत कह कर भाग खडे हुए। आज तक उस भवन में कोई नहीं गया था। लोगों की धारणा थी कि वहाँ एक ब्रह्मराक्षस रहता है।
बारह साल और कुछ दिन पहले —
सडक़ पर दोपहर के दो बजे, एक देहाती लडक़ा, भूखा-प्यासा अपने सूखे होठों पर जीभ फेरता हुआ, उसी बगल वाले ऊँचे सेमल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। हवा के झोकों से, फूलों के फलों का रेशमी कपास हवा में तैरता हुआ, दूर-दूर तक और इधर-उधर बिखर रहा था। उसके माथे पर फिक्रें गुँथ-बिंध रही थीं। उसने पास में पडी हुई एक मोटी ईंट सिरहाने रखी और पेड-तले लेट गया।
धीरे-धीरे, उसकी विचार-मग्नता को तोडते हुए कान के पास उसे कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। वे कौन थे?
उनमें से एक कह रहा था, ”अरे, वह भट्ट। नितान्त मूर्ख है और दम्भी भी। मैंने जब उसे ईशावास्योपनिषद् की कुछ पंक्तियों का अर्थ पूछा, तो वह बौखला उठा। इस काशी में कैसे-कैसे दम्भी इकठ्ठे हुए हैं?
वार्तालाप सुनकर वह लेटा हुआ लडक़ा खट से उठ बैठा। उसका चेहरा धूल और पसीने से म्लान और मलिन हो गया था, भूख और प्यास से निर्जीव।
वह एकदम, बात करनेवालों के पास खडा हुआ। हाथ जोडे, माथा जमीन पर टेका। चेहरे पर आश्चर्य और प्रार्थना के दयनीय भाव! कहने लगा, हे विद्वानों! मैं मूर्ख हूँ। अपढ देहाती हूँ किन्तु ज्ञान-प्राप्ति की महत्वाकांक्षा रखता हूँ। हे महाभागो! आप विद्यार्थी प्रतीत होते हैं। मुझे विद्वान गुरू के घर की राह बताओ।
पेड-तले बैठे हुए दो बटुक विद्यार्थी उस देहाती को देखकर हँसने लगे; पूछा –
कहाँ से आया है?
दक्षिण के एक देहात से! …पढने-लिखने से मैंने बैर किया तो विद्वान् पिताजी ने घर से निकाल दिया। तब मैंने पक्का निश्चय कर लिया कि काशी जाकर विद्याध्ययन करूँगा। जंगल-जंगल घूमता, राह पूछता, मैं आज ही काशी पहुँचा हूँ। कृपा करके गुरू का दर्शन कराइए।
अब दोनों विद्यार्थी जोर-जोर से हँसने लगे। उनमें-से एक, जो विदूषक था, कहने लगा —
देख बे सामने सिंहद्वार है। उसमें घुस जा, तुझे गुरू मिल जायेगा। कह कर वह ठठाकर हँस पडा।
आशा न थी कि गुरू बिलकुल सामने ही है। देहाती लडक़े ने अपना डेरा-डण्डा सँभाला और बिना प्रणाम किये तेजी से कदम बढाता हुआ भवन में दाखिल हो गया।
दूसरे बटुक ने पहले से पूछा, तुमने अच्छा किया उसे वहाँ भेज कर? उसके हृदय में खेद था और पाप की भावना।
दूसरा बटुक चुप था। उसने अपने किये पर खिन्न होकर सिर्फ इतना ही कहा, आखिर ब्रह्मराक्षस का रहस्य भी तो मालूम हो।
सिंहद्वार की लाल-लाल बरें गूँ-गूँ करती उसे चारों ओर से काटने के लिए दौडी; लेकिन ज्यों ही उसने उसे पार कर लिया तो सूरज की धूप में चमकनेवाली भूरी घास से भरे, विशाल, सूने आँगन के आस-पास, चारों ओर उसे बरामदे दिखाई दिये — विशाल, भव्य और सूने बरामदे जिनकी छतों में फानूस लटक रहे थे। लगता था कि जैसे अभी-अभी उन्हें कोई साफ करके गया हो! लेकिन वहाँ कोई नहीं था।
आँगन से दीखनेवाली तीसरी मंजिल की छज्जेवाली मुँडेरे पर एक बिल्ली सावधानी से चलती हुई दिखाई दे रही थी। उसे एक जीना भी दिखाई दिया, लम्बा-चौडा, साफ-सुथरा। उसकी सीढियाँ ताजे गोबर से पुती हुई थीं। उसकी महक नाक में घुस रही थी। सीढियों पर उसके चलने की आवाज गूँजती; पर कहीं, कुछ नहीं!
वह आगे-आगे चढता-बढता गया। दूसरी मंजिल के छज्जे मिले जो बीच के आँगन के चारों ओर फैले हुए थे। उनमें सफेद चादर लगी गद्दियाँ दूर-दूर तक बिछी हुई थीं। एक ओर मृदंग, तबला, सितार आदि अनेक वाद्य-यन्त्र करीने से रखे हुए थे। रंग-बिरंगे फानूस लटक रहे थे और कहीं अगरबत्तियाँ जल रही थीं।
इतनी प्रबन्ध-व्यवस्था के बाद भी उसे कहीं मनुष्य के दर्शन नहीं हुए। और न कोई पैरों की आवाजें सुनाई दीं, सिवाय अपनी पग-ध्वनि के। उसने सोचा शायद ऊपर कोई होगा।
उसने तीसरी मंजिल पर जाकर देखा। फिर वही सफेद-सफेद गद्दियाँ, फिर वही फानूस, फिर वही अगरबत्तियाँ। वही खाली-खालीपन, वही सूनापन, वही विशालता, वही भव्यता और वही मनुष्य-हीनता।
अब उस देहाती के दिल में से आह निकली। यह क्या? यह कहाँ फँस गया; लेकिन इतनी व्यवस्था है तो कहीं कोई और जरूर होगा। इस खयाल से उसका डर कम हुआ और वह बरामदे में से गुजरता हुआ अगले जीने पर चढने लगा।
इन बरामदों में कोई सजावट नहीं थी। सिर्फ दरियाँ बिछी हुई थीं। कुछ तैल-चित्र टँगे थे। खिडक़ियाँ खुली हुई थीं जिनमें-से सूरज की पीली किरणें आ रही थीं। दूर ही से खिडक़ी के बाहर जो नजर जाती तो बाहर का हरा-भरा ऊँचा-नीचा, माल-तलैयों, पेडों-पहाडों वाला नजारा देखकर पता चलता कि यह मंजिल कितनी ऊँची हैं और कितनी निर्जन।
अब वह देहाती लडक़ा भयभीत हो गया। यह विशालता और निर्जनता उसे आतंकित करने लगी। वह डरने लगा। लेकिन वह इतना ऊपर आ गया था कि नीचे देखने ही से आँखों में चक्कर आ जाता। उसने ऊपर देखा तो सिर्फ एक ही मंजिल शेष थी। उसने अगले जीने से ऊपर की मंजिल चढना तय किया।
डण्डा कन्धे पर रखे और गठरी खोंसे वह लडक़ा धीरे-धीरे अगली मंजिल का जीना चढने लगा। उसके पैरों की आवाज उसी से जाने क्या फुसलाती और उसकी रीढ
क़ी हड्डी में-से सर्द संवेदनाएँ गुजरने लगतीं।
जीन खत्म हुआ तो फिर एक भव्य बरामदा मिला, लिपा-पुता और अगरू-गन्ध से महकता हुआ। सभी ओर मृगासन, व्याघ्रासन बिछे हुए। एक ओर योजनों विस्तार-दृश्य देखती, खिडक़ी के पास देव-पूजा में संलग्न-मन मुँदी आँखोंवाले ॠषि-मनीषि कश्मीर की कीमती शाल ओढे ध्यानस्थ बैठे।
लडक़े को हर्ष हुआ। उसने दरवाजे पर मत्था टेका। आनन्द के आँसू आँखों में खिल उठे। उसे स्वर्ग मिल गया।
ध्यान-मुद्रा भंग नहीं हुई तो मन-ही-मन माने हुए गुरू को प्रणाम कर लडक़ा जीने की सर्वोच्च सीढी पर लेट गया। तुरन्त ही उसे नींद आ गयी। वह गहरे सपनों में खो गया। थकित शरीर और सन्तुष्ट मन ने उसकी इच्छाओं को मूर्त-रूप दिया। ..वह विद्वान् बन कर देहात में अपने पिता के पास वापस पहुँच गया है। उनके चरणों को पकडे, उन्हें अपने आँसुओं से तर कर रहा है और आर्द्र-हृदय हो कर कह रहा है, पिताजी! मैं विद्वान बन कर आ गया, मुझे और सिखाइए। मुझे राह बताइए। पिताजी! पिताजी! और माँ अंचल से अपनी आँखें पोंछती हुई, पुत्र के ज्ञान-गौरव से भर कर, उसे अपने हाथ से खींचती हुई गोद में भर रही है। साश्रुमुख पिता का वात्सल्य-भरा हाथ उसके शीश पर आशीर्वाद का छत्र बन कर फैला हुआ है।
वह देहाती लडक़ा चल पडा और देखा कि उस तेजस्वी ब्राह्मण का दैदिप्यमान चेहरा, जो अभी-अभी मृदु और कोमल होकर उस पर किरनें बिखेर रहा था, कठोर और अजनबी होता जा रहा है।
ब्राह्मण ने कठोर होकर कहा, तुमने यहाँ आने का कैसे साहस किया? यहाँ कैसे आये?लडक़े ने मत्था टेका, भगवन्! मैं मूढ हूँ, निरक्षर हूँ, ज्ञानार्जन करने के लिए आया हूँ।
ब्राह्मण कुछ हँसा। उसकी आवाज धीमी हो गयी किन्तु दृढता वही रही। सूखापन और कठोरता वही।
तूने निश्चय कर लिया है?
जी!
नहीं, तुझे निश्चय की आदत नहीं है; एक बार और सोच ले! …ज़ा फिलहाल नहा-धो उस कमरे में, वहाँ जाकर भोजन कर लेट, सोच-विचार! कल मुझ से मिलना।
दूसरे दिन प्रत्युष काल में लडक़ा गुरू से पूर्व जागृत हुआ। नहाया-धोया। गुरू की पूजा की थाली सजायी और आज्ञाकारी शिष्य की भांति आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। उसके शरीर में अब एक नई चेतना आ गयी थी। नेत्र प्रकाशमान थे।
विशालबाहु पृथु-वक्ष तेजस्वी ललाटवाले अपने गुरू की चर्या देखकर लडक़ा भावुक-रूप से मुग्ध हो गया था। वह छोटे-से-छोटा होना चाहता था कि जिससे लालची चींटी की भाँति जमीन पर पडा, मिट्टी में मिला, ज्ञान की शक्कर का एक-एक कण साफ देख सके और तुरन्त पकड सके!
गुरू ने संशयपूर्ण दृष्टि से देख उसे डपट कर पूछा; सोच-विचार लिया?
जी! की डरी हुई आवाज!
कुछ सोच कर गुरू ने कहा, नहीं, तुझे निश्चय करने की आदत नहीं है। एक बार पढाई शुरू करने पर तुम बारह वर्ष तक फिर यहाँ से निकल नहीं सकते।
सोच-विचार लो। अच्छा, मेरे साथ एक बजे भोजन करना, अलग नहीं!
और गुरू व्याघ्रासन पर बैठकर पूजा-अर्चा में लीन हो गये। इस प्रकार दो दिन और बीत गये। लडक़े ने अपना एक कार्यक्रम बना लिय था, जिसके अनुसार वह काम करता रहा। उसे प्रतीत हुआ कि गुरू उससे सन्तुष्ट हैं।
एक दिन गुरू ने पूछा, तुमने तय कर लिया है कि बारह वर्ष तक तुम इस भवन के बाहर पग नहीं रखोगे?
नतमस्तक हो कर लडक़े ने कहा, जी!
गुरू को थोडी हँसी आयी, शायद उसकी मूर्खता पर या अपनी मूर्खता पर, कहा नहीं जा सकता। उन्हें लगा कि क्या इस निरे निरक्षर के आँखें नहीं है? क्या यहाँ का वातावरण सचमुच अच्छा मालूम होता है? उन्होंने अपने शिष्य के मुख का ध्यान से अवलोकन किया। एक सीधा, भोला-भाला निरक्षर बालमुख! चेहरे पर निष्कपट, निश्छल ज्योति!
अपने चेहरे पर गुरू की गडी हुई दृष्टि से किंचित विचलित होकर शिष्य ने अपनी निरक्षर बुध्दिवाला मस्तक और नीचा कर लिया।
गुरू का हृदय पिघला! उन्होंने दिल दहलाने वाली आवाज से, जो काफी धीमी थी, कहा, देख! बारह वर्ष के भीतर तू वेद, संगीत, शास्त्र, पुराण, आयुर्वेद, साहित्य, गणित आदि-आदि समस्त शास्त्र और कलाओं में पारंगत हो जावेगा। केवल भवन त्याग कर तुझे बाहर जाने की अनुज्ञा नहीं मिलेगी। ला, वह आसन। वहाँ बैठ।
और इस प्रकार गुरू ने पूजा-पाठ के स्थान के समीप एक कुशासन पर अपने शिष्य को बैठा, परंपरा के अनुसार पहले शब्द-रूपावली से उसका विद्याध्ययन प्रारम्भ कराया।
गुरू ने मृदुता ने कहा, — बोलो बेटे —
रामः, रामौ, रामाः
और इस बाल-विद्यार्थी की अस्फुट हृदय की वाणी उस भयानक निःसंग, शून्य, निर्जन, वीरान भवन में गूँज-गूँज उठती।
सारा भवन गाने लगा —
रामः रामौ रामाः — प्रथमा!
धीरे-धीरे उसका अध्ययन सिध्दान्तकौमुदी तक आया और फिर अनेक विद्याओं को आत्मसात् कर, वर्ष एक-के-बाद-एक बीतने लगे। नियमित आहार-विहार और संयम के फलस्वरूप विद्यार्थी की देह पुष्ट हो गयी और आँखों में नवीन तारूण्य की चमक प्रस्फुटित हो उठी। लडक़ा, जो देहाती था अब गुरू से संस्कृत में वार्तालाप भी करने लगा।
केवल एक ही बात वह आज तक नहीं जान सका। उसने कभी जानने का प्रयत्न नहीं किया। वह यह कि इस भव्य-भवन में गुरू के समीप इस छोटी-सी दुनिया में यदि और कोई व्यक्ति नहीं है तो सारा मामला चलता कैसे है? निश्चित समय पर दोनों गुरू-शिष्य भोजन करते। सुव्यवस्थित रूप से उन्हें सादा किन्तु सुचारू भोजन मिलता। इस आठवीं मंजिल से उतर सातवीं मंजिल तक उनमें से कोई कभी नहीं गया। दोनों भोजन के समय अनेक विवादग्रस्त प्रश्नों पर चर्चा करते। यहाँ इस आठवीं मंजिल पर एक नई दुनिया बस गयी।
जब गुरू उसे कोई छन्द सिखलाते और जब विद्यार्थी मन्दाक्रान्ता या शार्दूल्विक्रीडित गाने लगता तो एकाएक उस भवन में हलके-हलके मृदंग और वीणा बज उठती और वह वीरान, निर्जन, शून्य भवन वह छन्द गा उठता।
एक दिन गुरू ने शिष्य से कहा, बेटा! आज से तेरा अध्ययन समाप्त हो गया है। आज ही तुझे घर जाना है। आज बारहवें वर्ष की अन्तिम तिथि है। स्नान-सन्ध्यादि से निवृत्त हो कर आओ और अपना अन्तिम पाठ लो।
पाठ के समय गुरू और शिष्य दोनों उदास थे। दोनों गम्भीर। उनका हृदय भर रहा था। पाठ के अनन्तर यथाविधि भोजन के लिए बैठे।
दूसरे कक्ष में वे भोजन के लिए बैठे थे। गुरू और शिष्य दोनों अपनी अन्तिम बातचीत के लिए स्वयं को तैयार करते हुए कौर मुँह में डालने ही वाले थे कि गुरू ने कहा, बेटे, खिचडी में घी नहीं डाला है?
शिष्य उठने ही वाला था कि गुरू ने कहा, नहीं, नहीं, उठो मत! और उन्होंने अपना हाथ इतना बढा दिया कि वह कक्ष पार जाता हुआ, अन्य कक्ष में प्रवेश कर क्षण के भीतर, घी की चमचमाती लुटिया लेकर शिष्य की खिचडी में घी उडेलने लगा। शिष्य काँप कर स्तम्भित रह गया। वह गुरू के कोमल वृध्द मुख को कठोरता से देखने लगा कि यह कौन है? मानव है या दानव? उसने आज तक गुरू के व्यवहार में कोई अप्राकृतिक चमत्कार नहीं देखा था। वह भयभीत, स्तम्भित रह गया।
गुरू ने दुःखपूर्ण कोमलता से कहा, शिष्य! स्पष्ट कर दूँ कि मैं ब्रह्मराक्षस हूँ किन्तु फिर भी तुम्हारा गुरू हूँ। मुझे तुम्हारा स्नेह चाहिए। अपने मानव-जीवन में मैंने विश्व की समस्त विद्या को मथ डाला किन्तु दुर्भाग्य से कोई योग्य शिष्य न मिल पाया कि जिसे मैं समस्त ज्ञान दे पाता। इसीलिए मेरी आत्मा इस संसार में अटकी रह गयी और मैं ब्रह्मराक्षस के रूप में यहाँ विराजमान रहा।
तुम आये, मैंने तुम्हें बार-बार कहा, लौट जाओ। कदाचित् तुममें ज्ञान के लिए आवश्यक श्रम और संयम न हो किन्तु मैंने तुम्हारी जीवन-गाथा सुनी। विद्या से वैर रखने के कारण, पिता-द्वारा अनेक ताडनाओं के बावजूद तुम गँवार रहे और बाद में माता-पिता-द्वारा निकाल दिये जाने पर तुम्हारे व्यथित अहंकार ने तुम्हें ज्ञान-लोक का पथ खोज निकालने की ओर प्रवृत्त किया। मैं प्रवृत्तिवादी हूँ, साधु नहीं। सैंकडों मील जंगल की बाधाएँ पार कर तुम काशी आये। तुम्हारे चेहरे पर जिज्ञासा का आलोक था। मैंने अज्ञान से तुम्हारी मुक्ति की। तुमने मेरा ज्ञान प्राप्त कर मेरी आत्मा को मुक्ति दिला दी। ज्ञान का पाया हुआ उत्तदायित्व मैंने पूरा किया। अब मेरा यह उत्तरदायित्व तुम पर आ गया है। जब तक मेरा दिया तुम किसी और को न दोगे तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं।
शिष्य, आओ, मुझे विदा दो।
अपने पिताजी और माँजी को प्रणाम कहना। शिष्य ने साश्रुमुख ज्यों ही चरणों पर मस्तक रखा आशीर्वाद का अन्तिम कर-स्पर्श पाया और ज्यों ही सिर ऊपर उठाया तो वहाँ से वह ब्रह्मराक्षस तिरोधान हो गया।
वह भयानक वीरान, निर्जन बरामदा सूना था। शिष्य ने ब्रह्मराक्षस गुरू का व्याघ्रासन लिया और उनका सिखाया पाठ मन-ही-मन गुनगुनाते हुए आगे बढ ग़या।
काठ का सपना – कहानी
भरी, धुआँती मैली आग जो मन में है और कभी-कभी सुनहली आँच भी देती है। पूरा शनिश्चरी रूप।
वे एक बालिका के पिता हैं, और वह बालिका एक घर के बरामदे की गली में निकली मुँडेर पर बैठी है, अपने पिता को देखती हुई। उन्हें देख उसके दुबले पीले चेहरे पर मुस्कराहट खिलती है। और वह अपने दोनों हाथ आगे कर देती है जिससे कि उसके काका उसे अपने कंधों पर ले लें।
उसके पिता अपनी बालिकाओं को देख प्रसन्न नहीं होते हैं। विक्षुब्ध हो जाता है उनका मन। नन्हीं बालिका सरोज का पीला उतरा चेहरा, तन में फटा हुआ सिर्फ एक ‘फ्राक’ और उसके दुबले हाथ उन्हें बालिका के प्रति अपने कर्तव्य की याद दिलाते हैं; ऐसे कर्तव्य की जिसे वे पूरा नहीं कर सके, कर भी नहीं सकेगें, नहीं कर सकते थे। अपनी अक्षमता के बोध से ये चिढ़ जाते हैं। और वे उस नन्हीं बालिका को डाँट कर पूछते हैं, ‘यहाँ क्यों बैठी है? अंदर क्यों नहीं जाती।’
बालिका सरोज, गंभीर, वृद्ध दार्शनिक-सी बैठी रहती है। अपने क्रोध पर पिता को लज्जा आती है। उनका मन गलने लगता है। उनके हृदय में बच्ची के प्रति प्यार उमड़ता है। वे उसे अपने कंधे पर ले लेते हैं। ऊँचे उठने का सुख अनुभव कर बच्ची मुस्करा उठती है।
पिता बच्ची को लिए घर में प्रवेश करते हैं तो एक ठंडा सूना, मटियाली बास-भरा अँधेरा प्रस्तुत होता है, पिछवाड़े के अंतिम छोर में आसमान की नीलाई का एक छोटा चौकोर टुकड़ा खड़ा हुआ है! वह दरवाजा है।
घर में कोई नहीं है।
सिर्फ दो साँसें हैं,
एक पिता की।
दूसरी पुत्री की।
वे एक अँधेरे कोने में बैठ जाते हैं और उनके घुटनों में वह बालिका है। उसका चेहरा पिता को दिखाई नहीं देता। फिर भी वह पूरा-का-पूरा महसूस होता है। वे चुपचाप उसके गाल पर हाथ फेरते जाते हैं और सोचते हैं कि वह लड़की मेरे समान ही धैर्यवान है, सब कुछ पहचानती है। बड़ी प्यारी लड़की है। उन्हें लगता है कि उनकी आँखे तर हो रही हैं।
एकाएक खयाल आता है कि अगर घर में बड़ा आईना होता तो अच्छा होता; अपनी बड़ी आँसू-भरी सूरत की बदसूरती देख लेते। उन्हें उमर रसीदा आदमियों का रोना अच्छा नहीं लगता।
सामने, अँधेरे में, रंग-बिरंगी पर धुँधली आकृतियाँ तैर जाती हैं। सुंदर चेहरेवाली एक लड़की है, वह उनकी सरोज है! नारंगी साड़ी है, सुनहली किनारी है सफेद ब्लाउज है! गले में हार है। हाथों में रंग-बिरंगी चूड़ियाँ हैं – एक-एक दर्जन! पति के घर से वापस लौटी है। खुश है, दामाद मैकेनिकल इंजीनियर है जिसकी गरीब सूरत है। और वह बाहर बरामदे में कुरसी पर बैठा है; क्या करे सूझता नहीं!
घर में उनकी स्त्री पूड़ी बना रही है। पकौड़ियाँ बन रही हैं। बहुत-बहुत-सी चीजें हैं। भाग-दौड़ है। हल्ला-गुल्ला है। शोर-शराबा है। लोग आ-आ कर बैठ रहे हैं – आ रहे हैं, जा रहे हैं। पास-पड़ोस की लुगाइयाँ चौके में मदद कर रही हैं। और उनके दिल में… क्या करें, क्या न करें, सब कुछ कर डालें! क्या ही अच्छा होता कि उनमें यह ताकत होती कि वे सबको प्रसन्न कर सकते और सारी दुनिया को खुश देख सकते। …कि इतने में सपना टूट जाता है।
बरामदे का दरवाजा बज उठता है। पैरों की आवाज से साफ जाहिर होता है कि स्त्री, जो कहीं गई थी लौट आई है।
अंदर आ कर देखती है। उसे अचंभा होता है। ‘यहाँ क्या कर रहे हो?’
उसकी आवाज गूँजती है। जैसे लोहे की साँकल बजती है। जैसे ईमान बजता है!
‘सरोज कहाँ है?’
कोई आवाज नहीं! सरोज और उसके पिता स्तब्ध बैठे हैं।
पिता बोलते हैं मानो छाती के कफ को चीरती हुई घरघराती आवाज आ रही हो। कहते हैं, ‘कहाँ गई थी? घर बड़ा सूना लग रहा था।’
स्त्री कोई जवाब नहीं दे कर वहाँ से चली जाती है। आँगन में पहुँच कर, जमीन में गड़ा हुआ एक पुराना पेड़, जो कट चुका है और जिसकी झिल्लियाँ बिखरी हैं, उस पर पैर रख कर खड़ी होती है। जमीन में उस कटे पेड़ में से जमीन की तहें छूते हुए नए अंकुर निकले हैं। बाद मे उन पर से उतर कर वह झिल्लियाँ बीनती है। पड़ोस से लाई हुई कुल्हाड़ी चला कर उन अधकटे ठूँठों से लकड़ी निकालने का खयाल आता है। लेकिन काटने का जी नहीं होता। इसलिए झिल्लियाँ बीन कर वह उनका एक ढेर बना देती है और फिर आँगन की दीवार की मुँडेर पर चढ़ जाती है, क्योंकि उस मुँडेर के एक ओर नीम की एक सूखी डाल निकल आई है।
उसे वह तोड़ती है। ऊँची मुँडेर पर चढ़ कर नीम की सूखी डाल तोड़ लाने का जो साहस है, उस साहस से दीप्त हो कर वह प्रफुल्ल हो जाती है। सारी लकड़ी ठंडे चूल्हे के पास लाती है, जमा कर देती है।
सरोज पिता की गोद से उठ आई है। वह देखती है कि चूल्हे में सुनहली ज्वाला निकल रही है! वह देखती है, और देखती रह जाती है। उसे उस ज्वाला का रंग अच्छा लगता है। वह चूल्हे के पास जा कर बैठ गई है। उसकी रीढ़ की हड्डी दु:ख रही है, पर चूल्हे में जलती हई ज्वाला उसे अच्छी लग रही है।
सारा चौका सुहाना हो उठता है – भूरा-मटियाला, साफ-सुथरा! भीत की पटिया पर रखी पीतल की एक भगोनी, छोटे-छोटे दो गिलास और दो कटोरियाँ, कैसी चमचमा रही हैं, कितनी सुंदर! उन पर माँ का हाथ फिरा है। तभी तो… तभी तो…।
सुबह के पकाए भात में पानी डाला जाता है और नमक! चूल्हे पर चढ़ गया है भात! सुबह का बेसन भी है। उसमें पानी मिला दिया जाता है। उसे भी चूल्हे के दूसरे मुँह पर रख दिया गया है, सीझता रहेगा!
सरोज बोलती नहीं, माँ बोलती नहीं, पिता बोलते नहीं!
जब वह नन्ही बालिका भोजन कर चुकी तो उसकी जान में जान आई। बोरे पर बिछे, माँ के चिथड़े से बने, अपने मुलायम बिस्तर पर वह सो गई। पिताजी के बिस्तर से सटा हुआ उसका बिस्तर है! वे उसे अपने पास नहीं लेते। रात को वह बिस्तर गीला करती है, इसलिए!
दोनों तथाकथित बिस्तरों पर लेट गए हैं! दोनों को नींद नहीं! दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं; कहना आवश्यक है। उस पूर्व-ज्ञान को वे कहना-सुनना नहीं चाहते। वह पूर्व-ज्ञान वेदनाकारक है, इसलिए उसे न कहना ही अच्छा! फिर भी न कहने से काम नहीं बनता, क्योंकि कह-सुन लेने से अपने-अपने निवेदनों पर सील लग जाती है, व्यक्तिगत मुहर लग जाती है। वह व्यक्तिगत मुहर अभी लगी नहीं हैं। हर एक उत्तर हर एक ज्ञान है। फिर भी बहुत कुछ अज्ञात छूट जाता है!
वे नहीं चाहते थे कि रात में नींद के पहले के ये कुछ क्षण खराब हो जाएँ, मन:स्थिति विकृत हो और दुर्दमनीय चिंता से ग्रस्त हो कर वे रात-भर जागते-कराहते रहें। नहीं, ऐसा नहीं! चिंता सुबह उठ कर करेंगे। रात है। यह रात अपनी है। कल की कल देखी जाएगी!
किंतु इन खयालों से माथे का दुखना नहीं थमता, देह की थकान दूर नहीं होती, असंतोष की आग और बेबसी का धुआँ दूर नहीं होता।
नहीं, उसका एक उपाय है! जबरदस्ती नींद लाने के लिए आप एक से सौ तक गिनते जाइए! इस तरह, आप कई बार गिनेंगे, दिमाग थक जाएगा और आप ही आप भीतर अँधेरा छा जाएगा। एक दूसरा तरीका है! रेखागणित की एक समस्या ले लीजिए। मन-ही-मन चित्र तैयार कीजिए। उसके कोणों को नाम दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। अंत तक आने के पहले ही नींद घेर लेगी। एक और भी मार्ग है, जिसे इस लेख का लेखक अपनाया करता है! मस्तिष्क की सारी नसें ढीली कर दीजिए। आँखे मूँद कर पलकें बिलकुल बंद करके, सिर्फ अँधेरे को एकाग्र देखते रहिए। तरह-तरह की तसवीरें बनेंगी। पेड़दार रास्ते और उस पर चलती हुई भीड़ अथवा पहाड़ और नदियाँ जिनकों पार करती हुई रेलगाड़ी… भक-भक-भक ।
अँधेरा जड़ हो गया और छाती पर बैठ गया। नहीं, उसे हटाना पड़ेगा ही – सरोज के पिता सोच रहे हैं! और उनकी आँखे बगल में पड़े हुए बिस्तर की ओर गईं।
वहाँ हलचल है। वहाँ भी बेचैनी है। लेकिन कैसी?
…लेकिन उन दोनों में न स्वीकार है न अस्वीकार! सिर्फ एक संदेह है, यह संदेह साधार है कि इस निष्क्रियता में एक अलगाव है – एक भीतरी अलगाव है। अलगाव में विरोध है, विरोध में आलोचना है, आलोचना में करुणा है। आलोचना पूर्णत: स्वीकरणीय है, जिसे इस पुरुष ने कभी पूरा नहीं किया। वह पूरा नहीं कर सकता।
कर्तव्य कर्म को पूरा करना केवल उसके संकल्प-द्वारा ही नहीं हो सकता। उसके लिए और भी कुछ चाहिए! फिर भी, वह पुरुष मन-ही-मन यह वचन देता है, यह प्रतिज्ञा करता है कि कल जरूर वह कुछ-न-कुछ करेगा; विजयी हो कर लौटेगा।
पुरुष में भी आवेश नहीं है। वह भी ठंडा है, सिर्फ गरमी लाने की कोशिश कर रहा है।
वह उसकी बाँहों में थी। निश्चेष्ट शरीर! फिर भी, उसमें एक उष्मा है, जो मानो सौ नेत्रों से अपने पुरुष को देख रही हो, निर्णय प्रदान करने के लिए प्रमाण एकत्र कर रही हो। फिर भी निश्चेष्ट और सक्रिय!
पुरुष संवेदनाओं के जाल में खो गया। उसे स्त्री के होठ गुलाब की सूखी पंखुरियों-से लगे, जिससे उसे सूरज की गरमी की याद आई। उसके कपोल मिट्टी-से थे – भुसभुसी, नमकीन, शुष्क मृत्तिका! उसका हृदय एक अनजानी गूढ़ करुणा की सूचना से भर उठा। …हाँ, उसका पेट, उसकी त्वचा में तो घरेलू बास थी। उसने उसे अपनी बाँहों में भर लिया और वह, मन-ही-मन, उस पूरी गरम चिलकती हुई पृथ्वी को याद करने लगा जिस पर वह बेसहारा मारा-मारा फिरता है। क्या यह पृथ्वी उतनी ही दु:खी रही है जितना कि वह स्वयं है!
एक उर्जा उठी और गिर गई। पुरुष निश्चेष्ट पड़ा रहा। मन जाग्रत था।
…दोनों स्त्री-पुरुष के जीवन पर विराम का पूर्ण चिह्न लग गया है, काठ हो गए हैं। बाढ़ आती है। किनारे पर पड़े हुए काठों को बहा कर ले जाती है। जल-विप्लव में। काठ बहते जाते हैं, फिर भी वे प्राणहीन काठ, आपस में गुँथे हुए बहे जा रहे हैं।
बादल-तूफान के कारण, पेड़ तिरछे हो रहे हैं। पर वे गुँथे-बँधे बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं… और, हाँ गुँथे-बँधे काठ खाली नहीं हैं। उन पर एक बालिका बैठी हुई है। हाँ, वह सरोज है। अपने नन्हे दो हाथ उसने दोनों के काठों पर टेक दिए हैं, जिनके सहारे वह स्वयं चली जा रही है।
सरोज की उस बाल मूर्ति की रक्षा करनी ही होगी! उन दो निष्प्राण काठ-लट्ठों का यही कर्तव्य है।
पुरुष इस स्वप्न को देखता ही रहता है। बारह का गजर होता है। रात और आगे बढ़ती है। सप्तर्षि, जो अब तक कोने में थे, सामने आ कर साफ दिखाई देते हैं।
अँधेरे में – कहानी
एक रात को बारह बजे, ट्रेन से एक युवक उतरा। स्टेशन पर लोग एक कतार में खड़े थे और ज्यादा नहीं थे। इसलिए ट्रेन से नीचे आने में उसको ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। स्टेशन पर बिजली की रोशनी थी; परंतु वह रात के अँधियारे को चीर न सकती थी, और इसलिए मानो रात अपने सघन रेशमी अँधियारे से तंबूनुमा घर हो गई थी, जिसमें बिजली के दीये जलते हों। उतरते ही युवक को प्लेटफॉर्म की परिचित गंध ने, जिसमें गरम धुआँ और ठंडी हवा के झोंके, गरम चाय की बास और पोर्टरों के काले लोहे में बंद मोटे काँचों से सुरक्षित पीली ज्वालाओं के कंदीले पर से आती हुई अजीब उग्र बास, इत्यादि सारी परिचित ध्वनियाँ और गंध थे, उसकी संज्ञा से भेंट की। युवक के हृदय में जैसे एक दरवाजा खुल गया था, एक ध्वनि के साथ और मानो वह ध्वनि कह रही थी – आ गया, अपना आ गया
युवक झटपट उतरा। उसके पास कुछ भी सामान नहीं था, कोयले के कणों से भरे हुए लंबे बालों में हाथों से कंघी करता हुआ वह चला। पाँच साल पहले वह यहीं रहता था। इन पाँच सालों की अवधि में दुनिया में काफी परिवर्तन हो गया; परंतु उस स्टेशन पर परिवर्तन आना पसंद नहीं करता था। युवक ने अपने पूर्वप्रिय नगर की खुशी में एक कप चाय पीना स्वीकार किया। और वहीं स्टॉल पर खडा हो कर कपबशी की आवाज सुनता हुआ इधर-उधर देखने लगा। सब पुराना वातावरण था। परंतु इस नगर के मुहल्ले में बीस साल बिता चुकने वाला यह पच्चीस साल का युवक पुराना नहीं रह गया था। उसकी आत्मा एक नए महीन चश्मे से स्टेशन को देख रही थी।
टिकिट दे कर स्टेशन पर आगे बढ़ा तो देखता है कि ताँगे निर्जल अलसाए बादलों कि भाँति निष्प्रभ और स्फूर्तिहीन ऊँघते हुए चले जा रहे हैं। युवक ने इसी से पहचान लिया कि यह विशेषता इस नगर की अपनी चीज है।
दुकानें सब बंद हो चुकी थीं, जिनके पास नीचे सड़क पर आदमी सिलसिलेवार सो रहे थे। उनके साथी और उन्हीं के समान सभ्य पशुओं में से निर्वासित श्वान-जाति दुबकी इधर-उधर पड़ी हुई थी। युवक ने पैर बढ़ाने शुरू कर दिए। उखड़ी हुई डामर की काली सड़क पर बिजली की धुँधली रोशनी बिखर रही थी। एक ओर दुकानें, फिर सराय, फिर अफीम-गोदाम, फिर एक टुटपुँजिया म्यूनिसिपल पार्क, फिर एक छोटा चौराहा जहाँ डनलप टॉयर के विज्ञापनवाली दुकान और उसके सामने लाल पंप, फिर उसके बाद कॉलेज! और इस तरह इस छोटे शहर की बौनी इमारतें और नकली आधुनिकता इसी सड़क के किनारे-किनारे एक ओर चली गई थी। दूसरी ओर रेल का हिस्सा, जहाँ शंटिंग का सिलसिला इस समय कुछेक घंटों के लिए चुप था।
युवक को रात का यह वातावरण अत्यंत प्रिय मालूम हुआ। गरमी के दिन थे। फिर भी हवा बहुत ठंडी चल रही थी। सड़क के खुले हिस्से मे जहाँ रेल के तार जा रहे थे, नीम और पीपल के वृक्ष के पत्ते झिरमिर-झिरमिर कर सघन आम के बड़े-बड़े दरख्त दूर से ही दीख रहे थे। उसी मैदान पर, एक ओर, एक नवीन मुहल्ला, शहर के अमीरों, व्यापारियों, अफसरों का उपनिवेश सिकुड़ा हुआ था।
सब दूर शांति थी। रात का गाढ़ा मौन था। युवक के रोजमर्रा के कर्मप्रधान जीवन में रोज रात का एक सोने का समय था, और सुबह के साढ़े आठ के अनंतर जागने का समय था। वैदिक ॠषि-मनीषियों के उष:सूक्त से लगा कर तो अत्याधुनिक छायावादियों के ‘बीती विभावरी जाग री, अंबर पनघट ऊषा नागरी’ का दर्शन इस युवक ने इस गए पाँच सालों में बहुत कम किया है।
अपने उस कर्म-जटिल क्षेत्र को पीछे छोड़ कर जैसे मनुष्य अपनी अरुचिकर यादों से बचना चाहता हो – यह युवक इस रात में पा रहा था कि वातावरण में पठार-मैदान से उठ कर आने वाली हवा की उत्फुल्ल और मीठी ताजगी के साथ-ही-साथ मानो मनुष्यों की सोई हुई चुपचाप आत्माएँ अपनी गाढ़ नीरवता में अधिक मधुर हो कर वन की सुगंध और वृक्ष के मर्मर में मिल गई हैं।
रेल की पटरियों के पार – रेलवे यार्ड में ही वहाँ के मध्यमवर्गीय नौकरों के क्वार्टर्स बने हुए थे। बाहर ही, जो उसका आँगन कहा जा सकता है; दो खाटें समानांतर बिछी हुई थीं जिनके बीच में एक छोटा-सा टेबल रखा हुआ था। उस पर एक आधुनिक लैंप अपनी अध्ययन समर्पित रोशनी डाल रहा था। एक खाट पर एक पुरुष कोई पुस्तक पढ़ रहा था और दूसरी पर घोर निद्रा थी। लैंप की धुँधली रोशनी में घर के सामनेवाले बाजू पर एक काला-सा अधखुला दरवाजा ओर बाँस की चिमटियों से बनाए गए बंद बरामदे के लेटे-से चतुष्कोण साफ दीख रहे थे। उस घर की पंक्ति में ही कई क्वार्टर्स और दीख रहे थे, उसी तरह पंक्तिबद्ध खाटें बराबर यथास्थान लगी हुई चली गई थीं।
युवक के मन में एक प्यार उमड़ आया! ये घर उसे अत्यंत आत्मीय-जैसे लगे, मानो वे उसके अभिन्न अंग हों!
यही बात उसकी समझ में नहीं आई। इस अजीब आनंदमय भावना ने उसके मन के संतुलित तराजू को झटके देने शुरू कर दिए। वह भावनाओं से अब इतना अभ्यस्त नहीं रह गया था कि उनका आदर्शीकरण कर सके। रोज का कठिन, शुष्क, जीवन उसे एक विशेष तरह का आत्मविश्वास-सा देता था। परंतु… आज…
वह बैठने वाला जीव न था। रास्ते पर पैर चल रहे थे। मन कहीं घूम रहा था। दूसरे उसे अत्यंत आत्मीय एकांत, जहाँ उसकी सहज प्रवृत्तियों का खुला बालिश खिलवाड़ हो बहुत दिनों से नहीं मिला था!
उसने सोचना शुरू किया कि आखिर क्यों यह अजीब जल के निर्मलिन सहस्त्र स्रोतों-सी भावना उसके मन में आ गई!
उसको जहाँ जाना था, वहाँ का रास्ता उसे मिल नहीं सकता था। एक तो यह कि पाँच साल के बाद शहर की गलियों को वह भूल चुका था। दूसरे जिस स्थान पर उसे जाना था, वह किसी खास ढंग से उसे अरुचिकर मालूम हो रहा था! इसलिए लक्ष्यस्थान की बात ही उसके दिमाग से गायब हो गई थी।
पैर चल रहे थे या उसके पैर के नीचे से रास्ता खिसक रहा था, यह कहना संभव नहीं, परंतु यह जरूर है कि कुछ कुत्ते-चिर जाग्रत रक्षक की भाँति खड़े हुए – भूँक रहे थे।
उसके मन में किसी अजान स्त्रोत से एक घर का नक्शा आया। उसका भी बरामदा इसी तरह बाँस की चिमटियों से बना हुआ था। वहाँ भी वासंती रातों में नीम के झिरिर-मिरिर के नीचे खाटें पड़ी रहती थीं। युवक को एक धुँधली सूरत याद आती है, उसकी बहन की-और आते ही फौरन चली जाती है। बस चित्र इतना ही। यह मत समझिए कि उसके माता-पिता मर गए! उसके भाई हैं, माता-पिता हैं। वे सब वहीं रहते हैं जिस शहर में वह रहता है।
युवक हँस पड़ा। उसे समझ में आ गया कि क्यों उन क्वार्टरों को देख कर एक आत्मीयता उमड़ आई। मजदूर चालों में, जहाँ वह नित्य जाता है, या उसके अमीर दोस्तों के स्वच्छ सुंदर मकानों में, जहाँ से वह चंदा इकट्ठा करता, चाय पीता, वाद-विवाद करता और मन-ही-मन अपने महत्व को अनुभव करता है – वहाँ से तो कोई आत्मीयता की फसफसाहट नहीं हुई। हमारा युवक अपने पर ही हँसने लगा। एक सूक्ष्म, मीठा और कटु हास्य।
दूर, एक दुकान पर साठ नंबर का खास बेलजियम का बिजली का लट्टू जल रहा था। सड़क पर ही कुरसियाँ पड़ी थीं, बीच मे टेबल था। एक आरामकुरसी पर लाल भैरोगढ़ी तहमत बाँधे हुए ताँगेवाले साहब बैठे हुए बिस्कुट खा रहे थे। दूसरी कुरसी पर एक निहायत गंदा, पीछे से फटी हुई चड्ढी पहने, उघाड़े बदन, लडका कभी बिस्कुटों के चूरे खाने की तरफ या भाप उठाते हुए टेबल पर रखे चाय के कप की तरफ देखता हुआ बैठा था! दूसरी कुरसी पर दूसरे मुसलमान सज्जन रोटी और मांस की कोई पतली वस्तु खा रहे थे और बहुत प्रसन्न मालूम हो रहे थे। जो होटल का मालिक था वह एक पैर पर अधिक दबाव डाले – उसको खूँटा किए खड़ा था, सिगरेट पी रहा था और कुछ खास बुद्धिमानी की बातें करता था जिसको सुन कर रोटी और मांस की पतली वस्तु को दोनों हाथों का उपयोग कर खाने वाले मुसलमान सज्जन ‘अल्लाहो अकबर’ ‘अल्ला रहम करे, इत्यादि भावनाप्लुत उद्गारों से उसका समर्थन करते जाते थे। सिगरेट का कश वह इतनी जोर से खींचता था कि उसका ज्वलंत भाग बिजली की भयानक रोशनी में भी चमक रहा था। उसका हाथ आराम से जंघा-क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था।
दुकान के अंदर से पानी को झाड़ू से फेंकने की क्रिया में झाड़ू की कर्कश दाँत पीसती-सी आवाज और पानी के ढकेले जाने के बालिश ध्वनि आ रही थी, साथ ही उसके छोटे-छोटे कंकड़ों की भाँति लगातार बाहर उन्नत-वक्र रेखा-मार्ग से चले आ रहे थे। बिजली का लट्टू दरवाजे के ऊपर लगे हुए कवर के बहुत नीचे लटक रहा, था जिस पर लगातार गिरने वाले छींटे सूख कर धब्बे बन रहे थे।
इतने में पुलिस के एक गश्तवान सिपाही लाल पगड़ी पहने और खाकी पोशाक में आ कर बैठ गए! वे भी मुसलमान ही थे। उनकी दाढ़ी पर छह बाल थे, और ओठों पर तो थे ही नहीं। चालीस साल की उम्र हो चुकी थी पर बालों ने उन पर कृपा नहीं की थी। नाक उनकी बुद्धि से व्यापक थी, काले डोरे की गुंडी की भाँति चमक रही थी। आँख में एक चुपचाप दयनीयता झाँक उठती। वह कोई मुसीबतजदा प्राणी था – शायद उसे सूजाक था – या उसकी घरवाली दूसरे के साथ फरार हो गई थी! या वह किसी अभागी बदसूरत-वेश्या का शरीर-जात था। उसे न जाने कौन-सी पीड़ा थी जो चार आदमियों में प्रकट नहीं की जा सकती थी। वह पीड़ा-थीड़ा तो दूसरों के आनंद और निर्बाध हास्य को देख कर चुपचाप निबिड़ आँखों में चमक उठती थी! वह इस समय भी चमक रहीं थी, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसके सामने क्रमानुसार चाय आ गई और वह फुर-फुर करते हुए पीने लगा।
ताँगेवाले महाशय का ताँगा वहीं दुकान के सामने सड़क के दूसरे किनारे खड़ा था। घोड़ा अपने मालिक की भाँति बड़ा चढ़ैल और गुस्सैल था। एक ओर तो वह बिजली की रोशनी में चमकनेवाली हरी घास को बादशाह की भाँति खा रहा था, तो दूसरी ओर आध घंटे में एक बार अपनी टाँग ताँगे में मार देता था। उसके घास खाने की आवाज लगातार आ रही थी और उसका भव्य सफेद गंभीर चेहरा होटल को अपेक्षा की दृष्टि से देख रहा था।
ताँगेवाले महाशय ने चाय पीनी शुरू की। तगड़ा मुँह था। बेलौस सीधी नाक थी और उजला रंग था। ठाठदार मोतिया साफा अब भी बँधा हुआ था। बोलो-चाल निहायत शुस्ता और सलीके से भरी थी। चेहरा पर मार्दव था जो कि किसी अक्खड़ बहादुर सिपाही में ही सकता है। आज दिन में उन्होंने काफी कमाई की थी; इसीलिए रात में जगने का उत्साह बहुत अधिक मालूम हो रहा था।
दुकान के अंदर झाड़ू की कर्कश आवाज और पानी की खलखल ध्वनि बंद हो गई। छोटी-छोटी बूँदें टपकानेवाली मैली झाड़ू लिए एक पंद्रह साल का लड़का, एक घुटने पर से फटे पाजामे को कमर पर इकट्ठा किए खड़ा था कि मालिक का अब आगे क्या हुक्म होता है। परंतु बाहर मजलिस जमी थी। लाल साफेवाला सिपाही बड़ी रुचि के साथ उसे सुन रहा था। चाहता था कि वह भी कुछ कहे…।
इतने में इन लोगों को दूर से एक छाया आती हुई दिखाई दी। सब लोगों ने सोचा कि इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं! पर धीरे-धीरे आनेवाली उस छाया का सिर्फ पैंट ही दिखाई दिया और कुछ थकी-सी चाल! युवक चुपचाप उन्हीं की ओर आया और हलकी-सी आवाज में बोला ‘चाय है?’ उत्तर में ‘हाँ’ पा कर और बैठने के लिए एक अच्छी आरामदेह कुरसी पा कर वह खुश मालूम हुआ। लोगों ने जब देखा कि चेहरे से कोई खास आकर्षक या आसाधारण आदमी मालूम नहीं होता, तब आश्वस्त हो, साँस ले कर बातें करने लगे!
लाल पगड़ीवाला दयनीय प्राणी कुछ बोलना चाहता था! इतने मे उसके दो साथी दूर से दिखाई दिए! उन्हें देख कर वह अत्यंत अनिच्छा से वहाँ से उठने लगा। उसने सोचा था कि शायद है कोई, बैठने को कहे। परंतु लोगों को मालूम भी नहीं हुआ कि कोई आया था और जा रहा है!
‘माधव महारज के जमाने में ताँगेवालों को ये आफत नहीं थी मौलवी सॉब! मैंने बहुत जमाना देखा है! कई सुपरडंट आए, चले गए, कोतवाल आए, निकल गए। पर अब पुलिसवाला ताँगे में मुफ्त बैठेगा भी, और नंबर भी नोट करेगा…’ ताँगेवाले ने कहा।
होटलवाला जो अब तक मौलवी साहब से कुछ खास बुद्धिमानी की बात कर रहा था, उसने अब जोर से बोलना शुरू किया! धोती की तहमत बाँधे, बहुत दुबला, नाटे कद का एक अधेड़ हँसमुख आदमी था। वह बहुत बातूनी, और बहुत खुशमिजाज आदमी और अश्लील बातों से घृणा करनेवाला, एक खास ढंग से संस्कारशील और मेहनती मालूम होता था। उसने कहा, ‘मौलवी सॉब, दुनिया यों ही चलती रहेगी। मैंने कई कारोबार किए। देखा, सबमें मक्कारी है। और कारोबारी की निगाह में मक्कारी का नाम दुनियादारी है। पुलिसवाले भी मक्कार हैं – ताँगेवाले कम मक्कार नहीं हैं। वह जैनुल आबेदीन-मिर्जावाड़ी में रहने वाला… सुना है आपने किस्सा!’
मौलवी साहब ठहाका मार कर हँस पड़े। ‘या अल्लाह’ कहते हुए दाढ़ी पर दो बार हाथ फेरा और अपनी उकताहट को छिपाते हुए – मौलवी साहब को एक कप चाय और बिस्कुट मुफ्त या उधार लेना था – आँखों में मनोरंजन विस्मय – कुढ़ कर होटलवाले की बात सुनने लगे।
होटलवाले ने अपने जीवन का रहस्योद्घाटन करने से डर कर बात को बदलते हुए कहा, ‘मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। दुनिया में बदमाशी है, बदतमीजी है। है, पर करना क्या? गालियों से तो काम नहीं चलता, क्यों रहीमबक्श (ताँगेवाले की ओर संकेत कर) ताँगेवाले बहुत गालियाँ देते हैं! दूसरे, सड़क पर से गुजरती हुई औरतों को देख – चाहे वे मारवाड़िनियाँ ही हों ढिल्लमढाल पेटवाली, बस इन्हें फौरन लैला याद आ जाती है! यह देख कर मेरी रूह काँपती है। मौलवी सॉब, मेरा दिल एक सच्चे सैयद का दिल है! एक दफा क्या हुआ कि हजरत अली अपने महल में बैठे हुए थे। और राज-काज देख रहे थे कि इतने में दरबान ने कहा कि कुछ मिस्त्री सौदागर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अब उनमें का एक सौदागर आलिम था।’
मौलवी सिर्फ उसके चेहरे को देख रहे थे जिस पर अनेक भावनाएँ उमड़ रहीं थीं, जिससे उसका चिपका – काला चेहरा और भी विकृत मालूम होता था। दूसरे वह यह अनुभव कर रहे थे कि यह अपना ज्ञान बघार रहा है और ज्ञान का अधिकार तो उन्हें है। तीसरे, उन्होंने यह योग्य समय जान कर कहा, ‘भाई, एक कप चाय और बुलवा दो।’
चाय का नाम सुन कर कुरसी पर बैठे हुए युवक ने कहा, ‘एक कप यहाँ भी।’
पीछे से फटी चड्ढी पहने हुए गंदा लड़का ऊँघ रहा था! वह ऊँघता हुआ ही चाय लाने लगा। ताँगेवाला रहीमबख्श बातों को गौर से सुन रहा था। वह जानना चाहता था कि इस कहानी का ताँगेवालों से क्या संबंध है!
होटलवाले ने कहना शुरू किया, उनमें का एक सौदागर आलिम था। उसने हजरत अली का नाम सुन रखा था कि गरीबों के ये सबसे बड़े हिमायती हैं। शानो-शौकत बिलकुल पसंद नहीं करते। और अब देखता क्या है कि महल की दीवारें संगमरमर से बनी हुई हैं, जिसमें ख्वाब-कोहके हीरे दरवाजों के मेहराबों पर जड़े हुए हैं और चबूतरा काले चिकने संगमूसे का बना हुआ है। हरे-हरे बाग हैं और फव्वारे छूट रहे हैं। वह मन-ही-मन मुसकराया। गरमी पड़ रही थी, और रूमाल से बँधे हुए सिर से पसीना छूट रहा था।
हजरत अली के सामने जब माल की कीमत नक्की हो चुकी, तो सौदागर उनकी मेहरबान सूरत से खिंच कर बोला, ‘बादशाह सलामत! सुना था कि हजरत अली गरीबों के गुलाम हैं। पर मैंने कुछ और ही देखा है। हो सकता है, गलत देखा हो।’
सौदागर अपना गट्ठा बाँधते-बाँधते कह रहे थे। हजरत अली की आँख से एक बिलजी-सी निकली। सौदागर ने देखा नहीं, उसकी पीठ उधर थी, वह अपने माल का गट्ठा बाँध रहा था!
हजरत अली ने कहा, ‘ज्यादा बातें मैं आपसे नहीं कहना चाहता। आप मुझे इस वक्त महल में देखते हैं, पर हमेशा यहाँ नहीं रहता। बाजार में अनाज के बोरे उठाते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा है।’ हजरत अली की आँखें किसी खास बेचैनी से चमक रही थीं!
वे रेशम का लंबा शाही लबादा पहने हुए थे। उन्होंने उसके बंद खोले। सौदागर ने आश्चर्य से देखा कि हजरत अली मोटे बोरे के कपड़े अंदर से पहने हुए हैं।
सौदागर ने सिर नीचा कर लिया।
सैयद होटलवाले की आँखों में आँसू आ गए। मौलवी साहब ने सिर नीचा कर लिया, मानो उन्हें सौ जूते पड़ गए हों। चाय की गरमी सब खतम हो गई। ताँगेवाले को इसमें खास मजा नहीं आया। युवक अपनी कुरसी पर बैठा हुआ ध्यान से सुन रहा था।
होटलवाले ने कहा, ‘असली मजहब इसे कहते हैं। मेरे पास मुस्लिम लीगी आते हैं! चंदा माँगते हैं। मुस्लिम कौम निहायत गरीब है! मुझसे पाकिस्तान नहीं माँगते। मुझसे पाकिस्तान की बातें भी नहीं करते। हिंदू-मुस्लिम इत्तेहाद पर मेरा विश्वास है। लेकिन मैं जरूर दे देता हूँ। ‘कौमी-जंग’ अखबार देखा है आपने? उसकी पॉलिसी मुझे पसंद है। लाल बावटे वालों का है। मैं उन्हें भी चंद देता हूँ। मेरा ममेरा भाई ‘बिरला मिल’ में है। खाता कमेटी का सेक्रेटरी है। वह मुझसे चंदा ले जाता है।’
युवक अब वहाँ बैठना नहीं चाहता था। फिर भी, सैयद साहब की बातों को पूरा सुन लेने की इच्छा थी। मालूम होता था, आज वे मजे में आ रहे हैं।
रात काफी आगे बढ़ चुकी थी। होटल के सामने म्युनिसिपल बगीचे के बड़े-बड़े दरख्त रात की गहराई में ऊँघ-से रहे थे, जिनके पीछे आधा चाँद, मुस्लिम नववधू के भाल पर लटकते हुए अलंकार के समान लग रहा था।
नवयुवक जब और चलने लगा तो मालूम हुआ कि उसके पीछे भी कोई चल रहा है। उन दोनों के पैरों की आवाज गूँज रही थी। परंतु चाँद की तरफ (जिसकी काली पृष्ठभूमि भी कुछ आरुण्य लिए थी, मानो किसी मुग्ध रुचिर चेहरे पर खिली हुई लाल मिठास हो), जो घने दरख्तों के पीछे से उठ रहा था, वह युवक मुँह उठाए देखता जा रहा था। विशाल, गहरा काला, शुक्रतारकालोकित आकाश और नीचे निस्तब्ध शांति जो दरख्तों की पत्तियों में भटकने वाले पवन की क्रीड़ा में गा उठती थी।
युवक ऐसी लंबी एकांत रात में अर्ध-अपरिचित नगर की राह में अनुभव कर रहा था कि मानो नग्न आसमान, मुक्त दिशा और (एकाकी स्वपथचारी सौंदर्य के उत्सा-सा, व्यक्तिनिरपेक्ष मस्त आत्मधारा के खुमार-सा) नित्य नवीन चाँद से लाखों शक्ति-धाराएँ फूट कर नवयुवक के हृदय में मिल रही हों। नग्न, ठंडे पाषाण-आसमान और चाँद की भाँति ही – उसी प्रकार, उसका हृदय नग्न और शुभ्र शीतल हो गया है। द्रव्य की गतिमयी धारा ही उसके हृदय में बह रही है। पाषाण जिस प्रकार प्रकृति का अविभाज्य अंग है, मनुष्य प्रकृति पर अधिकार करके भी अपने रूप से उसका अविभाज्य अंग है।
चाँद धीरे-धीरे आसमान में ऊपर सरक रहा था। वृक्षों का मर्मर रात के सुनसान अँधेरे में स्वप्न की भाँति चल रहा था, परस्पर-विरोधी विचित्रगति ताल के संयोग-सा।
जो छाया दो कदम पीछे चल रही थी, वह नवयुवक के साथ हो गई। नवयुवक ने देखा कि सफेद, नाजुक, लाठी के हिलते त्रिकोण पर चाँद की चाँदनी खेल रही है; लंबी और सुरेख नाक की नाजुक कगार पर चाँद का टुकड़ा चमक रहा है, जिससे मुँह का करीब-करीब आधा भाग छायाच्छन्न है। और दो गहरी छोटी आँखें चाँदनी और हर्ष से प्रतिबिंबित हैं। उस वृद्ध मौलबी के चेहरे को देख कर नवयुवक को डी.एच. लॉरेन्स का चित्र याद आ गया! उस अर्द्ध-वृद्ध ने आते ही अपनी ठेठ प्रकृति से उत्सुक हो कर पूछा, ‘आप कहाँ रहते है?’
वृद्ध के चेहरे पर स्वाभाविक अच्छाई हँस रही थी। इस नए शहर के (यद्यपि नवयुवक पाँच साल पहले यहीं रहता था) अजनबीपन में उसे इस मौलवी का स्वाभाविक अच्छाई से हँसता चेहरा प्रिय मालूम हुआ। उसने कहा, ‘मैं इस शहर से भलीभाँति वाकिक नहीं हूँ। सराय में उतरा हूँ। नींद आ रही थी, इसलिए बाहर निकल पड़ा हूँ।’
होटल में बैठा हुआ यह वृद्ध मौलवी सैयद से हार गया था, मानो उसकी विद्वत्ता भी हार गई थी। इस हार से मन में उत्पन्न हुए अभाव और आत्मलीन जलन को वह शांत करना चाहता था। ‘सैयद सॉब बहुत अच्छे आदमी हैं, हम लोगों पर उनकी बड़ी मेहरबानी है।’
नयुवक ने बात काट कर पूछा, ‘आप कहाँ काम करते हैं?’
‘मैं मस्जिद मदरसे में पढ़ाता हूँ। जी हाँ, गुजर करने के लिए काफी हो जाता है।’ उसकी आँखें सहसा म्लान हो गईं और वह चुप हो कर, गरदन झुका कर, नीचे देखने लगा। फिर कहा, ‘जी हाँ, दस साल पहले शादी हो चुकी थी। मालूम नहीं था कि वह गहने समेट करके चंपत हो जाएगी। …तब से इस मस्जिद में हूँ।’
युवक ने देखा कि बूढ़ा एक ऐसी बात कह गया है जो एक अपरिचित से कहना नहीं चाहिए। बूढ़े ने कुछ ज्यादा नहीं कहा। परंतु इतने नैकट्य की बात सुन कर युवक की सहानुभूति के द्वार खुल गए। उसने बूढ़े की सूरत से ही कई बातें जान लीं, वही दु:ख जो किसी-न-किसी रूप में प्रत्येक कुचले मध्यवर्गीय के जीवन में मुँह फाड़े खड़ा हुआ है।
‘जी हाँ, मस्जिद में पाँच साल हो गए, पंधरा रुपया मिलते हैं, गुजर कर लेता हूँ। लेकिन अब मन नहीं लगता। दुनिया सूनी-सूनी-सी लगती है। इस लड़ाई ने एक बात और पैदा कर दी है – दिलचस्पी! रेडियो सुनने में कभी नागा नहीं करता। रोज कई अखबार टटोल लेता हूँ। जी हाँ, एक नई दिलचस्पी। किताब पढ़ने का मुझे शौक जरूर है। पर मैं तालीमयफ्ता हूँ नहीं। तो, गर्जे कि समझ में नहीं आती।’
बूढ़ा अपनी नर्म, रेशमी, सितार के हलके तारों की गूँज-सी आवाज में कहता जा रहा था। बातें मामूली तथ्यात्मक थीं, परंतु उनके आस-पास भावना का आलोकवलय था। उसकी जिंदगी में आहत भावनाओं की जो तर्कहीन शक्ति थी, वह उसकी बातों की साधारणता में अपूर्व वैयक्तिक रंग भर देती थी।
युवक को यह अच्छा लगा। प्रिय मालूम हुआ। एक क्षण में उसने अपनी सहानुभूति की जादुई आँख से जान लिया कि कोई असंगत (अजीब) मस्जिद होगी, जहाँ रोज चुपचाप लोग यंत्रचालित-सी कतार में प्रार्थना पढ़ते होंगे। और उसकी सूनी, खाली, दूसरी मंजिल पर यह असंतुष्ट और जीवनपूर्ण अर्द्ध-वृद्ध छोटे-छोटे मैले-कुचैले लड़के-लड़कियों को दुपहर में पढ़ाता होगा। अपने लड़कों की ऊधम से परेशान माँ-बाप उन्हें काम में जुटाए रखने के लिए मदरसे में भेज देते होंगे, और यह अनमने भाव से पढ़ाता होगा और अपनी जिंदगी, दुनिया और दुपहर का सारा क्रुद्ध सूनापन इसके दिल में बेचैनी से तड़पता होगा…।
उसने मौलवी से पूछा, ‘अपकी उम्र क्या होगी!’
युवक ने देखा कि मौलवी को यह सवाल अच्छा लगा। उसका चेहरा और भी कोमल होता-सा दिखाई दिया। उसने कहा, ‘सिर्फ चालीस। यद्यपि मैं पचास साल के ऊपर मालूम होता हूँ। अजी, इन पाँच सालों ने मुझको खा डाला। फिर भी मैं कमजोर नहीं हूँ। काफी हट्टा-कट्टा हूँ।’
मौलवी यह सिद्ध करना चाहता था कि अभी वह युवक है। जीवन की स्वाभाविक, स्वातंत्र्यर्ण, उच्छृंखल आकांक्षा-शक्तियाँ उसके शरीर में तारल्य भर देती थीं। उसके चलने में, बातचीत में वह अंतिमता नहीं थी जो शैथिल्य और उदासी में पक्वता का आभास पैदा कर देती हैं। उसने चालीस ठीक कहा था और नवयुवक को भी उसकी बात पर अविश्वास करने की इच्छा न हुई।
‘ओफ्फो, तो आप जवान हैं।’ युवक ने थम कर आगे कहा, ‘तो आपका दिमाग लड़ाई पर जरूर चलता होगा…’
‘अरे, साहब! कुछ न पूछिए, सैयद साहब मुझसे परेशान हैं।’
‘आप ‘कौमी जंग’ पढते हैं? आपके होटल में तो मैंने अभी ही देखा है।’
‘कौमी-जंग तो हमारी मस्जिद में भी आता है! हमारे सबसे बड़े मौलवी परजामंडल के कार्यकर्ता हैं। जमीयत-उल-उलेमा हिंद के मुअज्जिज हैं। वहीं के उलेमा हैं। सब तरह के अखबार खरीदते हैं। यहाँ उन्होंने मुस्लिम-फारवर्ड ब्लॉक खोल रखा है।’
युवक को यहाँ की राजनीति में उलझने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी, उससे अलग रहने की भी कोई इच्छा नहीं थी। इतने में एक गली आ गई जिसमें मुड़ने के लिए मौलवी तैयार दिखाई दिया। युवक ने सिर्फ इतना ही कहा, ‘किताबों के लिए हम आपकी मदद करेंगे। अब तो मैं यहाँ हूँ कुछ दिनों के लिए। कहाँ मुलाकात होगी आपसे?’
‘सैयद साहब की होटल में। जी हाँ, सुबह और शाम!’
मौलवी साहब के साथ युवक का कुछ समय अच्छा कटा। वह कृतज्ञ था। उसने धन्यवाद दिया नहीं। उसकी जिंदगी में न मालूम कितने ही ऐसे आदमी आए हैं जिन्होंने उस पर सहज विश्वास कर लिया, उसकी जिंदगी में एक निर्वैयक्तिक गीलापन प्रदान किया। जब कभी युवक उन पर सोचता है। उनके झरनों ने उनकी जिंदगी को एक नदी बना दिया। उनमें से सब एक सरीखे नहीं थे। और न उन सबको उसने अपना व्यक्तित्व दे दिया था। परंतु उनके व्यक्तित्व की काली छायाओं, कंटकों और जलते हुए फास्फोरिक द्रव्यों, उनके दोषों से उसने नाक-भौं नहीं सिकोड़ी थी। अगर वह स्वयं कभी आहत हो जाता, तो एक बार अपना धुआँ उगल चुकने के बाद उनके व्रणों को चूमने और उनका विष निकाल फेंकने के लिए तैयार होता। उनके व्यक्तित्व की बारीक से बारीक बातों को सहानुभूति के मायक्रोस्कोप (बृहद्दर्शक ताल) से बड़ा करके देखने में उसे वही आनंद मिलता था, जो कि एक डॉक्टर को। और उसका उद्देश्य भी एक डॉक्टर का ही था। उसमें का चिकित्सक एक ऐसा सीधा-सादा हकीम था, जो दुनिया की पेटेंट दवाइयों के चक्कर में न पड़ कर अपने मरीजों से रोज सुबह उठने, व्यायाम करने, दिमाग को ठंडा रखने और उसको दो पैसे की दो पुड़िया शहद के साथ चाट लेने की सलाह देता था। सहानुभूति की एक किरण, एक सहज स्वास्थ्यपूर्ण निर्विकार मुसकान का चिकित्सा-संबंधी महत्व सहानुभूति के लिए प्यासी, लँगड़ी दुनिया के लिए कितना हो सकता है – यह वह जानता था! इसलिए वह मतभेद और परस्पर पैदा होने वाली विशिष्ट विसंवादी कटुताओं को बचा कर निकल जाता था। वह उन्हें जानता था और उसकी उसे जरूरत नहीं थी! दुनिया की कोई ऐसी कलुषता नहीं थी जिस पर उलटी हो जाय – सिवा विस्तृत सामाजिक शोषणों और उनके उत्पन्न दंभों और आदर्शवाद के नाम पर किए गए अंध अत्याचारों, यांत्रिक नैतिकताओं और आध्यात्मिक अहंताओं की तानाशाहियों को छोड़ कर! दुनिया के मध्यवर्गीय जनों के अनेक विषों को चुपचाप वह पी गया था, और राह देख रहा था सिर्फ क्रांति-शक्ति की! परंतु इससे उसको एक नुकसान भी हुआ था! व्यक्ति उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था, व्यक्तित्व अधिक, चाहे वह व्यक्तित्व मामूली ही हो और वह भी तभी जब तक उसकी जिज्ञासा और उष्णता का तालाब सूख न जाए। उसकी उष्णता का दृष्टिकोण भी काफी अमूर्त था क्योंकि उसके व्यक्तित्व का उद्देश्य अमूर्त था। इसलिए अपने आप में व्यक्ति उससे यदा-कदा छूट जाता था, सिवा उनके जो उसकी धड़कनों और रक्त के साथ मिल गए हैं! हकिम मरीजों को फौरन भूल जाते हैं, और मजे के लिए और मर्ज के साथ-साथ वे याद आते है। परिणामत: उसकी सहज उष्णता पा कर व्यक्ति उसके साथ एक हो जाते, अपने को नग्न कर देते; और फिर उससे नाना प्रकार की अपेक्षाएँ करने लगते जो संभव होना असंभव था।
मौलवी जब गली में मुड़ कर गया तो युवक की आँखें उस पर थीं। मौलवी का लंबा, दुबला और श्वेत वस्त्रवृत सारा शरीर उसे एक चलता-फिरता इतिहास मालूम हुआ। उसकी दाढ़ी का त्रिकोण, आँखों की चपल-चमक और भावना-शक्तियों से हिलते कपोलों का इतिहास जान लेने की इच्छा उसमें दुगुनी हो गई।
तब सड़क के आधे भाग पर चाँदनी बिछी थी और आधा भाग चंद्र के तिरछे होने के कारण छायाच्छन्न हो कर काला हो गया था। उसका कालापन चाँदनी से अधिक उठा हुआ मालूम हो रहा था।
युवक के सामने समस्याएँ दो थीं। एक आराम की, दूसरी आराम के स्थान की। और दो रास्ते थे। एक, कि रात-भर घूमा जाए – रात के समाप्त होने में सिर्फ साढ़े तीन घंटे थे और दूसरे, स्टेशन पर कहीं भी सो लिया जाए!
कुछ सोच-विचार कर उसने स्टेशन का रास्ता लिया।
उसके शरीर में तीन दिन के लगातार श्रम की थकान थी। और उसके पैर शरीर का बोझ ढोने से इनकार कर रहे थे। परंतु जिस प्रकार जिंदगी में अकेले आदमी को अपनी थकान के बावजूद भोजन खुद ही तैयार करना पड़ता है – तभी तो पेट भर सकता है – उसी प्रकार उसके पैर चुपचाप, अपने दु:ख की कथा अपने से ही कहते हुए अपने कार्य में संलग्न थे।
उसको एक बार मुड़ना पड़ा। वह एक कम चौड़ा रास्ता था जिसके दोनों ओर बड़ी-बड़ा अट्टालिकाएँ चुपचाप खडी थीं, जिसके पैरों-नीचे बिछा हुआ रास्ता दो पहाड़ियों में से गुजरे हुए रास्ते की भाँति गड्ढे में पड़ा हुआ मालूम होता था। बाईं ओर की अट्टालिकाओं के ऊपरी भाग पर चाँदनी बिछी हुई थी।
थकान से शून्य मन में नींद के झोंके आ रहे थे, परंतु एक डर था पुलिसवाले का जो अगर रास्ते में मिल जाए जो उसके संदेहों को शांत करना मुश्किल है! डर इसलिए भी अधिक है कि रास्ता अँधेरे से ढँका हुआ है, सिर्फ अट्टालिकाओं पर गिरी हुई चाँदनी के कुछ-कुछ प्रत्यावर्तित प्रकाश से रास्ते का आकार सूझ रहा है।
मन में शून्यता की एक और बाढ़। नींद का एक और झोंका। रास्ता दोनों ओर से बंद होने के कारण शीत से बचा हुआ है – उसमें अधिक गरमी है।
युवक कैसे तो भी चल रहा है! नींद के गरम लिहाफ में सोना चाहता है। नींद का एक और झोंका! मन में शून्यता की एक और बाढ़।
युवक के पैरों में कुछ तो भी नरम-नरम लगा – अजीब, सामान्यत: अप्राप्य, मनुष्य के उष्ण शरीर-सा कोमल! उसने दो-तीन कदम और आगे रखे। और उसका संदेह निश्चत में परिवर्तित हो गया। उसका शरीर काँप गया। उसकी बुद्धि, उसका विवेक काँप गया। वह यदि कदम नहीं रखता हैं तो एक ही शरीर पर – न जाने वह बच्चे का है या स्त्री का, बूढ़े का या जवान का – उसका सारा वजन एक ही पर जा गिरे। वह क्या करे? वह भागने लगा एक किनारे की ओर। परंतु कहाँ-वहाँ तक आदमी सोए हुए थे उसके शरीर की गरम कोमलता उसके पैरों से चिपक गई थी। वहीं एक पत्थर मिला; वह उस पर खड़ा हो गया, हाँफता हुआ। उसके पैर काँप रहे थे। वह आँखे फाड़-फाड़ कर देख रहा था। परंतु अँधेरे के उस समुद्र में उसे कुछ नहीं दीखा। यह उसके लिए और भी बुरा हुआ। उसका पाप यों ही अँधेरे में छिपा रह जाएगा! उसकी विवेक-भावना सिटपिटा कर रह गई; उसको ऐसा धक्का लगा कि वह सँभलने भी नहीं पाया। वह पुण्यात्मा विवेक शक्ति केवल काँप रही थी!
युवक के मन में एक प्रश्न, बिजली के नृत्य की भाँति मुड़ कर मटक-मटक कर, घूमने लगा – क्यों नहीं इतने सब भूखे भिखारी जग कर, जाग्रत हो कर, उसको डंडे मार कर चूर कर देते हैं – क्यों उसे अब तक जिंदा रहने दिया गया?
परंतु इसका जवाब क्या हो सकता है?
वह हारा-सा, सड़क के किनारे-किनारे चलने लगा! मानो उस गहरे अँधेरे में भी भूखी आत्माओं की हजार-हजार आँखें उसकी बुजदिली, पाप और कलंक को देख रहीं हों। स्टेशन की ओर जानेवाली सीधी सड़क मिलते ही युवक ने पटरी बदल ली।
लंबी सीधी सड़क पर चाँदनी आधी नहीं थी क्योंकि दोनों ओर अट्टालिकाएँ नहीं थीं; केवल किनारे पर कुछ-कुछ दूरियों से छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए थे। मौन, शीतल चाँदनी सफेद कफन की भाँति रास्ते पर बिछती हुई दो क्षितिजों को छू रही थी। एक विस्तृत, शांत खुलापन युवक को ढँक रहा था और उसे सिर्फ अपनी आवाज सुनाई दे रही थी – पाप, हमारा पाप, हम ढीले-ढाले, सुस्त, मध्यवर्गीय आत्म-संतोषियों का घोर पाप। बंगाल की भूख हमारे चरित्र-विनाश का सबसे बड़ा सबूत। उसकी याद आते ही, जिसको भुलाने की तीव्र चेष्टा कर रहा था, उसका हृदय काँप जाता था, और विवेक-भावना हाँफने लगती थी।
उस लंबी सुदीर्घ श्वेत सड़क पर वह युवक एक छोटी-सी नगण्य छाया हो कर चला जा रहा था।
सौन्दर्य के उपासक- कहानी
कोमल तृणों के उरस्थल पर मेघों के प्रेमाश्रु बिखरे पड़े थे। रवि की सांध्य किरणें उन मृदुल-स्पन्दित तृणों के उरों में न मालूम किसे खोज रही थी। मैं चुपचाप खड़ा था। बायाँ हाथ ‘उसके’ बाएँ कन्धे पर। कभी निसर्ग-देवता की इस रम्य कल्पना की ओर तो कभी मेरी प्रणयिनी के श्रम-जल-सिक्त सुन्दर मुख पर दृष्टिक्षेप करता हुआ न मालूम किस उत्ताल-तरंगित जलधि में गोते खा रहा था। सहसा मेरी स्थिति पर मेरा ध्यान गया। आसपास देखा कोई नहीं था। चिडि़याँ वृक्षों पर ‘किल बिल’ ‘किल बिल’ कर रही थी। मैंने उसकी पीठ पर कोमल थपकी देकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। वह शुचि स्मिता रमणी मेरी ओर किंचित हँस दी।
मैंने मौन तोड़ने के लिए कहा, ‘देखो, अनिल, कैसी मनोहर है प्रकृति की शोभा।’
वह ‘हूँ’ कहकर मुसकुरा दी। ‘अनिल, क्या तुम सौन्दर्य की उपासिका नहीं! अनिल, बोलो न !’ मैंने विव्हल होकर पूछा। ‘क्यों नहीं ! प्रमोद, मैं सौन्दर्य की उपासिका तो हूँ पर उसी सौन्दर्य के हृदय की भी। प्रमोद, घबराओ ना। मैं सोच रही थी कि यह निसर्ग देवी किसके लिए इतना रम्य, पवित्र, श्रृंगार किए बैठी हैं ! कौन है वह सौभाग्यशाली पुरूष ! प्रमोद, मैं सौन्दर्य की उपासिका हूँ, मैं प्रेम की उपासिका हूँ।’
- ‘तो क्या मैं तुमसे प्रेम नहीं करता ! तुम मुझे समझती क्या हो। सच-सच बतला दो, अनिल।’
‘मैं ! तुम्हें ! मेरे देवता, मेरे ध्येय, मेरी मुक्ति। मैं तुम्हें मेरा सब कुछ समझती हूँ प्रमोद।’
मैं खिल गया, मैंने उत्साहित होकर पूछा, ‘तो क्या मैं सौन्दर्य का उपासक नहीं?’
वह मेरे उरस्थल पर नशीली आँखें गड़ाती हुई समीपस्थ वृक्ष पर टिक गयी। अँधेरा हो चुका था।
- मैं दूसरे मंजिल पर था, और वह मेरे पीछे-एक हाथ मेरे कन्धे पर और दूसरा सिर पर। सिर के बालों को सहलाती हुई, कुछ गुनगुनाती हुई खड़ी थी। मैं तन्मय होकर ‘हैपिनेस इन मैरिज’ नामक पुस्तक पढ़ रहा था। सहसा उसका हाथ मेरी आँखों पर से फिर गया। मैंने उसे पकड़ लिया। अपनी नशीली आँखें मुख पर दौड़ाती हुई अस्तव्यस्त हो अपना सारा भार मेरी कुर्सी के हत्थों पर डाल दिया। मैं कुर्सी को टेकता सीधा हो गया। साहसा घर डोल गया और एक…
- उसका हृदय मेरे हृदय से मिल गया था।
- भूकम्प क्या था – प्रलय का दूसरा रूप। भाग्य से ही हम बचे। हम अच्छे हो चुके थे। वैसी ही सन्ध्या थी। वह मेरे पास आयी। सामने की कुर्सी पर बैठ गयी। उसकी आँखों में प्रेम था, पवित्रता थी। बोली- ‘प्रमोद, मैं एक बात तुम से पूछूँ?’ मैंने उसका कोमल हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, ‘मेरे लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है, अनिल।’ वह बोली, ‘प्रमोद, तुम जानते हो देश कैसा दुखी है, त्रस्त है। हम अच्छे हो गये हैं। हमारा उपयोग होना चाहिए, प्रमोद।’ मैं फूट पड़ा।
‘तुम्हारा हृदय कितना उच्च है, कितनी सहानुभति से भरा है अनिल। हम कवि लोग अपनी भावनाओं को ही घूमाने-फिराने में लगे रहते हैं। क्या किसी कवि को तुमने कार्य-कवि होते भी देखा है। होते भी होंगे पर बहुत कम। हमारी कल्पनाएँ क्या भूकम्प त्रस्त लोगों को कुछ भी सुख पहुँचा सकती हैं। नहीं, अनिल, नहीं।’
‘प्रमोद, शान्त हो। तुम नहीं, मैं तो हूँ। मुझे आज्ञा दो प्रमोद, कि मैं विश्व-सेवा में उपस्थित होऊँ।’
वह एकदम खड़ी हो गयी। मैं भी एकदम खड़ा हो गया। मैंने आवेश से कहा- ‘अनिल जाओ। मैं नहीं आ सकता – तुम जाओ। मेरी हृदय-कामने, तुम जाओ।’
‘जाती हूँ, प्रमोद। तुम सच्चे कवि हो। तुम मेरे सच्चे हृदयेश्वर हो। और हो तुम सौन्दर्य के सच्चे उपासक-प्रमोद यही सौन्दर्य है।’
उस दिन की स्मृति दौड़ती हुई आयी। मैंने अपने को स्वर्ग में पाया। पुलकित हो गया। समय और स्थिति की परवाह न कर मैंने उसे हृदय से चिपका लिया। ऑंखों में अश्रु थे और अधरों पर सुधा।
यह था मेरा प्रथम प्रणय-चुम्बन।
(माधव कॉलेज मैगजीन में 1935 में तथा 27 दिसंबर 1992 के दैनिक भास्कर में पुनः प्रकाशित)
स्रोत : शेष-अशेष, संपादक : अशोक वाजपेयी, रमेश गजानन मुक्तिबोध, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
क्लाड ईथरली – कहानी
मैं सड़क पार कर लेता हूँ। जंगली, बेमहक लेकिन खूबसूरत विदेशी फूलों के नीचे ठहर-सा जाता हूँ कि जो फूल, भीत के पासवाले अहाते की आदमकद दीवार के ऊपर फैले, सड़क के बाजू पर बाँहें बिछा कर झुक गए हैं। पता नहीं कैसे, किस साहस से व क्यों उसी अहाते के पास बिजली का ऊँचा खंभा – जो पाँच-छह दिशाओं में जानेवाली सूनी सड़कों पर तारों की सीधी लकीरें भेज रहा है – मुझे दीखता है और एकाएक खयाल आता है कि दुमंजिला मकानों पर चढ़ने की एक ऊँची निसैनी उसी से टिकी हुई है। शायद, ऐसे मकानों की लंब-तड़ंग भीतों की रचना अभी भी पुराने ढंग से होती है।
सहज, जिज्ञासावश देखें, कहाँ, क्या होता है। दृश्य कौन-से, कौन-से दिखाई देते हैं! मैं उस निसैनी पर चढ़ जाता हूँ और सामनेवाली पीली ऊँची भीत के नीली फ्रेमवाले रोशनदान में से मेरी निगाहें पार निकल जाती हैं।
और, मैं स्तब्ध हो उठता हूँ।
छत से टँगे ढिलाई से गोल-गोल घूमते पंखे के नीचे, दो पीली स्फटिक-सी तेज आँखे और लंबी शलवटों-भरा तंग मोतिया चेहरा है जो ठीक उन्हीं ऊँचे रोशनदानों में से, भीतर से बाहर, पार जाने के लिए ही मानो अपनी दृष्टि केंद्रित कर रहा है। आँखों से आँखे लड़ पड़ती हैं। ध्यान से एक-दूसरे की ओर देखती है। स्तब्ध, एकाग्र!
आश्चर्य?
साँस के साथ शब्द निकले! ऐसी ही कोई आवाज उसने भी की होगी!
चेहरा बहुत बुरा नहीं है, अच्छा है, भला आदमी मालूम होता है। पैंट पर शर्ट ढीली पड़ गई है। लेकिन यह क्या!
मैं नीचे उतर पड़ता हूँ। चुपचाप रास्ता चलने लगता हूँ। कम-से-कम दो फर्लांग दूरी पर एक आदमी मिलता है। सिर्फ एक आदमी! इतनी बड़ी सड़क होने पर भी लोग नहीं! क्यों नहीं?
पूछने पर वह शख्स कहता है, शहर तो इस पार है, उस ओर है; वहीं कहीं इस सड़क पर बिल्डिंग का पिछवाड़ा पड़ता है। देखते नहीं हो!
मैंने उसका चेहरा देखा ध्यान से। बाईं और दाहिनी भौंहें नाक के शुरू पर मिल गई थीं। खुरदुरा चेहरा, पंजाबी कहला सकता था। वह नि:संदेह जनाना आदमी होने की संभावना रखता है! नारी तुल्य पुरुष, जिनका विकास किशोर काव्य में विशेषज्ञों का विषय है।
इतने में मैंने उससे स्वाभाविक रूप से, अति सहज बन कर पूछा, ‘यह पीली बिल्डिंग कौन-सी है।’ उसने मुझ पर अविश्वास करते हुए कहा, ‘जानते नहीं हो? यह पागलखाना है – प्रसिद्ध पागलखाना!’
‘अच्छा…!’ का एक लहरदार डैश लगा कर मैं चुप हो गया और नीची निगाह किए चलने लगा।
और फिर हम दोनों के बीच दूरियाँ चौड़ी हो कर गोल होने लगीं। हमारे साथ हमारे सिफर भी चलने लगे।
अपने-अपने शून्यों की खिड़कियाँ खोल कर मैंने – हम दोनों ने एक-दूसरे की तरफ देखा कि आपस में बात कर सकते हैं या नहीं! कि इतने में उसने मुझसे पूछा, ‘आप क्या काम करते हैं?’
मैंने झेंप कर कहा, ‘मैं? उठाईगिरा समझिए।’
‘समझें क्यों? जो हैं सो बताइए।’
‘पता नहीं क्यों, मैं बहुत ईमानदारी की जिंदगी जीता हूँ; झूठ नहीं बोला करता, पर-स्त्री को नहीं देखता; रिश्वत नहीं लेता; भ्रष्टाचारी नहीं हूँ; दगा या फरेब नहीं करता; अलबत्ता कर्ज मुझ पर जरूर है जो मैं चुका नहीं पाता। फिर भी कमाई की रकम कर्ज में जाती है। इस पर भी मैं यह सोचता हूँ कि बुनियादी तौर से बेईमान हूँ। इसीलिए, मैंने अपने को पुलिस की जबान में उठाईगिरा कहा। मैं लेखक हूँ। अब बताइए, आप क्या हैं?’
वह सिर्फ हँस दिया। कहा कुछ नहीं। जरा देर से उसका मुँह खुला। उसने कहा, ‘मैं भी आप ही हूँ।’
एकदम दब कर मैंने उससे शेकहैंड किया (दिल में भीतर से किसी ने कचोट लिया। हाल ही में निसैनी पर चढ़ कर मैंने उस रोशनदान में से एक आदमी की सूरत देखी थी; वह चोरी नहीं तो क्या था। संदिग्धावस्था में उस साले ने मुझे देख लिया!)
‘बड़ी अच्छी बात है। मुझे भी इस धंधे में दिलचस्पी है, हम लेखकों का पेशा इससे कुछ मिलता-जुलता है।’
इतने में भीमाकार पत्थरों की विक्टोरियन बिल्डिंग के दृश्य दूर से झलक रहे थे। हम खड़े हो गए हैं। एक बड़े-से पेड़ के नीचे पान की दुकान थी वहाँ। वहाँ एक सिलेटी रंग की औरत मिस्सी और काजल लगाए हुए बैठी हुई थी।
मेरे मुँह से अचानक निकल पड़ा, ‘तो यहाँ भी पान की दुकान है?’
उसने सिर्फ इतना ही कहा, ‘हाँ, यहाँ भी।’
और मैं उन अध-विलायती नंगी औरतों की तस्वीरें देखने लगा जो उस दुकान की शौकत को बढ़ा रही थीं।
दुकान में आईना लगा था। लहर थीं धुँधली, पीछे के मसाले के दोष से। ज्यों ही उसमें मैं अपना मुँह देखता, बिगड़ा नजर आता। कभी मोटा, लंबा, तो कभी चौड़ा। कभी नाक एकदम छोटी, तो एकदम लंबी और मोटी! मन में वितृष्णा भर उठी। रास्ता लंबा था, सूनी दुपहर। कपड़े पसीने से भीतर चिपचिपा रहे थे। ऐसे मौके पर दो बातें करनेवाला आदमी मिल जाना समय और रास्ता कटने का साधन होता है।
उससे वह औरत कुछ मजाक करती रही। इतने में चार-पाँच आदमी और आ गए। वे सब घेरे खड़े रहे। चुपचाप कुछ बातें हुईं।
मैंने गौर नहीं किया। मैं इन सब बातों से दूर रहता हूँ। जो सुनाई दिया उससे यह जाहिर हुआ कि वे या तो निचले तबके में पुलिस के इनफॉर्मर्स हैं या ऐसे ही कुछ!
हम दोनों ने अपने-अपने और एक-दूसरे के चेहरे देखे! दोनों खराब नजर आए। दोनों रूप बदलने लगे! दोनों हँस पड़े और यही मजाक चलता रहा।
पान खा कर हम लोग आगे बढ़े। पता नहीं क्यों मुझे अपने अजनबी साथी के जनानेपन में कोई ईश्वरीय अर्थ दिखाई दिया। जो आदमी आत्मा की आवाज दाब देता है, विवेक-चेतना को घुटाले में डाल देता है, उसे क्या कहा जाए! वैसे, वह शख्स भला मालूम होता था। फिर, क्या कारण है कि उसने यह पेशा अख्तियार किया! साहसी, हाँ, कुछ साहसिक लोग पत्रकार या गुप्तचर या ऐसे ही कुछ हो जाते हैं, अपनी आँखों में महत्वपूर्ण बनने के लिए, अस्तित्व की तीखी संवेदनाएँ अनुभव करने और करते रहने के लिए!
लेकिन, प्रश्न यह है कि वे वैसा क्यों करते हैं! किसी भीतरी न्यूनता के भाव पर विजय प्राप्त करने का यह एक तरीका भी हो सकता है। फिर भी, उसके दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं! यही पेशा क्यों? इसलिए, उसमें पेट और प्रवृत्ति का समन्वय है! जो हो, इस शख्स का जनानापन खास मानी रखता है!
हमने वह रास्ता पार कर लिया और अब हम फिर से फैशनेबल रास्ते पर आ गए, जिसके दोनों ओर युकलिप्टस के पेड़ कतार बाँधे खड़े थे। मैंने पूछा, ‘यह रास्ता कहाँ जाता है?’ उसने कहा, ‘पागलखाने की ओर ।’ मैं जाने क्यों सन्नाटे में आ गया।
विषय बदलने के लिए मैंने कहा, ‘तुम यह धंधा कब से कर रहे हो?’
उसने मेरी तरफ इस तरह देखा मानो यह सवाल उसे नागवार गुजरा हो।
मैं कुछ नहीं बोला। चुपचाप चला, चलता रहा। लगभग पाँच मिनट बाद जब हम उस भैरों के गेरूए, सुनहले, पन्नी जड़े पत्थर तक पहुँच गए, जो इस अत्याधुनिक युग में एक तार के खंभे के पास श्रद्धापूर्वक स्थापित किया गया था, उसने कहा, ‘मेरा किस्सा मुख्तसर है। लाज-शरम दिखावे की चीजें हैं। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए कह रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़े करोड़पति सेठ का लड़का हूँ। उनके घर में जो काम करनेवालियाँ हुआ करती थीं, उनमें-से एक मेरी माँ है, जो अभी भी वहीं हैं। मैं, घर से दूर पाला-पोसा गया, मेरे पिता के खर्चे से! माँ पिलाने आती। उसी के कहने से मैंने बमुश्किल तमाम मैट्रिक किया। फिर, किसी सिफारिश से सी.आई.डी. की ट्रेनिंग में चला गया। तबसे यही काम कर रहा हूँ। बाद में पता चला कि वहाँ का खर्च भी वही सेठ देता है। उसका हाथ मुझ पर अभी तक है। तुम उठाईगिरे हो, इसलिए कहा! अरे! वैसे तो तुम लेखक-वेखक भी हो। बहुत-से लेखक और पत्रकार इनफॉर्मर हैं! तो, इसलिए, मैंने सोचा, चलो अच्छा हुआ। एक साथी मिल गया।’
उस आदमी में मेरी दिलचस्पी बहुत बढ़ गई। डर भी लगा। घृणा भी हुई। किस आदमी से पाला पड़ा। फिर भी, उस अहाते पर चढ़ कर मैं झाँक चुका था। इसलिए एक अनदिखती जंजीर से बँध तो गया ही था।
उस जनाने ने कहना जारी रखा, ‘उस पागलखाने में कई ऐसे लोग डाल दिए गए हैं जो सचमुच आज की निगाह से बड़े पागल हैं। लेकिन उन्हें पागल कहने की इच्छा रखने के लिए आज की निगाह होना जरूरी है।’
मैंने उकसाते हुए कहा, ‘आज की निगाह से क्या मतलब?’
उसने भौंहें समेट लीं। मेरी आँखों में आँखे डाल कर उसने कहना शुरू किया, ‘जो आदमी आत्मा की आवाज कभी-कभी सुन लिया करता है और उसे बयान करके उससे छुट्टी पा लेता है, वह लेखक हो जाता है। आत्मा की आवाज को लगातार सुनता है, और कहता कुछ नहीं, वह भोला-भाला सीधा-सादा बेवकूफ है। जो उसकी आवाज बहुत ज्यादा सुना करता है और वैसा करने लगता है, वह समाज-विरोधी तत्वों में यों ही शामिल हो जाया करता है। लेकिन जो आदमी आत्मा की आवाज जरूरत से ज्यादा सुन करके हमेशा बेचैन रहा करता है और उस बेचैनी में भीतर के हुक्म का पालन करता है, वह निहायत पागल है। पुराने जमाने में संत हो सकता था। आजकल उसे पागलखाने में डाल दिया जाता है।’
मुझे शक हुआ कि मैं किसी फैंटेसी में रह रहा हूँ। यह कोई ऐसा-वैसा कोई गुप्तचर नहीं है। या तो यह खुद पागल है या कोई पहुँचा हुआ आदमी है! लेकिन वह पागल भी नहीं है न पहुँचा हुआ है। वह तो सिर्फ जनाना आदमी है या वैज्ञानिक शब्दावली प्रयोग करूँ तो यह कहना होगा कि वह है तो जवान-पट्ठा लेकिन उसमें जो लचक है वह औरत के चलने की याद दिलाती है!
मैंने उससे पूछा, ‘तुमने कहीं ट्रेनिंग पाई है?’
‘सिर्फ तजुर्बे से सीखा है! मुझे इनाम भी मिला है।’
मैंने कहा, ‘अच्छा!’
और मैं जिज्ञासा और कुतूहल से प्रेरित हो कर उसकी अंधकारपूर्ण थाहों में डूबने का प्रयत्न करने लगा।
किंतु उसने सिर्फ मुस्करा दिया! तब मुझे वह ऐसा लगा मानो वह अज्ञात साइंस के गणितिक सूत्र की अंक-राशि हो, जिसका मतलब तो कुछ जरूर होता है लेकिन समझ में नहीं आता।
मन में विचारों की पंक्तियों की पंक्तियाँ बनती गईं। पंक्तियों पर पंक्तियाँ। शायद उसे भी महसूस हुआ होगा! और जब दोनों के मन में चार-चार पंक्तियाँ बन गईं कि इस बीच उसने कहा, ‘तुम क्यों नहीं यह धंधा करते?’
मैं हतप्रभ हो गया। यह एक विलक्षण विचार था! मुझे मालूम था कि धंधा पैसों के लिए किया जाता है। आजकल बड़े-बड़े शहरों के मामूली होटलों में जहाँ दस-पाँच आदमी तरह-तरह की गप लड़ाते हुए बैठते हैं, उनकी बातें सुन कर, अपना अंदाज जमाने के लिए, कई भीतरी सूची-भेदक-प्रवेशक आँखे भी सुनती बैठती रहती हैं। यह मैं सब जानता हूँ। खुद के तजुर्बे से बता सकता हूँ। लेकिन, फिर भी, उस आदमी की हिम्मत तो देखिए कि उसने कैसा पेचीदा सवाल किया!
आज तक किसी आदमी ने मुझसे इस तरह का सवाल न किया था। जरूर मुझमें ऐसा कुछ है कि जिसे मैं विशेष योग्यता कह सकता हूँ। मैंने अपने जीवन में जो शिक्षा और अशिक्षा प्राप्त की, स्कूलों-कॉलेजों में में जो विद्या और अविद्या उपलब्ध की, जो कौशल और अकौशल प्राप्त की, उसने – मैं मानूँ या न मानूँ – भद्रवर्ग का ही अंग बना दिया है। हाँ, मैं उस भद्रवर्ग का अंग हूँ कि जिसे अपनी भद्रता के निर्वाह के लिए अब आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, और यह भाव मन में जमा रहता है कि नाश सन्निकट है। संक्षेप में, मैं सचेत व्यक्ति हूँ, अति-शिक्षित हूँ, अति-संस्कृत हूँ। लेकिन चूँकि अपनी इस अतिशिक्षा और अतिसंस्कृति के सौष्ठव को उद्घाटित करते रहने के लिए, जो स्निग्ध प्रसन्नमुख चाहिए, वह न होने से मैं उठाईगिरा भी लगता हूँ – अपने-आप को!
तो मेरी इस महक को पहचान उस अद्भुत व्यक्ति ने मेरे सामने जो प्रस्ताव रखा, उससे मैं अपने-आप से एकदम सचेत हो उठा! क्या हर्ज है? इनकम का एक खासा जरिया यह भी तो हो सकता है।
मैंने बात पलट कर उससे पूछा, ‘तो हाँ, तुम उस पागलखाने की बात कह रहे थे। उसका क्या?’
मैंने गरदन नीचे डाल ली। कानों में अविराम शब्द-प्रवाह गतिमान हुआ। मैं सुनता गया। शायद वह उसके वक्तव्य की भूमिका रही होगी। इस बीच मैंने उससे टोक कर पूछा, ‘तो उसका नाम क्या है?
‘क्लॉड ईथरली!’
‘क्या वह रोमन कैथलिक है – आदिवासी इसाई है?’
उसने नाराज हो कर कहा, ‘तो अब तक तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे?’
मैंने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी एक-एक बात दिल में उतर रही थी। फिर भी उसके चेहरे के भाव से पता चला कि उसे मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, ‘क्लॉड ईथरली वह अमरीकी विमान चालक है, जिसने हिरोशिमा पर बम गिराया था।’
मुझे आश्चर्य का एक धक्का लगा। या तो वह पागल है, या मैं! मैंने उससे पूछा, ‘तो उससे क्या होता है?’
अब उसने बहुत ही नाराज हो कर कहा, ‘अबे बेवकूफ! नेस्तनाबूद हुए हिरोशिमा की बदरंग और बदसूरत, उदास और गमगीन जिंदगी की सरदारत करनेवाले मेयर को वह हर माह चेक भेजता रहा जिससे कि उन पैसों से दीन-हीनों को सहायता तो पहुँचे ही; उसने जो भयानक पाप किया है वह भी कुछ कम हो!’
मैंने उसके चेहरे का अध्ययन करना शुरू किया। उसकी वे खुरदुरी घनी मोटी भौंहें नाक के पास आ मिलती थीं। कड़े बालों की तेज रेजर से हजामत किया हुआ उसका वह हरा-गोरा चेहरा, सीधी-मोटी नाक और मजाकिया होठ और गमगीन आँखे, जिस्म की जनाना लचक, डबल ठुड्डी, जिसके बीच में हलका-सा गड्ढा!
यह कौन शख्स है, जो मुझसे इस तरह बात कर रहा है। लगा कि मैं सचमुच इस दुनिया में नहीं रह रहा हूँ, उससे कोई दो सौ मील ऊपर आ गया हूँ, जहाँ आकाश, चाँद-तारे, सूरज सभी दिखाई देते हैं। रॉकेट उड़ रहे हैं। आते हैं, जाते हैं और पृथ्वी एक चौड़े-नीले गोल जगत-सी दिखाई दे रही है, जहाँ हम किसी एक देश के नहीं हैं, सभी देशों के हैं। मन में एक भयानक उद्वेगपूर्ण भावहीन चंचलता है! कुल मिला कर, पल-भर यही हालत रही। लेकिन वह पल बहुत ही घनघोर था। भयावह और संदिग्ध! और उसी पल से अभिभूत हो कर मैंने उससे पूछा, ‘तो क्या हिरोशिमा वाला क्लॉड ईथरली इस पागलखाने में है।’
वह हाथ फैला कर उँगलियों से उस पीली बिल्डिंग की तरफ इशारा कर रहा था, जिसके अहाते की दीवार पर चढ़ कर मेरी आँखों ने रोशनदान पार करके उन तेज आँखों को देखा था, जो उसी रोशनदान में से गुजर कर बाहर जाना चाहती हैं। तो, अगर मैं जस जनाने लचकदार शख्स पर यकीन करूँ तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरी देखी वे आँखे और किसी की नहीं, खास क्लॉड ईथरली की ही थीं। लेकिन यह कैसे हो सकता है!
उसने मेरी बात ताड़ कर कहा, ‘हाँ, वह क्लॉड ईथरली ही था।’
मैंने चिढ़ कर कहा, ‘तो क्या यह हिंदुस्तान नहीं है। हम अमेरिका में ही रह रहे हैं?’
उसने मानो मेरी बेवकूफी पर हँसी का ठहाका मारा, कहा, ‘भारत के हर बड़े नगर में एक-एक अमेरिका है! तुमने लाल ओठवाली चमकदार, गोरी-सुनहली औरतें नहीं देखी, उनके कीमती कपड़े नहीं देखे! शानदार मोटरों में घूमने वाले अशिक्षित लोग नहीं देखे! नफीस किस्म की वेश्यावृत्ति नहीं देखी! सेमिनार नहीं देखे! एक जमाने में हम लंदन जाते थे और इंग्लैंड रिर्टन कहलाते थे और आज वाशिंगटन जाते हैं। अगर हमारा बस चले और आज हम सचमुच उतने ही धनी हों और हमारे पास उतने ही एटम बम और हाइड्रोजन बम हों और रॉकेट हों तो फिर क्या पूछना! अखबार पढ़ते हो कि नहीं?’
मैंने कहा, ‘हाँ।’
तो तुमने मैकमिलन की वह तकरीर भी पढ़ी होगी जो उसने… को दी थी। उसने क्या कहा था? यह देश, हमारे सैनिक गुट में तो नहीं है, किंतु संस्कृति और आत्मा से हमारे साथ है। क्या मैकमिलन सफेद झूठ कह रहा था? कतई नहीं। वह एक महत्वपूर्ण तथ्य पर प्रकाश डाल रहा था।
और अगर यह सच है तो यह भी सही है कि उनकी संस्कृति और आत्मा का संकट हमारी संस्कृति और आत्मा का संकट है! यही कारण है कि आजकल के लेखक और कवि अमरीकी, ब्रिटिश तथा पश्चिम यूरोपीय साहित्य तथा विचारधाराओं में गोते लगाते हैं और वहाँ से अपनी आत्मा को शिक्षा और संस्कृति प्रदान करते हैं! क्या यह झूठ है। और हमारे तथाकथित राष्ट्रीय अखबार और प्रकाशन-केंद्र! वे अपनी विचारधारा और दृष्टिकोण कहाँ से लेते हैं?’
यह कह कर वह जोर से हँस पड़ा और हँसी की लहरों में उसका जिस्म लचकने लगा।
उसने कहना जारी रखा, ‘क्या हमने इंडोनेशियाई या चीनी या अफ्रीकी साहित्य से प्रेरणा ली है या लुमुंबा के काव्य से? छि: छि:! वह जानवरों का, चौपायों का साहित्य है! और रूस का? अरे! यह तो स्वार्थ की बात है! इसका राज और ही है। रूस से हम मदद चाहते हैं, लेकिन डरते भी हैं।’
‘छोड़ो! तो मतलब यह है कि अगर उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति है, उनकी आत्मा हमारी आत्मा और उनका संकट हमारा संकट है – जैसा कि सिद्ध है – जरा पढ़ो अखबार, करो बातचीत अंगरेजीदाँ फर्राटेबाज लोगों से – तो हमारे यहाँ भी हिरोशिमा पर बम गिरानेवाला विमान चालक क्यों नहीं हो सकता और हमारे यहाँ भी संप्रदायवादी, युद्धवादी लोग क्यों नहीं हो सकते! मुख्तसर किस्सा यह है कि हिंदुस्तान भी अमेरिका ही है।’
मुझे पसीना छूटने लगा। फिर भी मन यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि भारत अमेरिका ही है और यह कि क्लॉड ईथरली उसी पागलखाने में रहते हैं – उसी पागलखाने में रहता है! मेरी आँखों में संदेह, अविश्वास, भय और आशंका की मिली-जुली चमक जरूर रही होगी, जिसको देख कर वह बुरी तरह हँस पड़ा। और उसने मुझे एक सिगरेट दी।
एक पेड़ के नीचे खड़े हो कर हम दोनों बात करते हुए नीचे एक पत्थर पर बैठ गए। उसने कहा, ‘देखा नहीं! ब्रिटिश-अमरीकी या फ्रांसीसी कविता में जो मूड्स, जो मनःस्थितियाँ रहती हैं – बस वे ही हमारे यहाँ भी हैं, लाई जाती हैं। सुरुचि और आधुनिक भावबोध का तकाजा है कि उन्हें लाया जाया क्यों? इसलिए कि वहाँ औद्योगिक सभ्यता है, हमारे यहाँ भी। मानो कि कल-कारखाने खोले जाने से आदर्श ओर कर्तव्य बदल जाते हों।’
मैंने नाराज हो कर सिगरेट फेंक दी। उसके सामने हो लिया। शायद, उस समय मैं उसे मारना चाहता था। हाथापाई करना चाहता था। लेकिन वह व्यंग्य-भरे चेहरे से हँस पड़ा और उसकी आँखे ज्यादा गमगीन हो गईं।’
उसने कहा, ‘क्लॉड ईथरली एक विमान चालक था! उसके एटमबम से हिरोशिमा नष्ट हुआ। वह अपनी कारगुजारी देखने उस शहर गया। उस भयानक, बदरंग, बदसूरत कटी लोथों के शहर को देख कर उसका दिल टुकड़े-टुकड़े हो गया। उसको पता नहीं था कि उसके पास ऐसा हथियार है और उस हथियार का यह अंजाम होगा। उसके दिल में निरपराध जनों के प्रेतों, शवों, लोथों, लाशों के कटे-पिटे चेहरे तैरने लगे। उसके हृदय में करुणा उमड़ आई। उधर, अमरीकी सरकार ने उसे इनाम दिया। वह ‘वॉर हीरो’ हो गया। लेकिन उसकी आत्मा कहती थी कि उसने पाप किया, जघन्य पाप किया है। उसे दंड मिलना ही चाहिए। नहीं। लेकिन उसका देश तो उसे हीरो मानता था। अब क्या किया जाय। उसने सरकारी नौकरी छोड़ दी। मामूली से मामूली काम किया। लेकिन, फिर भी वह ‘वॉर हीरो’ था, महान था। क्लॉड ईथरली महानता नहीं, दंड चाहता था, दंड!’
‘उसने वारदातें शुरू कीं जिससे कि वह गिरफ्तार हो सके और जेल में डाला जा सके। किंतु प्रमाण के अभाव में वह हर बार छोड़ दिया गया। उसने घोषित किया कि वह पापी है, पापी है, उसे दंड मिलना चाहिए, उसने निरपराध जनों की हत्या की है, उसे दंड दो। हे ईश्वर! लेकिन अमरीकी व्यवस्था उसे पाप नहीं, महान कार्य मानती थी। देश-भक्ति मानती थी। जब उसने ईथरली की ये हरकतें देखीं तो उसे पागलखाने में डाल दिया। टेक्सॉस प्रांत में वायो नाम की एक जगह है – वहाँ उसका दिमाग दुरुस्त करने के लिए उसे डाल दिया गया। वहाँ वह चार साल तक रहा, लेकिन उसका पागलपन दुरुस्त नहीं हो सका।’
‘चार साल बाद वह वहाँ से छूटा तो उसे राय.एल. मैनटूथ नाम का एक गुंडा मिला। उसकी मदद से उसने डाकघरों पर धावा मारा। आखिर मय साथी के वह पकड़ लिया गया। मुकदमा चला। कोई फायदा नहीं। जब यह मालूम हुआ कि वह कौन है और क्या चाहता है तो उसे तुरंत छोड़ दिया गया। उसके बाद, उसने डल्लॉस नाम की एक जगह के कैशियर पर सशस्त्र आक्रमण किया। परिणाम कुछ नहीं निकला, क्योंकि बड़े सैनिक अधिकारियों को यह महसूस हुआ कि ऐसे ‘प्रख्यात युद्ध वीर’ को मामूली उचक्का और चोर कह कर उसकी बदनामी न हो। इसलिए उसके उस प्राप्त पद की रक्षा करने के लिए, उसे फिर से पागलखाने में डाल दिया गया।’
‘यह है क्लॉड ईथरली! ईथरली की ईमानदारी पर अविश्वास करने की किसी को शंका ही नहीं रही। उसकी जीवन-कथा की फिल्म बनाने का अधिकार खरीदने के लिए कंपनी ने उसे एक लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा। उसने कतई इनकार कर दिया। उसके इस अस्वीकार से सबके सामने यह जाहिर हो गया कि वह झूठा और फरेबी नहीं है। वह बन नहीं रहा।’
‘कौन नहीं जानता कि क्लॉड ईथरली अणु युद्ध का विरोध करनेवाली आत्मा की आवाज का दूसरा नाम है। हाँ! ईथरली मानसिक रोगी नहीं है। आध्यात्मिक अशांति का, आध्यात्मिक उद्विग्नता का ज्वलंत प्रतीक है। क्या इससे तुम इनकार करते हो?’
उसके हाथ की सिगरेट कभी की नीचे गिर चुकी थी। वह जनाना आदमी तमतमा उठा था। चेहरे पर बेचैनी की मलिनता छाई थी।
वह कहता गया, ‘इस आध्यात्मिक अशांति, इस आध्यात्मिक उद्विग्नता को समझने वाले लोग कितने हैं! उन्हें विचित्र, विलक्षण, विक्षिप्त कह कर पागलखाने में डालने की इच्छा रखने वाले लोग न जाने कितने हैं! इसलिए पुराने जमाने में हमारे बहुतेरे विद्रोही संतों को भी पागल कहा गया। आज भी बहुतों को पागल कहा जाता है। अगर वह बहुत तुच्छ हुए तो सिर्फ उनकी उपेक्षा की जाती है, जिससे कि उनकी बात प्रकट न हो और फैल न जाए।’
‘हमारे अपने-अपने मन-हृदय-मस्तिष्क में ऐसा ही एक पागलखाना है, जहाँ हम उन उच्च पवित्र और विद्रोही विचारों और भावों को फेंक देते हैं, जिससे कि धीरे-धीरे या तो वह खुद बदल कर समझौतावादी पोशाक पहन सभ्य भद्र हो जाए यानी दुरुस्त हो जाए या उसी पागलखाने में पड़ा रहे!’
मैं हतप्रभ तो हो ही गया! साथ-ही-साथ, उसकी इस कहानी पर मुग्ध भी। उस जीवन-कथा से अत्यधिक प्रभावित हो कर मैंने पूछा, ‘तो क्या यह कहानी सच्ची है?’
उसने जवाब दिया, भई वाह! अमरीकी साहित्य पढ़ते हो कि नहीं? ब्रिटिश भी नहीं! तो क्या पढ़ते हो खाक!… अरे भाई रूस पर तो अनेक भाषाओं में कई पुस्तकें निकल गई हैं। तो क्या पत्थर जानकारी रखते हो। विश्वास न हो, तो खंडन करो, जाओ टटोलो। और, इस बीच में इसी पागलखाने की सैर करवा लाता हूँ।’
मैंने हाथ हिला कर इनकार करते हुए कहा, ‘नहीं मुझे नहीं जाना।’
क्यों नहीं? उसने झिड़क कर कहा, ‘आजकल हमारे अवचेतन में हमारी आत्मा आ गई है, चेतन में स्व-हित और अधिचेतन में समाज से सामंजस्य का आदर्श भले ही वह बुरा समाज क्यों न हो? यही आज के जीवन-विवेक का रहस्य है।…’
‘तुमको वहाँ की सैर करनी होगी। मैं तुम्हें पागलखाने ले चल रहा हूँ, लेकिन पिछले दरवाजे से नहीं, खुले अगले से।’
रास्ते में मैंने उससे कहा, ‘मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि भारत अमेरिका है! तुम कुछ भी कहो! न वह कभी हो सकता है, न वह कभी होगा ही।’
इस बात को उसने उड़ा दिया। उसे चाहिए था कि वह उस बात का जवाब देता । उसने सिर्फ इतना कहा, ‘मुश्किल यह है कि तुम मेरी बात नहीं समझते।’ मैंने कहा, ‘कैसे?’
‘क्लॉड ईथरली हमारे यहाँ भले ही देह-रूप में न रहे, लेकिन आत्मा की वैसी बेचैनी रखने वाले लोग तो यहाँ रह ही सकते हैं।’
मैंने अविश्वास प्रकट करके उसके प्रति घृणा भाव व्यक्त करते हुए कहा, ‘यह भी ठीक नहीं मालूम होता।’
उसने कहा, ‘क्यों नहीं? देश के प्रति ईमानदारी रखनेवाले लोगों के मन में, व्यापक पापाचारों के प्रति कोई व्यक्तिगत भावना नहीं रहती क्या?’
‘समझा नहीं।’
‘मतलब यह कि ऐसे बहुतेरे लोग हैं जो पापाचार रूपी, शोषण रूपी डाकुओं को अपनी छाती पर बैठा समझते हैं। वह डाकू न केवल बाहर का व्यक्ति है, वह उनके घर का आदमी भी है। समझने की कोशिश करो!’
मैंने भौंहें उठा कर कहा, ‘तो क्या हुआ?’
‘यह कि उस व्यापक अन्याय को अनुभव करनेवाले किंतु उसका विरोध करनेवाले लोगों के अंत:करण में व्यक्तिगत पाप-भावना रहती ही है, रहनी चाहिए। ईथरली में और उनमें यह बुनियादी एकता और अभेद है।’
‘इससे सिद्ध क्या हुआ?’
‘इससे यह सिद्ध हुआ कि तुम-सरीखे सचेत जागरुक संवेदनशील जन क्लॉड ईथरली हैं।’
उसने मेरे दिल में खंजर मार दिया। हाँ, यह सच था! बिलकुल सच! अवचेतन के अँधेरे तहखाने में पड़ी हुई आत्मा का विद्रोह करती है। आत्मा पापाचारों के लिए, अपने-आपको जिम्मेदार समझती है। हाय रे! यह मेरा भी तो रोग रहा है।
मैंने अपने चेहरे को सख्त बना लिया। गंभीर हो कर कहा, ‘लेकिन ये सब बातें तुम मुझसे क्यों कह रहे हो?’
‘इसलिए कि मैं सी.आई.डी. हूँ और मैं तुम्हारी स्क्रीनिंग कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे विभाग से संबद्ध रहो। तुम इनकार क्यों करते हो। कहो कि यह तुम्हारी अंतरात्मा के अनुकूल है।’
‘तो क्या तुम मुझे टटोलने के लिए ये बातें कर रहे थे। और, तुम्हारी ये सब बातें बनावटी थीं! मेरे दिल का भेद लेने के लिए थीं? बदमाश!’
‘मैं तो सिर्फ तुम्हारे अनुकूल प्रसंगों की जो हो सकती थी, वही कर रहा था।’
कविताएँ
ओ सूर्य, तुझ तक पहुँचने की
ओ सूर्य, तुझ तक पहुँचने की
मूर्खता करना नहीं मैं चाहता ( मर जाऊँगा )
बस, इसलिए
उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया
के रूप में
मैं क्यों न चमगादड बनूं
व धरित्री की ओर मुँह कर
पैर तेरे ओर करता लटकता ही रहूँ
चूंकि हे मार्तण्ड तुझ तक पहुँचना बिलकुल असम्भव है
इसलिए अपमान करना सहज है वह आत्मसम्भव
चाँद का मुंह टेढ़ा
नगर के बीचों-बीच
आधी रात–अंधेरे की काली स्याह
शिलाओं से बनी हुई
भीतों और अहातों के, काँच-टुकड़े जमे हुए
ऊँचे-ऊँचे कन्धों पर
चांदनी की फैली हुई सँवलायी झालरें।
कारखाना–अहाते के उस पार
धूम्र मुख चिमनियों के ऊँचे-ऊँचे
उद्गार–चिह्नाकार–मीनार
मीनारों के बीचों-बीच
चांद का है टेढ़ा मुँह!!
भयानक स्याह सन तिरपन का चांद वह !!
गगन में करफ़्यू है
धरती पर चुपचाप ज़हरीली छिः थूः है !!
पीपल के खाली पड़े घोंसलों में पक्षियों के,
पैठे हैं खाली हुए कारतूस ।
गंजे-सिर चांद की सँवलायी किरनों के जासूस
साम-सूम नगर में धीरे-धीरे घूम-घाम
नगर के कोनों के तिकोनों में छिपे है !!
चांद की कनखियों की कोण-गामी किरनें
पीली-पीली रोशनी की, बिछाती है
अंधेरे में, पट्टियाँ ।
देखती है नगर की ज़िन्दगी का टूटा-फूटा
उदास प्रसार वह ।
समीप विशालकार
अंधियाले लाल पर
सूनेपन की स्याही में डूबी हुई
चांदनी भी सँवलायी हुई है !!
भीमाकार पुलों के बहुत नीचे, भयभीत
मनुष्य-बस्ती के बियाबान तटों पर
बहते हुए पथरीले नालों की धारा में
धराशायी चांदनी के होंठ काले पड़ गये
हरिजन गलियों में
लटकी है पेड़ पर
कुहासे के भूतों की साँवली चूनरी–
चूनरी में अटकी है कंजी आँख गंजे-सिर
टेढ़े-मुँह चांद की ।
बारह का वक़्त है,
भुसभुसे उजाले का फुसफुसाता षड्यन्त्र
शहर में चारों ओर;
ज़माना भी सख्त है !!
अजी, इस मोड़ पर
बरगद की घनघोर शाखाओं की गठियल
अजगरी मेहराब–
मरे हुए ज़मानों की संगठित छायाओं में
बसी हुई
सड़ी-बुसी बास लिये–
फैली है गली के
मुहाने में चुपचाप ।
लोगों के अरे ! आने-जाने में चुपचाप,
अजगरी कमानी से गिरती है टिप-टिप
फड़फड़ाते पक्षियों की बीट–
मानो समय की बीट हो !!
गगन में कर्फ़्यू है,
वृक्षों में बैठे हुए पक्षियों पर करफ़्यू है,
धरती पर किन्तु अजी ! ज़हरीली छिः थूः है ।
बरगद की डाल एक
मुहाने से आगे फैल
सड़क पर बाहरी
लटकती है इस तरह–
मानो कि आदमी के जनम के पहले से
पृथ्वी की छाती पर
जंगली मैमथ की सूँड़ सूँघ रही हो
हवा के लहरीले सिफ़रों को आज भी
बरगद की घनी-घनी छाँव में
फूटी हुई चूड़ियों की सूनी-सूनी कलाई-सी
सूनी-सूनी गलियों में
ग़रीबों के ठाँव में–
चौराहे पर खड़े हुए
भैरों की सिन्दूरी
गेरुई मूरत के पथरीले व्यंग्य स्मित पर
टेढ़े-मुँह चांद की ऐयारी रोशनी,
तिलिस्मी चांद की राज़-भरी झाइयाँ !!
तजुर्बों का ताबूत
ज़िन्दा यह बरगद
जानता कि भैरों यह कौन है !!
कि भैरों की चट्टानी पीठ पर
पैरों की मज़बूत
पत्थरी-सिन्दूरी ईट पर
भभकते वर्णों के लटकते पोस्टर
ज्वलन्त अक्षर !!
सामने है अंधियाला ताल और
स्याह उसी ताल पर
सँवलायी चांदनी,
समय का घण्टाघर,
निराकार घण्टाघर,
गगन में चुपचाप अनाकार खड़ा है !!
परन्तु, परन्तु…बतलाते
ज़िन्दगी के काँटे ही
कितनी रात बीत गयी
चप्पलों की छपछप,
गली के मुहाने से अजीब-सी आवाज़,
फुसफुसाते हुए शब्द !
जंगल की डालों से गुज़रती हवाओं की सरसर
गली में ज्यों कह जाय
इशारों के आशय,
हवाओं की लहरों के आकार–
किन्हीं ब्रह्मराक्षसों के निराकार
अनाकार
मानो बहस छेड़ दें
बहस जैसे बढ़ जाय
निर्णय पर चली आय
वैसे शब्द बार-बार
गलियों की आत्मा में
बोलते हैं एकाएक
अंधेरे के पेट में से
ज्वालाओं की आँत बाहर निकल आय
वैसे, अरे, शब्दों की धार एक
बिजली के टॉर्च की रोशनी की मार एक
बरगद के खुरदरे अजगरी तने पर
फैल गयी अकस्मात्
बरगद के खुरदरे अजगरी तने पर
फैल गये हाथ दो
मानो ह्रदय में छिपी हुई बातों ने सहसा
अंधेरे से बाहर आ भुजाएँ पसारी हों
फैले गये हाथ दो
चिपका गये पोस्टर
बाँके तिरछे वर्ण और
लाल नीले घनघोर
हड़ताली अक्षर
इन्ही हलचलों के ही कारण तो सहसा
बरगद में पले हुए पंखों की डरी हुई
चौंकी हुई अजीब-सी गन्दी फड़फड़
अंधेरे की आत्मा से करते हुए शिकायत
काँव-काँव करते हुए पक्षियों के जमघट
उड़ने लगे अकस्मात्
मानो अंधेरे के
ह्रदय में सन्देही शंकाओं के पक्षाघात !!
मद्धिम चांदनी में एकाएक एकाएक
खपरैलों पर ठहर गयी
बिल्ली एक चुपचाप
रजनी के निजी गुप्तचरों की प्रतिनिधि
पूँछ उठाये वह
जंगली तेज़
आँख
फैलाये
यमदूत-पुत्री-सी
(सभी देह स्याह, पर
पंजे सिर्फ़ श्वेत और
ख़ून टपकाते हुए नाख़ून)
देखती है मार्जार
चिपकाता कौन है
मकानों की पीठ पर
अहातों की भीत पर
बरगद की अजगरी डालों के फन्दों पर
अंधेरे के कन्धों पर
चिपकाता कौन है ?
चिपकाता कौन है
हड़ताली पोस्टर
बड़े-बड़े अक्षर
बाँके-तिरछे वर्ण और
लम्बे-चौड़े घनघोर
लाल-नीले भयंकर
हड़ताली पोस्टर !!
टेढ़े-मुँह चांद की ऐयारी रोशनी भी ख़ूब है
मकान-मकान घुस लोहे के गज़ों की जाली
के झरोखों को पार कर
लिपे हुए कमरे में
जेल के कपड़े-सी फैली है चांदनी,
दूर-दूर काली-काली
धारियों के बड़े-बड़े चौखट्टों के मोटे-मोटे
कपड़े-सी फैली है
लेटी है जालीदार झरोखे से आयी हुई
जेल सुझाती हुई ऐयारी रोशनी !!
अंधियाले ताल पर
काले घिने पंखों के बार-बार
चक्करों के मंडराते विस्तार
घिना चिमगादड़-दल भटकता है चारों ओर
मानो अहं के अवरुद्ध
अपावन अशुद्ध घेरे में घिरे हुए
नपुंसक पंखों की छटपटाती रफ़्तार
घिना चिमगादड़-दल
भटकता है प्यासा-सा,
बुद्धि की आँखों में
स्वार्थों के शीशे-सा !!
बरगद को किन्तु सब
पता था इतिहास,
कोलतारी सड़क पर खड़े हुए सर्वोच्च
गान्धी के पुतले पर
बैठे हुए आँखों के दो चक्र
यानी कि घुग्घू एक–
तिलक के पुतले पर
बैठे हुए घुग्घू से
बातचीत करते हुए
कहता ही जाता है–
“……मसान में……
मैंने भी सिद्धि की ।
देखो मूठ मार दी
मनुष्यों पर इस तरह……”
तिलक के पुतले पर बैठे हुए घुग्घू ने
देखा कि भयानक लाल मूँठ
काले आसमान में
तैरती-सी धीरे-धीरे जा रही
उद्गार-चिह्नाकार विकराल
तैरता था लाल-लाल !!
देख, उसने कहा कि वाह-वाह
रात के जहाँपनाह
इसीलिए आज-कल
दिल के उजाले में भी अंधेरे की साख है
रात्रि की काँखों में दबी हुई
संस्कृति-पाखी के पंख है सुरक्षित !!
…पी गया आसमान
रात्रि की अंधियाली सच्चाइयाँ घोंट के,
मनुष्यों को मारने के ख़ूब हैं ये टोटके !
गगन में करफ़्यू है,
ज़माने में ज़ोरदार ज़हरीली छिः थूः है !!
सराफ़े में बिजली के बूदम
खम्भों पर लटके हुए मद्धिम
दिमाग़ में धुन्ध है,
चिन्ता है सट्टे की ह्रदय-विनाशिनी !!
रात्रि की काली स्याह
कड़ाही से अकस्मात्
सड़कों पर फैल गयी
सत्यों की मिठाई की चाशनी !!
टेढ़े-मुँह चांद की ऐयारी रोशनी
भीमाकार पुलों के
ठीक नीचे बैठकर,
चोरों-सी उचक्कों-सी
नालों और झरनों के तटों पर
किनारे-किनारे चल,
पानी पर झुके हुए
पेड़ों के नीचे बैठ,
रात-बे-रात वह
मछलियाँ फँसाती है
आवारा मछुओं-सी शोहदों-सी चांदनी
सड़कों के पिछवाड़े
टूटे-फूटे दृश्यों में,
गन्दगी के काले-से नाले के झाग पर
बदमस्त कल्पना-सी फैली थी रात-भर
सेक्स के कष्टों के कवियों के काम-सी !
किंग्सवे में मशहूर
रात की है ज़िन्दगी !
सड़कों की श्रीमान्
भारतीय फिरंगी दुकान,
सुगन्धित प्रकाश में चमचमाता ईमान
रंगीन चमकती चीज़ों के सुरभित
स्पर्शों में
शीशों की सुविशाल झाँइयों के रमणीय
दृश्यों में
बसी थी चांदनी
खूबसूरत अमरीकी मैग्ज़ीन-पृष्ठों-सी
खुली थी,
नंगी-सी नारियों के
उघरे हुए अंगों के
विभिन्न पोज़ों मे
लेटी थी चांदनी
सफे़द
अण्डरवियर-सी, आधुनिक प्रतीकों में
फैली थी
चांदनी !
करफ़्यू नहीं यहाँ, पसन्दगी…सन्दली,
किंग्सवे में मशहूर रात की है ज़िन्दगी
अजी, यह चांदनी भी बड़ी मसखरी है !!
तिमंज़ले की एक
खिड़की में बिल्ली के सफे़द धब्बे-सी
चमकती हुई वह
समेटकर हाथ-पाँव
किसी की ताक में
बैठी हुई चुपचाप
धीरे से उतरती है
रास्तों पर पथों पर;
चढ़ती है छतों पर
गैलरी में घूम और
खपरैलों पर चढ़कर
नीमों की शाखों के सहारे
आंगन में उतरकर
कमरों में हलके-पाँव
देखती है, खोजती है–
शहर के कोनों के तिकोने में छुपी हुई
चांदनी
सड़क के पेड़ों के गुम्बदों पर चढ़कर
महल उलाँघ कर
मुहल्ले पार कर
गलियों की गुहाओं में दबे-पाँव
खुफ़िया सुराग़ में
गुप्तचरी ताक में
जमी हुई खोजती है कौन वह
कन्धों पर अंधेरे के
चिपकाता कौन है
भड़कीले पोस्टर,
लम्बे-चौड़े वर्ण और
बाँके-तिरछे घनघोर
लाल-नीले अक्षर ।
कोलतारी सड़क के बीचों-बीच खड़ी हुई
गान्धी की मूर्ति पर
बैठे हुए घुग्घू ने
गाना शुरु किया,
हिचकी की ताल पर
साँसों ने तब
मर जाना
शुरु किया,
टेलीफ़ून-खम्भों पर थमे हुए तारों ने
सट्टे के ट्रंक-कॉल-सुरों में
थर्राना और झनझनाना शुरु किया !
रात्रि का काला-स्याह
कन-टोप पहने हुए
आसमान-बाबा ने हनुमान-चालीसा
डूबी हुई बानी में गाना शुरु किया ।
मसान के उजाड़
पेड़ों की अंधियाली शाख पर
लाल-लाल लटके हुए
प्रकाश के चीथड़े–
हिलते हुए, डुलते हुए, लपट के पल्लू ।
सचाई के अध-जले मुर्दों की चिताओं की
फटी हुई, फूटी हुई दहक में कवियों ने
बहकती कविताएँ गाना शुरु किया ।
संस्कृति के कुहरीले धुएँ से भूतों के
गोल-गोल मटकों से चेहरों ने
नम्रता के घिघियाते स्वांग में
दुनिया को हाथ जोड़
कहना शुरु किया–
बुद्ध के स्तूप में
मानव के सपने
गड़ गये, गाड़े गये !!
ईसा के पंख सब
झड़ गये, झाड़े गये !!
सत्य की
देवदासी-चोलियाँ उतारी गयी
उघारी गयीं,
सपनों की आँते सब
चीरी गयीं, फाड़ी गयीं !!
बाक़ी सब खोल है,
ज़िन्दगी में झोल है !!
गलियों का सिन्दूरी विकराल
खड़ा हुआ भैरों, किन्तु,
हँस पड़ा ख़तरनाक
चांदनी के चेहरे पर
गलियों की भूरी ख़ाक
उड़ने लगी धूल और
सँवलायी नंगी हुई चाँदनी !
और, उस अँधियाले ताल के उस पार
नगर निहारता-सा खड़ा है पहाड़ एक
लोहे की नभ-चुम्भी शिला का चबूतरा
लोहांगी कहाता है
कि जिसके भव्य शीर्ष पर
बड़ा भारी खण्डहर
खण्डहर के ध्वंसों में बुज़ुर्ग दरख़्त एक
जिसके घने तने पर
लिक्खी है प्रेमियों ने
अपनी याददाश्तें,
लोहांगी में हवाएँ
दरख़्त में घुसकर
पत्तों से फुसफुसाती कहती हैं
नगर की व्यथाएँ
सभाओं की कथाएँ
मोर्चों की तड़प और
मकानों के मोर्चे
मीटिंगों के मर्म-राग
अंगारों से भरी हुई
प्राणों की गर्म राख
गलियों में बसी हुई छायाओं के लोक में
छायाएँ हिलीं कुछ
छायाएँ चली दो
मद्धिम चांदनी में
भैरों के सिन्दूरी भयावने मुख पर
छायीं दो छायाएँ
छरहरी छाइयाँ !!
रात्रि की थाहों में लिपटी हुई साँवली तहों में
ज़िन्दगी का प्रश्नमयी थरथर
थरथराते बेक़ाबू चांदनी के
पल्ले-सी उड़ती है गगन-कंगूरों पर ।
पीपल के पत्तों के कम्प में
चांदनी के चमकते कम्प से
ज़िन्दगी की अकुलायी थाहों के अंचल
उड़ते हैं हवा में !!
गलियों के आगे बढ़
बगल में लिये कुछ
मोटे-मोटे कागज़ों की घनी-घनी भोंगली
लटकाये हाथ में
डिब्बा एक टीन का
डिब्बे में धरे हुए लम्बी-सी कूँची एक
ज़माना नंगे-पैर
कहता मैं पेण्टर
शहर है साथ-साथ
कहता मैं कारीगर–
बरगद की गोल-गोल
हड्डियों की पत्तेदार
उलझनों के ढाँचों में
लटकाओ पोस्टर,
गलियों के अलमस्त
फ़क़ीरों के लहरदार
गीतों से फहराओ
चिपकाओ पोस्टर
कहता है कारीगर ।
मज़े में आते हुए
पेण्टर ने हँसकर कहा–
पोस्टर लगे हैं,
कि ठीक जगह
तड़के ही मज़दूर
पढ़ेंगे घूर-घूर,
रास्ते में खड़े-खड़े लोग-बाग
पढ़ेंगे ज़िन्दगी की
झल्लायी हुई आग !
प्यारे भाई कारीगर,
अगर खींच सकूँ मैं–
हड़ताली पोस्टर पढ़ते हुए
लोगों के रेखा-चित्र,
बड़ा मज़ा आयेगा ।
कत्थई खपरैलों से उठते हुए धुएँ
रंगों में
आसमानी सियाही मिलायी जाय,
सुबह की किरनों के रंगों में
रात के गृह-दीप-प्रकाश को आशाएँ घोलकर
हिम्मतें लायी जायँ,
स्याहियों से आँखें बने
आँखों की पुतली में धधक की लाल-लाल
पाँख बने,
एकाग्र ध्यान-भरी
आँखों की किरनें
पोस्टरों पर गिरे–तब
कहो भाई कैसा हो ?
कारीगर ने साथी के कन्धे पर हाथ रख
कहा तब–
मेरे भी करतब सुनो तुम,
धुएँ से कजलाये
कोठे की भीत पर
बाँस की तीली की लेखनी से लिखी थी
राम-कथा व्यथा की
कि आज भी जो सत्य है
लेकिन, भाई, कहाँ अब वक़्त है !!
तसवीरें बनाने की
इच्छा अभी बाक़ी है–
ज़िन्दगी भूरी ही नहीं, वह ख़ाकी है ।
ज़माने ने नगर के कन्धे पर हाथ रख
कह दिया साफ़-साफ़
पैरों के नखों से या डण्डे की नोक से
धरती की धूल में भी रेखाएँ खींचकर
तसवीरें बनाती हैं
बशर्ते कि ज़िन्दगी के चित्र-सी
बनाने का चाव हो
श्रद्धा हो, भाव हो ।
कारीगर ने हँसकर
बगल में खींचकर पेण्टर से कहा, भाई
चित्र बनाते वक़्त
सब स्वार्थ त्यागे जायँ,
अंधेरे से भरे हुए
ज़ीने की सीढ़ियाँ चढ़ती-उतरती जो
अभिलाषा–अन्ध है
ऊपर के कमरे सब अपने लिए बन्द हैं
अपने लिए नहीं वे !!
ज़माने ने नगर से यह कहा कि
ग़लत है यह, भ्रम है
हमारा अधिकार सम्मिलित श्रम और
छीनने का दम है ।
फ़िलहाल तसवीरें
इस समय हम
नहीं बना पायेंगे
अलबत्ता पोस्टर हम लगा जायेंगे ।
हम धधकायेंगे ।
मानो या मानो मत
आज तो चन्द्र है, सविता है,
पोस्टर ही कविता है !!
वेदना के रक्त से लिखे गये
लाल-लाल घनघोर
धधकते पोस्टर
गलियों के कानों में बोलते हैं
धड़कती छाती की प्यार-भरी गरमी में
भाफ-बने आँसू के ख़ूँख़ार अक्षर !!
चटाख से लगी हुई
रायफ़ली गोली के धड़ाकों से टकरा
प्रतिरोधी अक्षर
ज़माने के पैग़म्बर
टूटता आसमान थामते हैं कन्धों पर
हड़ताली पोस्टर
कहते हैं पोस्टर–
आदमी की दर्द-भरी गहरी पुकार सुन
पड़ता है दौड़ जो
आदमी है वह ख़ूब
जैसे तुम भी आदमी
वैसे मैं भी आदमी,
बूढ़ी माँ के झुर्रीदार
चेहरे पर छाये हुए
आँखों में डूबे हुए
ज़िन्दगी के तजुर्बात
बोलते हैं एक साथ
जैसे तुम भी आदमी
वैसे मैं भी आदमी,
चिल्लाते हैं पोस्टर ।
धरती का नीला पल्ला काँपता है
यानी आसमान काँपता है,
आदमी के ह्रदय में करुणा कि रिमझिम,
काली इस झड़ी में
विचारों की विक्षोभी तडित् कराहती
क्रोध की गुहाओं का मुँह खोले
शक्ति के पहाड़ दहाड़ते
काली इस झड़ी में वेदना की तडित् कराहती
मदद के लिए अब,
करुणा के रोंगटों में सन्नाटा
दौड़ पड़ता आदमी,
व आदमी के दौड़ने के साथ-साथ
दौड़ता जहान
और दौड़ पड़ता आसमान !!
मुहल्ले के मुहाने के उस पार
बहस छिड़ी हुई है,
पोस्टर पहने हुए
बरगद की शाखें ढीठ
पोस्टर धारण किये
भैंरों की कड़ी पीठ
भैंरों और बरगद में बहस खड़ी हुई है
ज़ोरदार जिरह कि कितना समय लगेगा
सुबह होगी कब और
मुश्किल होगी दूर कब
समय का कण-कण
गगन की कालिमा से
बूंद-बूंद चू रहा
तडित्-उजाला बन !!
अँधेरे में [लम्बी कविता]
जिंदगी के…
कमरों में अँधेरे
लगाता है चक्कर
कोई एक लगातार;
आवाज पैरों की देती है सुनाई
बार-बार… बार-बार,
वह नहीं दीखता… नहीं ही दीखता,
किंतु वह रहा घूम
तिलस्मी खोह में गिरफ्तार कोई एक,
भीत-पार आती हुई पास से,
गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि-सा
अस्तित्व जनाता
अनिवार कोई एक,
और मेरे हृदय की धक्-धक्
पूछती है – वह कौन
सुनाई जो देता, पर नहीं देता दिखाई !
इतने में अकस्मात गिरते हैं भीतर से
फूले हुए पलस्तर,
खिरती है चूने-भरी रेत
खिसकती हैं पपड़ियाँ इस तरह –
खुद-ब-खुद
कोई बड़ा चेहरा बन जाता है,
स्वयमपि
मुख बन जाता है दिवाल पर,
नुकीली नाक और
भव्य ललाट है,
दृढ़ हनु
कोई अनजानी अन-पहचानी आकृति।
कौन वह दिखाई जो देता, पर
नहीं जाना जाता है !
कौन मनु ?
बाहर शहर के, पहाड़ी के उस पार, तालाब…
अँधेरा सब ओर,
निस्तब्ध जल,
पर, भीतर से उभरती है सहसा
सलिल के तम-श्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति
कुहरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है
और मुसकाता है,
पहचान बताता है,
किंतु, मैं हतप्रभ,
नहीं वह समझ में आता।
अरे ! अरे !!
तालाब के आस-पास अँधेरे में वन-वृक्ष
चमक-चमक उठते हैं हरे-हरे अचानक
वृक्षों के शीशे पर नाच-नाच उठती हैं बिजलियाँ,
शाखाएँ, डालियाँ झूमकर झपटकर
चीख, एक दूसरे पर पटकती हैं सिर कि अकस्मात् –
वृक्षों के अँधेरे में छिपी हुई किसी एक
तिलस्मी खोह का शिला-द्वार
खुलता है धड़ से
…
घुसती है लाल-लाल मशाल अजीब-सी
अंतराल-विवर के तम में
लाल-लाल कुहरा,
कुहरे में, सामने, रक्तालोक-स्नात पुरुष एक,
रहस्य साक्षात् !!
तेजो प्रभामय उसका ललाट देख
मेरे अंग-अंग में अजीब एक थरथर
गौरवर्ण, दीप्त-दृग, सौम्य-मुख
संभावित स्नेह-सा प्रिय-रूप देखकर
विलक्षण शंका,
भव्य आजानुभुज देखते ही साक्षात्
गहन एक संदेह।
वह रहस्यमय व्यक्ति
अब तक न पायी गयी मेरी अभिव्यक्ति है
पूर्ण अवस्था वह
निज-संभावनाओं, निहित प्रभावों, प्रतिमाओं की,
मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव,
हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव वह,
आत्मा की प्रतिमा।
प्रश्न थे गंभीर, शायद खतरनाक भी,
इसी लिए बाहर के गुंजान
जंगलों से आती हुई हवा ने
फूँक मार एकाएक मशाल ही बुझा दी –
कि मुझको यों अँधेरे में पकड़कर
मौत की सजा दी !
किसी काले डैश की घनी काली पट्टी ही
आँखों में बँध गयी,
किसी खड़ी पाई की सूली पर मैं टाँग दिया गया,
किसी शून्य बिंदु के अँधियारे खड्डे में
गिरा दिया गया मैं
अचेतन स्थिति में !
2
सूनापन सिहरा,
अँधेरे में ध्वनियों के बुलबुले उभरे,
शून्य के मुख पर सलवटें स्वर की,
मेरे ही उर पर, धँसाती हुई सिर,
छटपटा रही हैं शब्दों की लहरें
मीठी है दुःसह !!
अरे, हाँ, साँकल ही रह-रह
बजती है द्वार पर।
कोई मेरी बात मुझे बताने के लिए ही
बुलाता है – बुलाता है
हृदय को सहला मानो किसी जटिल
प्रसंग में सहसा होठों पर
होठ रख, कोई सच-सच बात
सीधे-सीधे कहने को तड़प जाय, और फिर
वही बात सुनकर धँस जाय मेरा जी –
इस तरह, साँकल ही रह-रह बजती है द्वार पर
आधी रात, इतने अँधेरे में, कौन आया मिलने?
विमन प्रतीक्षातुर कुहरे में घिरा हुआ
द्युतिमय मुख – वह प्रेम भरा चेहरा –
भोला-भाला भाव –
पहचानता हूँ बाहर जो खड़ा है
यह वही व्यक्ति है, जी हाँ !
जो मुझे तिलस्मी खोह में दिखा था।
अवसर-अनवसर
प्रकट जो होता ही रहता
मेरी सुविधाओं का न तनिक खयाल कर।
चाहे जहाँ, चाहे जिस समय उपस्थित,
चाहे जिस रूप में
चाहे जिन प्रतीकों में प्रस्तुत,
इशारे से बताता है, समझाता रहता,
हृदय को देता है बिजली के झटके
अरे, उसके चेहरे पर खिलती हैं सुबहें,
गालों पर चट्टानी चमक पठार की
आँखों में किरणीली शांति की लहरें
उसे देख, प्यार उमड़ता है अनायास!
लगता है – दरवाजा खोलकर
बाँहों में कस लूँ,
हृदय में रख लूँ
घुल जाऊँ, मिल जाऊँ लिपटकर उससे
परंतु, भयानक खड्डे के अँधेरे में आहत
और क्षत-विक्षत, मैं पड़ा हुआ हूँ,
शक्ति ही नहीं है कि उठ सकूँ जरा भी
(यह भी तो सही है कि
कमजोरियों से ही लगाव है मुझको)
इसीलिए टालता हूँ उस मेरे प्रिय को
कतराता रहता,
डरता हूँ उससे।
वह बिठा देता है तुंग शिखर के
खतरनाक, खुरदरे कगार-तट पर
शोचनीय स्थिति में ही छोड़ देता मुझको।
कहता है – “पार करो पर्वत-संधि के गह्वर,
रस्सी के पुल पर चलकर
दूर उस शिखर-कगार पर स्वयं ही पहुँचो”
अरे भाई, मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा,
मुझे डर लगता है ऊँचाइयों से
बजने दो साँकल!!
उठने दो अँधेरे में ध्वनियों के बुलबुले,
वह जन – वैसे ही
आप चला जायेगा आया था जैसा।
खड्डे के अँधेरे में मैं पड़ा रहूँगा
पीड़ाएँ समेटे !
क्या करूँ क्या नहीं करूँ मुझे बताओ,
इस तम-शून्य में तैरती है जगत्-समीक्षा
की हुई उसकी
(सह नहीं सकता)
विवेक-विक्षोभ महान् उसका
तम-अंतराल में (सह नहीं सकता)
अँधियारे मुझमें द्युति-आकृति-सा
भविष्य का नक्शा दिया हुआ उसका
सह नहीं सकता !
नहीं, नहीं, उसको छोड़ नहीं सकूँगा,
सहना पड़े – मुझे चाहे जो भले ही।
कमजोर घुटनों को बार-बार मसल,
लड़खड़ाता हुआ मैं
उठता हूँ दरवाजा खोलने,
चेहरे के रक्त-हीन विचित्र शून्य को गहरे
पोंछता हूँ हाथ से,
अँधेरे के ओर-छोर टटोल-टटोलकर
बढ़ता हूँ आगे,
पैरों से महसूस करता हूँ धरती का फैलाव,
हाथों से महसूस करता हूँ दुनिया,
मस्तक अनुभव करता है, आकाश
दिल में तड़पता है अँधेरे का अंदाज,
आँखें ये तथ्य को सूँघती-सी लगतीं,
केवल शक्ति है स्पर्श की गहरी।
आत्मा में, भीषण
सत्-चित्-वेदना जल उठी, दहकी।
विचार हो गए विचरण-सहचर।
बढ़ता हूँ आगे,
चलता हूँ सँभल-सँभलकर,
द्वार टटोलता,
जंग खायी, जमी हुई जबरन
सिटकनी हिलाकर
जोर लगा, दरवाजा खोलता
झाँकता हूँ बाहर…
सूनी है राह, अजीब है फैलाव,
सर्द अँधेरा।
ढीली आँखों से देखते हैं विश्व
उदास तारे।
हर बार सोच और हर बार अफसोस
हर बार फिक्र
के कारण बढे हुए दर्द का मानो कि दूर वहाँ, दूर वहाँ
अँधियारा पीपल देता है पहरा।
हवाओं की निःसंग लहरों में काँपती
कुत्तों की दूर-दूर अलग-अलग आवाज,
टकराती रहती सियारों की ध्वनियों से।
काँपती हैं दूरियाँ, गूँजते हैं फासले
(बाहर कोई नहीं, कोई नहीं बाहर)
इतने में अँधियारे सूने में कोई चीख गया है
रात का पक्षी
कहता है –
“वह चला गया है,
वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं
अब तेरे द्वार पर।
वह निकल गया है गाँव में शहर में !
उसको तू खोज अब
उसका तू शोध कर!
वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति,
उसका तू शिष्य है (यद्यपि पलातक…)
वह तेरी गुरु है,
गुरु है…”
3
समझ न पाया कि चल रहा स्वप्न या
जागृति शुरू है।
दिया जल रहा है,
पीतालोक-प्रसार में काल चल रहा है,
आस-पास फैली हुई जग-आकृतियाँ
लगती हैं छपी हुई जड़ चित्राकृतियों-सी
अलग व दूर-दूर
निर्जीव !!
यह सिविल लाइन्स है। मैं अपने कमरे में
यहाँ पड़ा हुआ हूँ
आँखें खुली हुई हैं,
पीटे गये बालक-सा मार खाया चेहरा
उदास इकहरा,
स्लेट-पट्टी पर खींची गयी तसवीर
भूत-जैसी आकृति –
क्या वह मैं हूँ ?
मैं हूँ ?
रात के दो हैं,
दूर-दूर जंगल में सियारों का हो-हो,
पास-पास आती हुई घहराती गूँजती
किसी रेल-गाड़ी के पहियों की आवाज !!
किसी अनपेक्षित
असंभव घटना का भयानक संदेह,
अचेतन प्रतीक्षा,
कहीं कोई रेल-एक्सीडेंट न हो जाय।
चिंता के गणित अंक
आसमानी-स्लेट-पट्टी पर चमकते
खिड़की से दीखते।
… … …
हाय! हाय! तॉल्सतॉय
कैसे मुझे दीख गये
सितारों के बीच-बीच
घूमते व रुकते
पृथ्वी को देखते।
शायद तॉल्सतॉय-नुमा
कोई वह आदमी
और है,
मेरे किसी भीतरी धागे का आखिरी छोर वह
अनलिखे मेरे उपन्यास का
केंद्रीय संवेदन
दबी हाय-हाय-नुमा।
शायद, तॉल्सतॉय-नुमा।
प्रोसेशन ?
निस्तब्ध नगर के मध्य-रात्रि-अँधेरे में सुनसान
किसी दूर बैंड की दबी हुई क्रमागत तान-धुन,
मंद-तार उच्च-निम्न स्वर-स्वप्न,
उदास-उदास ध्वनि-तरंगें हैं गंभीर,
दीर्घ लहरियाँ !!
गैलरी में जाता हूँ, देखता हूँ रास्ता
वह कोलतार-पथ अथवा
मरी हुई खिंची हुई कोई काली जिह्वा
बिजली के द्युतिमान दिये या
मरे हुए दाँतों का चमकदार नमूना!!
किंतु दूर सड़क के उस छोर
शीत-भरे थर्राते तारों के अँधियारे तल में
नील तेज-उद्भास
पास-पास पास-पास
आ रहा इस ओर!
दबी हुई गंभीर स्वर-स्वप्न-तरंगें,
शत-ध्वनि-संगम-संगीत
उदास तान-धुन
समीप आ रहा!!
और, अब
गैस-लाइट-पाँतों की बिंदुएँ छिटकीं,
बीचों-बीच उनके
साँवले जुलूस-सा क्या-कुछ दीखता!!
और अब
गैस-लाइट-निलाई में रँगे हुए अपार्थिव चेहरे,
बैंड-दल,
उनके पीछे काले-काले बलवान् घोड़ों का जत्था
दीखता,
घना व डरावना अवचेतन ही
जुलूस में चलता।
क्या शोभा-यात्रा
किसी मृत्यु दल की ?
अजीब!!
दोनों ओर, नीली गैस-लाइट-पाँत
रही जल, रही जल।
नींद में खोये हुए शहर की गहन अवचेतना में
हलचल, पाताली तल में
चमकदार साँपों की उड़ती हुई लगातार
लकीरों की वारदात !!
सब सोये हुए हैं।
लेकिन, मैं जाग रहा, देख रहा
रोमांचकारी वह जादुई करामात!!
विचित्र प्रोसेशन,
गंभीर क्विक मार्च…
कलाबत्तूवाला काला जरीदार ड्रेस पहने
चमकदार बैंड-दल –
अस्थि-रूप, यकृत-स्वरूप, उदर-आकृति
आँतों के जालों से, बाजे वे दमकते हैं भयंकर
गंभीर गीत-स्वप्न-तरंगें
उभारते रहते,
ध्वनियों के आवर्त मँडराते पथ पर।
बैंड के लोगों के चेहरे
मिलते हैं मेरे देखे हुओं-से
लगता है उनमें कई प्रतिष्ठित पत्रकार
इसी नगर के !!
बड़े-बड़े नाम अरे कैसे शामिल हो गये इस बैंड-दल में !
उनके पीछे चल रहा
संगीन नोकों का चमकता जंगल,
चल रही पदचाप, ताल-बद्ध दीर्घ पाँत
टैंक-दल, मोर्टार, ऑर्टिलरी, सन्नद्ध,
धीरे-धीरे बढ़ रहा जुलूस भयावना,
सैनिकों के पथराये चेहरे
चिढ़े हुए, झुलसे हुए, बिगड़े हुए गहरे !
शायद, मैंने उन्हे पहले भी तो कहीं देखा था।
शायद, उनमें कई परिचित !!
उनके पीछे यह क्या !!
कैवेलरी !
काले-काले घोड़ों पर खाकी मिलिट्री ड्रेस,
चेहरे का आधा भाग सिन्दूरी-गेरुआ
आधा भाग कोलतारी भैरव,
आबदार !!
कंधे से कमर तक कारतूसी बेल्ट है तिरछा।
कमर में, चमड़े के कवर में पिस्तोल,
रोष-भरी एकाग्रदृष्टि में धार है,
कर्नल, बिग्रेडियर, जनरल, मॉर्शल
कई और सेनापति सेनाध्यक्ष
चेहरे वे मेरे जाने-बूझे से लगते,
उनके चित्र समाचारपत्रों में छपे थे,
उनके लेख देखे थे,
यहाँ तक कि कविताएँ पढ़ी थीं
भई वाह!
उनमें कई प्रकांड आलोचक, विचारक जगमगाते कवि-गण
मंत्री भी, उद्योगपति और विद्वान
यहाँ तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात
डोमाजी उस्ताद
बनता है बलबन
हाय, हाय !!
यहाँ ये दीखते हैं भूत-पिशाच-काय।
भीतर का राक्षसी स्वार्थ अब
साफ उभर आया है,
छिपे हुए उद्देश्य
यहाँ निखर आये हैं,
यह शोभायात्रा है किसी मृत-दल की।
विचारों की फिरकी सिर में घूमती है
इतने में प्रोसेशन में से कुछ मेरी ओर
आँखें उठीं मेरी ओर-भर
हृदय में मानो कि संगीन नोकें ही घुस पड़ीं बर्बर,
सड़क पर उठ खड़ा हो गया कोई शोर –
“मारो गोली, दागो स्साले को एकदम
दुनिया की नजरों से हटकर
छिपे तरीके से
हम जा रहे थे कि
आधीरात – अँधेरे में उसने
देख लिया हमको
व जान गया वह सब
मार डालो, उसको खत्म करो एकदम”
रास्ते पर भाग-दौड़ थका-पेल !!
गैलरी से भागा मैं पसीने से शराबोर !!
एकाएक टूट गया स्वप्न व छिन्न-भिन्न हो गये
सब चित्र
जागते में फिर से याद आने लगा वह स्वप्न,
फिर से याद आने लगे अँधेरे में चेहरे,
और, तब मुझे प्रतीत हुआ भयानक
गहन मृतात्माएँ इसी नगर की
हर रात जुलूस में चलतीं,
परंतु दिन में
बैठती हैं मिलकर करती हुई षड्यंत्र
विभिन्न दफ्तरों-कार्यालयों, केंद्रों में, घरों में।
हाय, हाय! मैंने उन्हे दैख लिया नंगा,
इसकी मुझे और सजा मिलेगी।
4
अकस्मात्
चार का गजर कहीं खड़का
मेरा दिल धड़का,
उदास मटमैला मनरूपी वल्मीक
चल-विचल हुआ सहसा।
अनगिनत काली-काली हायफन-डैशों की लीकें
बाहर निकल पड़ीं, अंदर घुस पड़ीं भयभीत,
सब ओर बिखराव।
मैं अपने कमरे में यहाँ लेटा हुआ हूँ।
काले-काले शहतीर छत के
हृदय दबोचते।
यद्यपि आँगन में नल जो मारता,
जल खखारता।
किंतु न शरीर में बल है
अँधेरे में गल रहा दिल यह।
एकाएक मुझे भान होता है जग का,
अखबारी दुनिया का फैलाव,
फँसाव, घिराव, तनाव है सब ओर,
पत्ते न खड़के,
सेना ने घेर ली हैं सड़कें।
बुद्धि की मेरी रग
गिनती है समय की धक्-धक्।
यह सब क्या है
किसी जन-क्रांति के दमन-निमित्त यह
मॉर्शल-लॉ है!
दम छोड़ रहे हैं भाग गलियों में मरे पैर,
साँस लगी हुई है,
जमाने की जीभ निकल पड़ी है,
कोई मेरा पीछा कर रहा है लगातार
भागता मैं दम छोड़,
घूम गया कई मोड़,
चौराहा दूर से ही दीखता,
वहाँ शायद कोई सैनिक पहरेदार
नहीं होगा फिलहाल
दिखता है सामने ही अंधकार-स्तूप-सा
भयंकर बरगद –
सभी उपेक्षितों, समस्त वंचितों,
गरीबों का वही घर, वही छत,
उसके ही तल-खोह-अँधेरे में सो रहे
गृह-हीन कई प्राण।
अँधेरे में डूब गये
डालों में लटके जो मटमैले चिथड़े
किसी एक अति दीन
पागल के धन वे।
हाँ, वहाँ रहता है, सिर-फिरा एक जन।
किंतु आज इस रात बात अजीब है।
वही जो सिर-फिरा पागल कतई था
आज एकाएक वह
जागृत बुद्धि है, प्रज्वलत् धी है।
छोड़ सिर-फिरापन,
बहुत ऊँचे गले से,
गा रहा कोई पद, कोई गान
आत्मोद्बोधमय !!
खूब भई, खूब भई,
जानता क्या वह भी कि
सैनिक प्रशासन है नगर में वाकई!
क्या उसकी बुद्धि भी जग गयी!
(करुण रसाल वे हृदय के स्वर हैं
गद्यानुवाद यहाँ उनका दिया जा रहा)
”ओ मेरे आदर्शवादी मन,
ओ मेरे सिद्धांतवादी मन,
अब तक क्या किया?
जीवन क्या जिया !!
उदरंभरि बन अनात्म बन गये,
भूतों की शादी में कनात-से तन गये,
किसी व्यभिचारी के बन गये बिस्तर,
दुःखों के दागों को तमगों-सा पहना,
अपने ही खयालों में दिन-रात रहना,
असंग बुद्धि व अकेले में सहना,
जिंदगी निष्क्रिय बन गयी तलघर,
अब तक क्या किया,
जीवन क्या जिया!!
बताओ तो किस-किसके लिए तुम दौड़ गये,
करुणा के दृश्यों से हाय! मुँह मोड़ गये,
बन गये पत्थर,
बहुत-बहुत ज्यादा लिया,
दिया बहुत-बहुत कम,
मर गया देश, अरे जीवित रह गये तुम !!
लो-हित-पिता को घर से निकाल दिया,
जन-मन-करुणा-सी माँ को हंकाल दिया,
स्वार्थों के टेरियार कुत्तों को पाल लिया,
भावना के कर्तव्य – त्याग दिये,
हृदय के मंतव्य – मार डाले!
बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया,
तर्कों के हाथ उखाड़ दिये,
जम गये, जाम हुए, फँस गये,
अपने ही कीचड़ में धँस गये !!
विवेक बघार डाला स्वार्थों के तेल में
आदर्श खा गये !
अब तक क्या किया,
जीवन क्या जिया,
ज्यादा लिया और दिया बहुत-बहुत कम
मर गया देश, अरे जीवित रह गये तुम…”
मेरा सिर गरम है,
इसीलिए भरम है।
सपनों में चलता है आलोचन,
विचारों के चित्रों की अवलि में चिंतन।
निजत्व-माफ है बेचैन,
क्या करूँ, किससे कहूँ,
कहाँ जाऊँ, दिल्ली या उज्जैन?
वैदिक ऋषि शुनःशेप के
शापभ्रष्ट पिता अजीर्गत समान ही
व्यक्तित्व अपना ही, अपने से खोया हुआ
वही उसे अकस्मात् मिलता था रात में,
पागल था दिन में
सिर-फिरा विक्षिप्त मस्तिष्क।
हाय, हाय!
उसने भी यह क्या गा दिया,
यह उसने क्या नया ला दिया,
प्रत्यक्ष,
मैं खड़ा हो गया
किसी छाया मूर्ति-सा समक्ष स्वयं के
होने लगी बहस और
लगने लगे परस्पर तमाचे।
छिः पागलपन है,
वृथा आलोचन है।
गलियों में अंधकार भयावह –
मानो मेरे कारण ही लग गया
मॉर्शल-लॉ वह,
मानो मेरी निष्क्रिय संज्ञा ने संकट बुलाया,
मानो मेरे कारण ही दुर्घट
हुई यह घटना।
चक्र से चक्र लगा हुआ है…
जितना ही तीव्र है द्वंद्व क्रियाओं घटनाओं का
बाहरी दुनिया में,
उतनी ही तेजी से भीतरी दुनिया में,
चलता है द्वंद्व कि
फिक्र से फिक्र लगी हुई है।
आज उस पागल ने मेरी चैन भुला दी,
मेरी नींद गवाँ दी।
मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ।
मेरा यह चेहरा
घुलता है जाने किस अथाह गंभीर, साँवले जल से,
झुके हुए गुमसुम टूटे हुए घरों के
तिमिर अतल से
घुलता है मन यह।
रात्रि के श्यामल ओस से क्षालित
कोई गुरु-गंभीर महान् अस्तित्व
महकता है लगातार
मानो खंडहर-प्रसारों में उद्यान
गुलाब-चमेली के, रात्रि-तिमिर में,
महकते हों, महकते ही रहते हों हर पल।
किंतु वे उद्यान कहाँ हैं,
अँधेरे में पता नहीं चलता।
मात्र सुगंध है सब ओर,
पर, उस महक – लहर में
कोई छिपी वेदना, कोई गुप्त चिंता
छटपटा रही है।
5
एकाएक मुझे भान !!
पीछे से किसी अजनबी ने
कंधे पर रक्खा हाथ।
चौंकता मैं भयानक
एकाएक थरथर रेंग गयी सिर तक,
नहीं नहीं। ऊपर से गिरकर
कंधे पर बैठ गया बरगद-पात तक,
क्या वह संकेत, क्या वह इशारा?
क्या वह चिट्ठी है किसी की?
कौन-सा इंगित?
भागता मैं दम छोड़,
घूम गया कई मोड़!!
बंदूक धाँय-धाँय
मकानों के ऊपर प्रकाश-सा छा रहा गेरुआ।
भागता मैं दम छोड़
घूम गया कई मोड़।
घूम गयी पृथ्वी, घूम गया आकाश,
और फिर, किसी एक मुँदे हुए घर की
पत्थर, सीढ़ी दिख गयी, उस पार
चुपचाप बैठ गया सिर पकड़कर !!
दिमाग में चक्कर
चक्कर… भँवरें
भँवरों के गोल-गोल केंद्र में दीखा
स्वप्न सरीखा –
भूमि की सतहों के बहुत-बहुत नीचे
अँधियारी एकांत
प्राकृत गुहा एक।
विस्तृत खोह के साँवले तल में
तिमिर को भेदकर चमकते हैं पत्थर
मणि तेजस्क्रिय रेडियो-एक्टिव रत्न भी बिखरे,
झरता है जिन पर प्रबल प्रपात एक।
प्राकृत जल वह आवेग-भरा है,
द्युतिमान् मणियों की अग्नियों पर से
फिसल-फिसलकर बहती लहरें,
लहरों के तल में से फूटती हैं किरनें
रत्नों की रंगीन रूपों की आभा
फूट निकलती
खोह की बेडौल भीतें हैं झिलमिल !!
पाता हूँ निज को खोह के भीतर,
विलुब्ध नेत्रों से देखता हूँ द्युतियाँ,
मणि तेजस्क्रिय हाथों में लेकर
विभोर आँखों से देखता हूँ उनको –
पाता हूँ अकस्मात्
दीप्ति में वलयित रत्न वे नहीं हैं
अनुभव, वेदना, विवेक-निष्कर्ष,
मेरे ही अपने यहाँ पड़े हुए हैं
विचारों की रक्तिम अग्नि के मणि वे
प्राण-जल-प्रपात में घुलते हैं प्रतिपल
अकेले में किरणों की गीली है हलचल
गीली है हलचल !!
6
हाय, हाय! मैंने उन्हें गुहा-वास दे दिया
लोक-हित क्षेत्र से कर दिया वंचित
जनोपयोग से वर्जित किया और
निषिद्ध कर दिया
खोह में डाल दिया!!
वे खतरनाक थे,
(बच्चे भीख माँगते) खैर…
यह न समय है,
जूझना ही तै है।
सीन बदलता है
सुनसान चौराहा साँवला फैला,
बीच में वीरान गेरुआ घंटाघर,
ऊपर कत्थई बुजर्ग गुंबद,
साँवली हवाओं में काल टहलता है।
रात में पीले हैं चार घड़ी-चेहरे,
मिनिट के काँटों की चार अलग गतियाँ,
चार अलग कोण,
कि चार अलग संकेत
(मनस् में गतिमान् चार अलग मतियाँ)
खंभों पर बिजली की गरदनें लटकीं,
शर्म से जलते हुए बल्बों के आस-पास
बेचैन खयालों के पंखों के कीड़े
उड़ते हैं गोल-गोल
मचल-मचलकर।
घंटाघर तले ही
पंखों के टुकड़े व तिनके।
गुंबद-विवर में बैठे हुए बूढ़े
असंभव पक्षी
बहुत तेज नजरों से देखते हैं सब ओर,
मानो कि इरादे
भयानक चमकते।
सुनसान चौराहा
बिखरी हैं गतियाँ, बिखरी है रफ्तार,
गश्त में घूमती है कोई दुष्ट इच्छा।
भयानक सिपाही जाने किस थकी हुई झोंक में
अँधेरे में सुलगाता सिगरेट अचानक
ताँबे से चेहरे की ऐंठ झलकती।
पथरीली सलवट
दियासलाई की पल-भर लौ में
साँप-सी लगती।
पर उसके चेहरे का रंग बदलता है हर बार,
मानो अनपेक्षित कहीं न कुछ हो…
वह ताक रहा है –
संगीन नोंकों पर टिका हुआ
साँवला बंदूक-जत्था
गोल त्रिकोण एक बनाये खड़ा जो
चौक के बीच में !!
एक ओर
टैंकों का दस्ता भी खड़े-खड़े ऊँघता,
परंतु अड़ा है!!
भागता मैं दम छोड़,
घूम गया कई मोड़
भागती है चप्पल, चटपट आवाज
चाँटों-सी पड़ती।
पैरों के नीचे का कीच उछलकर
चेहरे पर छाती पर, पड़ता है सहसा,
ग्लानि की मितली।
गलियों का गोल-गोल खोह अँधेरा
चेहरे पर आँखों पर करता है हमला।
अजीब उमस-बास
गलियों का रुँधा हुआ उच्छवास
भागता हूँ दम छोड़,
घूम गया कई मोड़।
धुँधले-से आकार कहीं-कहीं दीखते,
भय के? या घर के? कह नहीं सकता
आता है अकस्मात् कोलतार-रास्ता
लंबा व चौड़ा व स्याह व ठंडा,
बेचैन आँखें ये देखती हैं सब ओर।
कहीं कोई नहीं है,
नहीं कहीं कोई भी।
श्याम आकाश में, संकेत-भाषा-सी तारों की आँखें
चमचमा रही हैं।
मेरा दिल ढिबरी-सा टिमटिमा रहा है।
कोई मुझे खींचता है रास्ते के बीच ही।
जादू से बँधा हुआ चल पड़ा उस ओर।
सपाट सूने में ऊँची-सी खड़ी जो
तिलक की पाषाण-मूर्ति है निःसंग
स्तब्ध जड़ीभूत…
देखता हूँ उसको परंतु, ज्यों ही मैं पास पहुँचता
पाषाण-पीठिका हिलती-सी लगती
अरे, अरे यह क्या!!
कण-कण काँप रहे जिनमें-से झरते
नीले इलेक्ट्रान
सब ओर गिर रही हैं चिनगियाँ नीली
मूर्ति के तन से झरते हैं अंगार।
मुस्कान पत्थरी होठों पर काँपी,
आँखों में बिजली के फूल सुलगते।
इतने में यह क्या!!
भव्य ललाट की नासिका में से
बह रहा खून न जाने कब से
लाल-लाल गरमीला रक्त टपकता
(खून के धब्बों से भरा अँगरखा)
मानो कि अतिशय चिंता के कारण
मस्तक-कोष ही फूट पड़े सहसा
मस्तक-रक्त ही बह उठा नासिका में से।
हाय, हाय, पितः पितः ओ,
चिंता में इतने न उलझो
हम अभी जिंदा हैं जिंदा,
चिंता क्या है !!
मैं उस पाषाण-मूर्ति के ठंडे
पैरों की छाती से बरबस चिपका
रुआँसा-सा होता
देह में तन गये करुणा के काँटे
छाती पर, सिर पर, बाँहों पर मेरे
गिरती हैं नीली
बिजली की चिनगियाँ
रक्त टपकता है हृदय में मेरे
आत्मा में बहता-सा लगता
खून का तालाब।
इतने में छाती के भीतर ठक्-ठक्
सिर में है धड़-धड़ !! कट रही हड्डी !!
फिक्र जबरदस्त !!
विवेक चलाता तीखा-सा रंदा
चल रहा बसूला
छीले जा रहा मेरा निजत्व ही कोई
भयानक जिद कोई जाग उठी मेरे भी अंदर
हठ कोई बड़ा भारी उठ खड़ा हुआ है।
इतने में आसमान काँपा व धाँय-धाँय
बंदूक-धड़ाका
बिजली की रफ्तार पैरों में घूम गयी।
खोहों-सी गलियों के अँधेरे में एक ओर
मैं थक बैठ गया,
सोचने-विचारने।
अँधेरे में डूबे मकानों के छप्परों के पार से
रोने की पतली-सी आवाज
सूने में काँप रही काँप रही दूर तक
कराहों की लहरों में पाशव प्राकृत
वेदना भयानक थरथरा रही है।
मैं उसे सुनने का करता हूँ यत्न
कि देखता क्या हूँ –
सामने मेरे
सर्दी में बोरे को ओढ़कर
कोई एक अपने
हाथ-पैर समेटे
काँप रहा, हिल रहा – वह मर जायगा।
इतने में वह सिर खोलता है सहसा
बाल बिखरते
दीखते हैं कान कि
फिर मुँह खोलता है, वह कुछ
बुदबुदा रहा है,
किंतु मैं सुनता ही नहीं हूँ।
ध्यान से देखता हूँ – वह कोई परिचित
जिसे खूब देखा था, निरखा था कई बार
पर पाया नहीं था।
अरे हाँ, वह तो…
विचार उठते ही दब गये,
सोचने का साहस सब चला गया है।
वह मुख – अरे, वह मुख, वे गाँधी जी !!
इस तरह पंगु !!
आश्चर्य !!
नहीं, नहीं वे जाँच-पड़ताल
रूप बदलकर करते हैं चुपचाप।
सुरागरसी-सी कुछ।
अँधेरे की स्याही में डूबे हुए देव को सम्मुख पाकर
मैं अति दीन हो जाता हूँ पास कि
बिजली का झटका
कहता है – “भाग जा, हट जा
हम हैं गुजर गये जमाने के चेहरे
आगे तू बढ़ जा।”
किंतु मैं देखा किया उस मुख को।
गंभीर दृढ़ता की सलवटें वैसी ही,
शब्दों में गुरुता।
वे कह रहे हैं –
“दुनिया न कचरे का ढेर कि जिस पर
दानों को चुगने चढ़ा हुआ कोई भी कुक्कुट
कोई भी मुरगा
यदि बाँग दे उठे जोरदार
बन जाये मसीहा”
वे कह रहे हैं –
”मिट्टी के लोंदे में किरगीले कण-कण
गुण हैं,
जनता के गुणों से ही संभव
भावी का उद्भव…”
गंभीर शब्द वे और आगे बढ़ गये,
जाने क्या कह गये!!
मैं अति उद्विग्न!
एकाएक उठ पड़ा आत्मा का पिंजर
मूर्ति की ठठरी।
नाक पर चश्मा, हाथ में डंडा,
कंधे पर बोरा, बाँह में बच्चा।
आश्चर्य ! अद्भुत ! यह शिशु कैसे !!
मुसकरा उस द्युति-पुरुष ने कहा तब –
“मेरे पास चुपचाप सोया हुआ यह था।
सँभालना इसको, सुरक्षित रखना”
मैं कुछ कहने को होता हूँ इतने में वहाँ पर
कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है :
और ज्यादा गहरा व और ज्यादा अकेला
अँधेरे का फैलाव!
बालक लिपटा है मेरे इस गले से चुपचाप,
छाती से कंधे से चिपका है नन्हा-सा आकाश
स्पर्श है सुकुमार प्यार-भरा कोमल
किंतु है भार का गंभीर अनुभव
भावी की गंध और दूरियाँ अँधेरी
आकाशी तारों को साथ लिये हुए मैं
चला जा रहा हूँ
घुसता ही जाता हूँ फासलों की खोहों तहों में।
सहसा रो उठा कंधे पर वह शिशु
अरे, अरे, वह स्वर अतिशय परिचित !!
पहले भी कई बार कहीं तो भी सुना था,
उसमें तो स्फोटक क्षोभ का आयेगा,
गहरी है शिकायत,
क्रोध भयंकर।
मुझे डर यदि कोई वह स्वर सुन ले
हम दोनों फिर कहीं नहीं रह सकेंगे।
मैं पुचकारता हूँ, बहुत दुलारता,
समझाने के लिए तब गाता हूँ गाने,
अधभूली लोरी ही होठों से फूटती !
मैं चुप करने की जितनी भी करता हूँ कोशिश,
और-और चीखता है क्रोध से लगातार !!
गरम-गरम अश्रु टपकते हैं मुझपर।
किंतु, न जाने क्यों खुश बहुत हूँ।
जिसको न मैं जीवन में कर पाया,
वह कर रहा है।
मैं शिशु-पीठ को थपथपा रहा हूँ,
आत्मा है गीली।
पैर आगे बढ़ रहे, मन आगे जा रहा।
डूबता हूँ मैं किसी भीतरी सोच में –
हृदय के थाले में रक्त का तालाब,
रक्त में डूबी हैं द्युतिमान् मणियाँ,
रुधिर से फूट रहीं लाल-लाल किरणें,
अनुभव-रक्त में डूबे हैं संकल्प,
और ये संकल्प
चलते हैं साथ-साथ।
अँधियारी गलियों में चला जा रहा हूँ।
इतने में पाता हूँ अँधेरे में सहसा
कंधे पर कुछ नहीं !!
वह शिशु
चला गया जाने कहाँ,
और अब उसके ही स्थान पर
मात्र हैं सूरज-मुखी-फूल-गुच्छे।
उन स्वर्ण-पुष्पों से प्रकाश-विकीरण
कंधों पर, सिर पर, गालों पर, तन पर,
रास्ते पर, फैले हैं किरणों के कण-कण।
भई वाह, यह खूब !!
इतने गली एक आ गयी और मैं
दरवाजा खुला हुआ देखता।
जीना है अँधेरा।
कहीं कोई ढिबरी-सी टिमटिमा रही है!
मैं बढ़ रहा हूँ
कंधों पर फूलों के लंबे वे गुच्छे
क्या हुए, कहाँ गये?
कंधे क्यों वजन से दुख रहे सहसा।
ओ हो,
बंदूक आ गयी
वाह वा… !!
वजनदार रॉयफल
भई खूब !!
खुला हुआ कमरा है साँवली हवा है,
झाँकते हैं खिड़कियों में से दूर अँधेरे में टँके हुए सितारे
फैली है बर्फीली साँस-सी वीरान,
तितर-बितर सब फैला है सामान।
बीच में कोई जमीन पर पसरा,
फैलाये बाँहें, ढह पड़ा आखिर।
मैं उस जन पर फैलाता टार्च कि यह क्या –
खून भरे बाल में उलझा है चेहरा,
भौहों के बीच में गोली का सूराख,
खून का परदा गालों पर फैला,
होठों पर सूखी है कत्थई धारा,
फूटा है चश्मा नाक है सीधी,
ओफ्फो !! एकांत-प्रिय यह मेरा
परिचित व्यक्ति है, वहीं, हाँ,
सचाई थी सिर्फ एक अहसास
वह कलाकार था
गलियों के अँधेरे का, हृदय में, भार था
पर, कार्य क्षमता से वंचित व्यक्ति,
चलाता था अपना असंग अस्तित्व।
सुकुमार मानवीय हृदयों के अपने
शुचितर विश्व के मात्र थे सपने।
स्वप्न व ज्ञान व जीवनानुभव जो –
हलचल करता था रह-रह दिल में
किसी को भी दे नहीं पाया था वह तो।
शून्य के जल में डूब गया नीरव
हो नहीं पाया उपयोग उसका।
किंतु अचानक झोंक में आकर क्या कर गुजरा कि
संदेहास्पद समझा गया और
मारा गया वह बधिकों के हाथों।
मुक्ति का इच्छुक तृषार्त अंतर
मुक्ति के यत्नों के साथ निरंतर
सबका था प्यारा।
अपने में द्युतिमान।
उनका यों वध हुआ,
मर गया एक युग,
मर गया एक जीवनादर्श !!
इतने में मुझको ही चिढ़ाता है कोई।
सवाल है – मैं क्या करता था अब तक,
भागता फिरता था सब ओर।
(फिजूल है इस वक़्त कोसना खुद को)
एकदम जरूरी-दोस्तों को खोजूँ
पाऊँ मैं नये-नये सहचर
सकर्मक सत्-चित्-वेदना-भास्कर!!
जीने से उतरा
एकाएक विद्रूप रूपों से घिर गया सहसा
पकड़ मशीन-सी,
भयानक आकार घेरते हैं मुझको,
मैं आततायी-सत्ता के सम्मुख।
एकाएक हृदय धड़ककर रुक गया, क्या हुआ !!
भयानक सनसनी।
पकड़कर कॉलर गला दबाया गया।
चाँटे से कनपटी टूटी कि अचानक
त्वचा उखड़ गयी गाल की पूरी।
कान में भर गयी
भयानक अनहद-नाद की भनभन।
आँखों में तैरीं
रक्तिम तितलियाँ, चिनगियाँ नीली।
सामने ऊगते-डूबते धुँधले
कुहरिल वर्तुल,
जिनका कि चक्रिल केंद्र ही फैलता जाता
उस फैलाव में दीखते मुझको
धँस रहे, गिर रहे बड़े-बड़े टॉवर
घुँघराला धूआँ, गेरूआ ज्वाला।
हृदय में भगदड़ –
सम्मुख दीखा
उजाड़ बंजर टीले पर सहसा
रो उठा कोई, रो रहा कोई
भागता कोई सहायता देने।
अंतर्तत्त्वों का पुनर्प्रबंध और पुनर्व्यवस्था
पुनर्गठन-सा होता जा रहा।
दृश्य ही बदला, चित्र बदल गया
जबरन ले जाया गया मैं गहरे
अँधियारे कमरे के स्याह सिफर में।
टूटे-से स्टूल में बिठाया गया हूँ।
शीश की हड्डी जा रही तोड़ी।
लोहे की कील पर बड़े हथौड़े
पड़ रहे लगातार।
शीश का मोटा अस्थि-कवच ही निकाल डाला।
देखा जा रहा –
मस्तक-यंत्र में कौन विचारों की कौन-सी ऊर्जा,
कौन-सी शिरा में कौन-सी धक्-धक्,
कौन-सी रग में कौन-सी फुरफुरी,
कहाँ है पश्यत् कैमरा जिसमें
तथ्यों के जीवन-दृश्य उतरते,
कहाँ-कहाँ सच्चे सपनों के आशय
कहाँ-कहाँ क्षोभक-स्फोटक सामान!
भीतर कहीं पर गड़े हुए गहरे
तलघर अंदर
छिपे हुए प्रिंटिंग प्रेस को खोजो।
जहाँ कि चुपचाप खयालों के परचे
छपते रहते हैं, बाँटे जाते।
इस संस्था के सेक्रेट्री को खोज निकालो,
शायद, उसका ही नाम हो आस्था,
कहाँ है सरगना इस टुकड़ी का
कहाँ है आत्मा?
(और, मैं सुनता हूँ चिढ़ी हुई ऊँची
खिझलायी आवाज)
स्क्रीनिंग करो – मिस्टर गुप्ता,
क्रॉस एक्जामिन हिम थॉरोली !!
चाबुक-चमकार
पीठ पर यद्यपि
उखड़े चर्म की कत्थई-रक्तिम रेखाएँ उभरीं
पर, यह आत्मा कुशल बहुत है,
देह में रेंग रही संवेदना की गरमीली कड़ुई धारा गहरी
झनझन थरथर तारों को उसके,
समेटकर वह सब
वेदना-विस्तार करके इकट्ठा
मेरा मन यह
जबरन उसकी छोटी-सी कड्ढी
गठान बाँधता सख्त व मजबूत
मानो कि पत्थर।
जोर लगाकर,
उसी गठान को हथेलियों से
करता है चूर-चूर,
धूल में बिखरा देता है उसको।
मन यह हटता है देह की हद से
जाता है कहीं पर अलग जगत् में।
विचित्र क्षण है,
सिर्फ है जादू,
मात्र मैं बिजली
यद्यपि खोह में खूँटे बँधा हूँ
दैत्य है आस-पास
फिर भी बहुत दूर मीलों के पार वहाँ
गिरता हूँ चुपचाप पत्र के रूप में
किसी एक जेब में
वह जेब…
किसी एक फटे हुए मन की।
समस्वर, समताल,
सहानुभूति की सनसनी कोमल !!
हम कहाँ नहीं हैं
सभी जगह हम।
निजता हमारी ?
भीतर-भीतर बिजली के जीवित
तारों के जाले,
ज्वलंत तारों की भीषण गुत्थी,
बाहर-बाहर धूल-सी भूरी
जमीन की पपड़ी
अग्नि को लेकर, मस्तक हिमवत्,
उग्र प्रभंजन लेकर, उर यह
बिलकुल निश्चल।
भीषण शक्ति को धारण करके
आत्मा का पोशाक दीन व मैला।
विचित्र रूपों को धारण करके
चलता है जीवन, लक्ष्यों के पथ पर।
7
रिहा !!
छोड़ दिया गया मैं,
कई छाया-मुख अब करते हैं पीछा,
छायाकृतियाँ न छोड़ती हैं मुझको,
जहाँ-जहाँ गया वहाँ
भौंहों के नीचे के रहस्यमय छेद
मारते हैं संगीन –
दृष्टि की पत्थरी चमक है पैनी।
मुझे अब खोजने होंगे साथी –
काले गुलाब व स्याह सिवंती,
श्याम चमेली,
सँवलाये कमल जो खोहों के जल में
भूमि के भीतर पाताल-तल में
खिले हुए कबसे भेजते हैं संकेत
सुझाव-संदेश भेजते रहते !!
इतने में सहसा दूर क्षितिज पर
दीखते हैं मुझको
बिजली की नंगी लताओं से भर रहे
सफेद नीले मोतिया चंपई फूल गुलाबी
उठते हैं वहीं पर हाथ अकस्मात्
अग्नि के फूलों को समेटने लगते।
मैं उन्हें देखने लगता हूँ एकटक,
अचानक विचित्र स्फूर्ति से मैं भी
जमीन पर पड़े हुए चमकीले पत्थर
लगातार चुनकर
बिजली के फूल बनाने की कोशिश
करता हूँ। रश्मि-विकिरण –
मेरे भी प्रस्तर करते हैं प्रतिक्षण।
रेडियो-एक्टिव रत्न हैं वे भी।
बिजली के फूलों की भाँति ही
यत्न हैं वे भी,
किंतु, असंतोष मुझको है गहरा,
शब्दाभिव्यक्ति-अभाव का संकेत।
काव्य-चमत्कार उतना ही रंगीन
परंतु, ठंडा।
मेरे भी फूल हैं तेजस्क्रिय, पर
अतिशय शीतल।
मुझको तो बेचैन बिजली की नीली
ज्वलंत बाँहों में बाँहों को उलझा
करनी है उतनी ही प्रदीप्त लीला
आकाश-भर में साथ-साथ उसके घूमना है मुझको
मेरे पास न रंग है बिजली का गौर कि
भीमाकार हूँ मेघ मैं काला
परंतु, मुझको है गंभीर आवेश
अथाह प्रेरणा-स्रोत का संयम।
अरे, इन रंगीन पत्थर-फूलों से मेरा
काम नहीं चलेगा !!
क्या कहूँ,
मस्तक-कुंड में जलती
सत्-चित्-वेदना-सचाई व गलती –
मस्तक शिराओं में तनाव दिन-रात।
अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे
उठाने ही होंगे।
तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब।
पहुँचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार
तब कहीं देखने मिलेंगी बाँहें
जिसमें कि प्रतिपल काँपता रहता
अरुण कमल एक
ले जाने उसको धँसना ही होगा
झील के हिम-शीत सुनील जल में
चाँद उग गया है
गलियों की आकाशी लंबी-सी चीर में
तिरछी है किरनों की मार
उस नीम पर
जिसके कि नीचे
मिट्टी के गोल चबूतरे पर, नीली
चाँदनी में कोई दिया सुनहला
जलता है मानो कि स्वप्न ही साक्षात्
अदृश्य साकार।
मकानों के बड़े-बड़े खंडहर जिनके कि सूने
मटियाले भागों में खिलती ही रहती
महकती रातरानी फूल-भरी जवानी में लज्जित
तारों की टपकती अच्छी न लगती।
भागता मैं दम छोड़
घूम गया कई मोड़,
ध्वस्त दीवालों के उस पार कहीं पर
बहस गरम है
दिमाग में जान है, दिलों में दम है
सत्य से सत्ता के युद्ध को रंग है,
पर कमजोरियाँ सब मेरे संग हैं,
पाता हूँ सहसा –
अँधेरे की सुरंग-गलियों में चुपचाप
चलते हैं लोग-बाग
दृढ़-पद गंभीर,
बालक युवागण
मंद-गति नीरव
किसी निज भीतरी बात में व्यस्त हैं,
कोई आग जल रही तो भी अंत:स्थ।
विचित्र अनुभव !!
जितना मैं लोगों की पाँतों को पार कर
बढ़ता हूँ आगे,
उतना ही पीछे मैं रहता हूँ अकेला,
पश्चात्-पद हूँ।
पर, एक रेला और
पीछे से चला और
अब मेरे साथ है।
आश्चर्य !! अद्भुत !!
लोगों की मुट्ठियाँ बँधी हैं।
अँगुली-संधि से फूट रहीं किरनें
लाल-लाल
यह क्या !!
मेरे ही विक्षोभ-मणियों को लिये वे,
मेरे ही विवेक-रत्नों को लेकर,
बढ़ रहे लोग अँधेरे में सोत्साह।
किंतु मैं अकेला।
बौद्धिक जुगाली में अपने से दुकेला।
गलियों के अँधेरे में मैं भाग रहा हूँ,
इतने में चुपचाप कोई एक
दे जाता पर्चा,
कोई गुप्त शक्ति
हृदय में करने-सी लगती है चर्चा !!
मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ उसको !
आश्चर्य!
उसमें तो मेरे ही गुप्त विचार व
दबी हुई संवेदनाएँ व अनुभव
पीड़ाएँ जगमगा रही हैं।
यह सब क्या है !!
आसमान झाँकता है लकीरों के बीच-बीच
वाक्यों की पाँतों में आकाशगंगा-फैली
शब्दों के व्यूहों में ताराएँ चमकीं
तारक-दलों में भी खिलता है आँगन
जिसमें कि चंपा के फूल चमकते
शब्दाकाशों के कानों में गहरे तुलसी श्यामल खिलते हैं
चेहरे !!
चमकता है आशय मनोज्ञ मुखों से
पारिजात-पुष्प महकते।
पर्चा पढ़ते हुए उड़ता हूँ हवा में,
चक्रवात-गतियों में घूमता हूँ नभ पर,
जमीन पर एक साथ
सर्वत्र सचेत उपस्थित।
प्रत्येक स्थान पर लगा हूँ मैं काम में,
प्रत्येक चौराहे, दुराहे व राहों के मोड़ पर
सड़क पर खड़ा हूँ,
मानता हूँ, मानता हूँ, मनवाता अड़ा हूँ !!
और तब दिक्काल-दूरियाँ
अपने ही देश के नक्शे-सी टँगी हुई
रँगी हुई लगतीं !!
स्वप्नों की कोमल किरनें कि मानो
घनीभूत संघनित द्युतिमान
शिलाओं में परिणत
ये दृढ़ीभूत कर्म-शिलाएँ हैं
जिनसे की स्वप्नों की मूर्ति बनेगी
सस्मित सुखकर
जिसकी कि किरनें,
ब्रह्मांड-भर में नापेंगी सब कुछ!
सचमुच, मुझको तो जिंदगी-सरहद
सूर्यों के प्रांगण पार भी जाती-सी दीखती !!
मैं परिणत हूँ,
कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूँ
वर्तमान समाज चल नहीं सकता।
पूँजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता,
स्वातंत्र्य व्यक्ति का वादी
छल नहीं सकता मुक्ति के मन को,
जन को।
8
एकाएक हृदय धड़ककर रुक गया, क्या हुआ !!
नगर से भयानक धुआँ उठ रहा है,
कहीं आग लग गयी, कहीं गोली चल गयी।
सड़कों पर मरा हुआ फैला है सुनसान,
हवाओं में अदृश्य ज्वाला की गरमी
गरमी का आवेग।
साथ-साथ घूमते हैं, साथ-साथ रहते हैं,
साथ-साथ सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं,
जन-मन उद्देश्य !!
पथरीले चेहरों के खाकी ये कसे ड्रेस
घूमते हैं यंत्रवत्,
वे पहचाने-से लगते हैं वाकई
कहीं आग लग गयी, कहीं गोली चल गयी !!
सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक्
चिंतक, शिल्पकार, नर्तक चुप हैं
उनके खयाल से यह सब गप है
मात्र किंवदंती।
रक्तपायी वर्ग से नाभिनाल-बद्ध ये सब लोग
नपुंसक भोग-शिरा-जालों में उलझे।
प्रश्न की उथली-सी पहचान
राह से अनजान
वाक् रुदंती।
चढ़ गया उर पर कहीं कोई निर्दयी,
कहीं आग लग गयी, कहीं गोली चल गयी।
भव्याकार भवनों के विवरों में छिप गये
समाचारपत्रों के पतियों के मुख स्थूल।
गढ़े जाते संवाद,
गढ़ी जाती समीक्षा,
गढ़ी जाती टिप्पणी जन-मन-उर-शूर।
बौद्धिक वर्ग है क्रीतदास,
किराये के विचारों का उद्भास।
बड़े-बड़े चेहरों पर स्याहियाँ पुत गयीं।
नपुंसक श्रद्धा
सड़क के नीचे की गटर में छिप गयी,
कहीं आग लग गयी, कहीं गोली चल गयी।
धुएँ के जहरीले मेघों के नीचे ही हर बार
द्रुत निज-विश्लेष-गतियाँ,
एक स्प्लिट सेकेंड में शत साक्षात्कार।
टूटते हैं धोखों से भरे हुए सपने।
रक्त में बहती हैं शान की किरनें
विश्व की मूर्ति में आत्मा ही ढल गयी,
कहीं आग लग गयी, कहीं गोली चल गयी।
राह के पत्थर-ढोकों के अंदर
पहाड़ों के झरने
तड़पने लग गये।
मिट्टी के लोंदे के भीतर
भक्ति की अग्नि का उद्रेक
भड़कने लग गया।
धूल के कण में
अनहद नाद का कंपन
खतरनाक !!
मकानों के छत से
गाडर कूद पड़े धम से।
घूम उठे खंभे
भयानक वेग से चल पड़े हवा में।
दादा का सोंटा भी करता दाँव-पेंच
नाचता है हवा में
गगन में नाच रही कक्का की लाठी।
यहाँ तक कि बच्चे की पेंपें भी उड़तीं,
तेजी से लहराती घूमती है हवा में
सलेट पट्टी।
एक-एक वस्तु या एक-एक प्राणाग्नि-बम है,
ये परमास्त्र हैं, प्रक्षेपास्त्र हैं, यम हैं।
शून्याकाश में से होते हुए वे
अरे, अरि पर ही टूट पड़े अनिवार।
यह कथा नहीं है, यह सब सच है, हाँ भई !!
कहीं आग लग गयी, कहीं गोली चल गयी !!
किसी एक बलवान् तन-श्याम लुहार ने बनाया
कंडों का वर्तुल ज्वलंत मंडल।
स्वर्णिम कमलों की पाँखुरी-जैसी ही
ज्वालाएँ उठती हैं उससे,
और उस गोल-गोल ज्वलंत रेखा में रक्खा
लोहे का चक्का
चिनगियाँ स्वर्णिम नीली व लाल
फूलों-सी खिलतीं। कुछ बलवान् जन साँवले मुख के
चढ़ा रहे लकड़ी के चक्के पर जबरन
लाल-लाल लोहे की गोल-गोल पट्टी
घन मार घन मार,
उसी प्रकार अब
आत्मा के चक्के पर चढ़ाया जा रहा
संकल्प शक्ति के लोहे का मजबूत
ज्वलंत टायर !!
अब युग बदल गया है वाकई,
कहीं आग लग गयी, कहीं गोली चल गयी।
गेरुआ मौसम उड़ते हैं अंगार,
जंगल जल रहे जिंदगी के अब
जिनके कि ज्वलंत-प्रकाशित भीषण
फूलों में बहतीं वेदना नदियाँ
जिनके कि जल में
सचेत होकर सैकड़ों सदियाँ, ज्वलंत अपने
बिंब फेंकतीं !!
वेदना नदियाँ
जिनमें कि डूबे हैं युगानुयुग से
मानो कि आँसू
पिताओं की चिंता का उद्विग्न रंग भी,
विवेक-पीड़ा की गहराई बेचैन,
डूबा है जिनमें श्रमिक का संताप।
वह जल पीकर
मेरे युवकों में होता जाता व्यक्तित्वांतर,
विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह से करते हैं संगर,
मानो कि ज्वाला-पंखुरियों से घिरे हुए वे सब
अग्नि के शत-दल-कोष में बैठे !!
द्रुत-वेग बहती हैं शक्तियाँ निश्चयी।
कहीं आग लग गयी, कहीं गोली चल गयी।
X X X
एकाएक फिर स्वप्न भंग
बिखर गये चित्र कि मैं फिर अकेला।
मस्तिष्क हृदय में छेद पड़ गये हैं।
पर उन दुखते हुए रंध्रों में गहरा
प्रदीप्त ज्योति का रस बस गया है।
मैं उन सपनों का खोजता हूँ आशय,
अर्थों की वेदना घिरती है मन में।
अजीब झमेला।
घूमता है मन उन अर्थों के घावों के आस-पास
आत्मा में चमकीली प्यास भर गयी है।
जग भर दीखती हैं सुनहली तस्वीरें मुझको
मानो कि कल रात किसी अनपेक्षित क्षण में ही सहसा
प्रेम कर लिया हो
जीवन भर के लिए !!
मानो कि उस क्षण
अतिशय मृदु किन्ही बाँहों ने आकर
कस लिया था इस भाँति कि मुझको
उस स्वप्न-स्पर्श की, चुंबन की याद आ रही है,
याद आ रही है !!
अज्ञात प्रणयिनी कौन थी, कौन थी?
कमरे में सुबह की धूप आ गयी है,
गैलरी में फैला है सुनहला रवि छोर
क्या कोई प्रेमिका सचमुच मिलेगी?
हाय ! यह वेदना स्नेह की गहरी
जाग गयी क्यों कर ?
सब ओर विद्युत्तरंगीय हलचल
चुंबकीय आकर्षण।
प्रत्येक वस्तु का निज-निज आलोक,
मानो कि अलग-अलग फूलों के रंगीन
अलग-अलग वातावरण हैं बेमाप,
प्रत्येक अर्थ की छाया में अन्य अर्थ
झलकता साफ-साफ !
डेस्क पर रखे हुए महान् ग्रंथों के लेखक
मेरी इन मानसिक क्रियाओं के बन गये प्रेक्षक,
मेरे इस कमरे में आकाश उतरा,
मन यह अंतरिक्ष-वायु में सिहरा।
उठता हूँ, जाता हूँ, गैलरी में खड़ा हूँ।
एकाएक वह व्यक्ति
आँखों के सामने
गलियों में, सड़कों पर, लोगों की भीड़ में
चला जा रहा है।
वही जन जिसे मैंने देखा था गुहा में।
धड़कता है दिल
कि पुकारने को खुलता है मुँह
कि अकस्मात् –
वह दिखा, वह दिखा
वह फिर खो गया किसी जन यूथ में…
उठी हुई बाँह यह उठी रह गयी !!
अनखोजी निज-समृद्धि का वह परम उत्कर्ष,
परम अभिव्यक्ति
मैं उसका शिष्य हूँ
वह मेरी गुरु है,
गुरु है !!
वह मेरे पास कभी बैठा ही नहीं था,
वह मेरे पास कभी आया ही नहीं था,
तिलस्मी खोह में देखा था एक बार,
आखिरी बार ही।
पर, वह जगत् की गलियों में घूमता है प्रतिपल
वह फटेहाल रूप।
तडित्तरंगीय वही गतिमयता,
अत्यंत उद्विग्न ज्ञान-तनाव वह
सकर्मक प्रेम की वह अतिशयता
वही फटेहाल रूप !!
परम अभिव्यक्ति
लगातार घूमती है जग में
पता नहीं जाने कहाँ, जाने कहाँ
वह है।
इसीलिए मैं हर गली में
और हर सड़क पर
झाँक-झाँक देखता हूँ हर एक चेहरा,
प्रत्येक गतिविधि
प्रत्येक चरित्र,
व हर एक आत्मा का इतिहास,
हर एक देश व राजनैतिक परिस्थिति
प्रत्येक मानवीय स्वानुभूत आदर्श
विवेक-प्रक्रिया, क्रियागत परिणति !!
खोजता हूँ पठार… पहाड़… समुंदर
जहाँ मिल सके मुझे
मेरी वह खोयी हुई
परम अभिव्यक्ति अनिवार
आत्म-संभवा।
ब्रम्हराक्षस
शहर के उस ओर खंडहर की तरफ
परित्यक्त सूनी बावड़ी
के भीतरी
ठंडे अँधेरे में
बसी गहराइयाँ जल की…
सीढ़ियाँ डूबी अनेकों
उस पुराने घिरे पानी में…
समझ में आ न सकता हो
कि जैसे बात का आधार
लेकिन बात गहरी हो।
बावड़ी को घेर
डालें खूब उलझी हैं,
खड़े हैं मौन औदुंबर।
व शाखों पर
लटकते घुग्घुओं के घोंसले
परित्यक्त भूरे गोल।
विद्युत शत पुण्य का आभास
जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर
हवा में तैर
बनता है गहन संदेह
अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि
दिल में एक खटके सी लगी रहती।
बावड़ी की इन मुँडेरों पर
मनोहर हरी कुहनी टेक
बैठी है टगर
ले पुष्प तारे-श्वेत
उसके पास
लाल फूलों का लहकता झौंर –
मेरी वह कन्हेर…
वह बुलाती एक खतरे की तरफ जिस ओर
अंधियारा खुला मुँह बावड़ी का
शून्य अंबर ताकता है।
बावड़ी की उन गहराइयों में शून्य
ब्रह्मराक्षस एक पैठा है,
व भीतर से उमड़ती गूँज की भी गूँज,
हड़बड़ाहट शब्द पागल से।
गहन अनुमानिता
तन की मलिनता
दूर करने के लिए प्रतिपल
पाप छाया दूर करने के लिए, दिन-रात
स्वच्छ करने –
ब्रह्मराक्षस
घिस रहा है देह
हाथ के पंजे बराबर,
बाँह-छाती-मुँह छपाछप
खूब करते साफ,
फिर भी मैल
फिर भी मैल!!
और… होठों से
अनोखा स्तोत्र कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार,
अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार,
मस्तक की लकीरें
बुन रहीं
आलोचनाओं के चमकते तार !!
उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह…
प्राण में संवेदना है स्याह!!
किंतु, गहरी बावड़ी
की भीतरी दीवार पर
तिरछी गिरी रवि-रश्मि
के उड़ते हुए परमाणु, जब
तल तक पहुँचते हैं कभी
तब ब्रह्मराक्षस समझता है, सूर्य ने
झुककर नमस्ते कर दिया।
पथ भूलकर जब चाँदनी
की किरन टकराए
कहीं दीवार पर,
तब ब्रह्मराक्षस समझता है
वंदना की चाँदनी ने
ज्ञान-गुरु माना उसे।
अति प्रफुल्लित कंटकित तन-मन वही
करता रहा अनुभव कि नभ ने भी
विनत हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी!!
और तब दुगुने भयानक ओज से
पहचान वाला मन
सुमेरी-बेबिलोनी जन-कथाओं से
मधुर वैदिक ऋचाओं तक
व तब से आज तक के सूत्र
छंदस्, मंत्र, थियोरम,
सब प्रेमियों तक
कि मार्क्स, एंजेल्स, रसेल, टॉएन्बी
कि हीडेग्गर व स्पेंग्लर, सार्त्र, गांधी भी
सभी के सिद्ध-अंतों का
नया व्याख्यान करता वह
नहाता ब्रह्मराक्षस, श्याम
प्राक्तन बावड़ी की
उन घनी गहराइयों में शून्य।
…ये गरजती, गूँजती, आंदोलिता
गहराइयों से उठ रही ध्वनियाँ, अतः
उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में
हर शब्द निज प्रति शब्द को भी काटता,
वह रूप अपने बिंब से भी जूझ
विकृताकार-कृति
है बन रहा
ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से यहाँ
बावड़ी की इन मुँडेरों पर
मनोहर हरी कुहनी टेक सुनते हैं
टगर के पुष्प-तारे श्वेत
वे ध्वनियाँ!
सुनते हैं करोंदों के सुकोमल फूल
सुनता है उन्हे प्राचीन ओदुंबर
सुन रहा हूँ मैं वही
पागल प्रतीकों में कही जाती हुई
वह ट्रेजिडी
जो बावड़ी में अड़ गई।
x x x
खूब ऊँचा एक जीना साँवला
उसकी अँधेरी सीढ़ियाँ…
वे एक आभ्यंतर निराले लोक की।
एक चढ़ना औ’ उतरना,
पुनः चढ़ना औ’ लुढ़कना,
मोच पैरों में
व छाती पर अनेकों घाव।
बुरे-अच्छे-बीच के संघर्ष
से भी उग्रतर
अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संगर
गहन किंचित सफलता,
अति भव्य असफलता
…अतिरेकवादी पूर्णता
की ये व्यथाएँ बहुत प्यारी हैं…
ज्यामितिक संगति-गणित
की दृष्टि के कृत
भव्य नैतिक मान
आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान…
…अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना
कब रहा आसान
मानवी अंतर्कथाएँ बहुत प्यारी हैं!!
रवि निकलता
लाल चिंता की रुधिर-सरिता
प्रवाहित कर दीवारों पर,
उदित होता चंद्र
व्रण पर बाँध देता
श्वेत-धौली पट्टियाँ
उद्विग्न भालों पर
सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए
अनगिन दशमलव से
दशमलव-बिंदुओं के सर्वतः
पसरे हुए उलझे गणित मैदान में
मारा गया, वह काम आया,
और वह पसरा पड़ा है…
वक्ष-बाँहें खुली फैलीं
एक शोधक की।
व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रासाद-सा,
प्रासाद में जीना
व जीने की अकेली सीढ़ियाँ
चढ़ना बहुत मुश्किल रहा।
वे भाव-संगत तर्क-संगत
कार्य सामंजस्य-योजित
समीकरणों के गणित की सीढ़ियाँ
हम छोड़ दें उसके लिए।
उस भाव तर्क व कार्य-सामंजस्य-योजन-शोध में
सब पंडितों, सब चिंतकों के पास
वह गुरु प्राप्त करने के लिए
भटका!!
किंतु युग बदला व आया कीर्ति-व्यवसायी
…लाभकारी कार्य में से धन,
व धन में से हृदय-मन,
और, धन-अभिभूत अंतःकरण में से
सत्य की झाईं
निरंतर चिलचिलाती थी।
आत्मचेतस् किंतु इस
व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन…
विश्वचेतस् बे-बनाव!!
महत्ता के चरण में था
विषादाकुल मन!
मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन यदि
तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर
बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य
उसकी महत्ता!
व उस महत्ता का
हम सरीखों के लिए उपयोग,
उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व!!
पिस गया वह भीतरी
औ’ बाहरी दो कठिन पाटों बीच,
ऐसी ट्रेजिडी है नीच!!
बावड़ी में वह स्वयं
पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा
वह कोठरी में किस तरह
अपना गणित करता रहा
औ’ मर गया…
वह सघन झाड़ी के कँटीले
तम-विवर में
मरे पक्षी-सा
विदा ही हो गया
वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई
यह क्यों हुआ !
क्यों यह हुआ !!
मैं ब्रह्मराक्षस का सजल-उर शिष्य
होना चाहता
जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य,
उसकी वेदना का स्रोत
संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक
पहुँचा सकूँ।
एक स्वप्न कथा
एक विजय और एक पराजय के बीच
मेरी शुद्ध प्रकृति
मेरा ‘स्व’
जगमगाता रहता है
विचित्र उथल-पुथल में।
मेरी साँझ, मेरी रात
सुबहें व मेरे दिन
नहाते हैं, नहाते ही रहते हैं
सियाह समुंदर के अथाह पानी में
उठते-गिरते हुए दिगवकाश-जल में।
विक्षोभित हिल्लोलित लहरों में
मेरा मन नहाता रहता है
साँवले पल में।
फिर भी, फिसलते से किनारे को पकड़कर मैं
बाहर निकलने की, रह-रहकर तड़पती कोशिश में
कौंध-कौंध उठता हूँ;
इस कोने, उस कोने
चकाचौंध-किरनें वे नाचतीं
सामने बगल में।
मेरी ही भाँति कहीं इसी समुंदर की
सियाह लहरों में नंगी नहाती हैं।
किरनीली मूर्तियाँ –
मेरी ही स्फूर्तियाँ
निथरते पानी की काली लकीरों के
कारण, कटी-पिटी अजीब-सी शकल में।
उनके मुखारविंद
मुझे डराते हैं,
इतने कठोर हैं कि कांतिमान पत्थर हैं
क्वार्ट्ज शिलाएँ हैं
जिनमें से छन-छनकर
नील किरण-मालाएँ
कोण बदलती हैं।
एक नया पहलू रोज
सामने आता है प्रश्नों के पल-पल में
2
सागर तट पथरीला
किसी अन्य ग्रह-तल के विलक्षण स्थानों को
अपार्थिव आकृति-सा
इस मिनिट, उस सेकेंड
चमचमा उठता है,
जब-जब वे स्फूर्ति-मुख मुझे देख
तमतमा उठते हैं
काली उन लहरों को पकड़कर अंजलि में
जब-जब मैं देखना चाहता हूँ –
क्या हैं वे? कहाँ से आई हैं?
किस तरह निकली हैं
उद्गम क्या, स्रोत क्या,
उनका इतिहास क्या?
काले समुंदर की व्याख्या क्या, भाष्य क्या?
कि इतने में, इतने में
झलक-झलक उठती हैं
जल-अंतर में से ही कठोर मुख आकृतियाँ
भयावने चेहरे कुछ, लहरों के नीचे से,
चिलक-चिलक उठते हैं,
मुझको अड़ाते हैं,
बहावदार गुस्से में भौंहें चढ़ाते हैं।
पहचान में आते-से, जान नहीं पाता हूँ,
शनाख्त न कर सकता।
खयाल यह आता है –
शायद है,
सागर की थाहों में महाद्वीप डूबे हों
रहती हैं उनमें ये मनुष्य आकृतिया
मुस्करा, लहरों में, उभरती रहती हैं।
थरथरा उठता हूँ!
सियाह वीरानी में लहराता आर-पार
सागर यह कौन है?
3
जाने क्यों, काँप-सिहरते हुए,
एक भयद
अपवित्रता की हद
ढूँढ़ने लगता हूँ कि इतने में
एक अनहद गान
निनादित सर्वतः
झूलता रहता है,
ऊँचा उठ, नीचे गिर
पुनः क्षीण, पुनः तीव्र
इस कोने, उस कोने, दूर-दूर
चारों ओर गूँजता रहता है।
आर-पार सागर के श्यामल प्रसारों पर
अपार्थिव पक्षिणियाँ
अनवरत गाती हैं –
चीखती रहती हैं
जमाने की गहरी शिकायतें
खूँरेज किस्सों से निकले नतीजे और
सुनाती रहती हैं
कोई तब कहता है –
पक्षिणियाँ सचमुच अपार्थिव हैं
कल जो अनैसर्गिक
अमानवीय दिखता था
आज वही स्वाभाविक लगता है,
निश्चित है कल वही अपार्थिव दीखेंगे।
इसीलिए, उसको आज अप्राकृत मान लो।
सियाह समुंदर के वे पाँखी उड़-उड़कर
कंधों पर, शीश पर
इस तरह मँडराकर बैठते
कि मानो मैं सहचर हूँ उनका भी,
कि मैंने भी, दुखात्मक आलोचन –
– किरनों के रक्त-मणि
हृदय में रक्खे हैं।
पक्षिणियाँ कहती है –
सहस्रों वर्षों से यह सागर
उफनता आया है
उसका तुम भाष्य करो
उसका व्याख्यान करो
चाहो तो उसमें तुम डूब मरो।
अतल निरीक्षण को,
मरकर तुम पूर्ण करो।
4
मुझसे जो छूट गए अपने वे
स्फूर्ति-मुख निहारता बैठा हूँ,
उनका आदेश क्या,
क्या करूँ?
रह-रहकर यह खयाल आता है –
ज्ञानी एक पूर्वज ने
किसी रात, नदी का पानी काट,
मन्त्र पढ़ते हुए,
गहन जल-धारा में
गोता लगाया था कि
अंधकार जल-तल का स्पर्श कर
इधर ढूँढ़, उधर खोज
एक स्निग्ध, गोल-गोल
मनोहर तेजस्वी शिलाखंड
तमोमय जल में से सहज निकला था;
देव बना, पूजा की।
उसी तरह संभव है –
सियाह समुंदर के
अतल-तले पड़ा हुआ
किरणीला एक दीप्त
प्रस्तर – युगानुयुग
तिमिर-श्याम सागर के विरुद्ध निज आभा की
महत्वपूर्ण सत्ता का
प्रतिनिधित्व करता हो, आज भी।
संभव है, वह पत्थऱ
मेरा ही नहीं वरन्
पूरे ब्रह्माण्ड की
केंद्र-क्रियाओं का तेजस्वी अंश हो।
संभव है,
सभी कुछ दिखता हो उसमें से,
दूर-दूर देशों में क्या हुआ,
क्यों हुआ, किस तरह, कहाँ हुआ,
इतने में कोई आ कानों में कहता है –
ऐसा यह ज्ञान-मणि
मरने से मिलता है;
जीवन के जंगल में
अनुभव के नए-नए गिरियों के ढालों पर
वेदना-झरने के,
पहली बार देखे-से, जल-तल में
आत्मा मिलती है
(कहीं-कहीं, कभी-कभी)
अरे, राह-गलियों में
पड़ा नहीं मिलता है ज्ञान-मणि।
हाय रे!
मेरे ही स्फूर्ति-मुख
मेरा ही अनादर करते हैं,
तिरस्कार करते हैं,
अविश्वास करते हैं!
मुझे देख तमतमा उठते हैं।
क्रोधारुण उनका मुख-मंडल देखकर लगता है,
छिड़ने ही वाली है युग-व्यापी एक बहस
उभरने वाली है बेहद जद्दोजहद?
बहुत बड़ा परिवर्तन
सघन वातावरण होने ही वाला है;
जिसके ये घनीभूत
अंधकार-पूर्ण शत
पूर्व-क्षण
महान अपेक्षा से यों तड़प उठते हैं
कि मेरे ही अंतःस्थित संवेदन
मुझ पर ही
झूम, बरस, गरज, कड़क उठते हैं।
उनका वार
बिलकुल मुझी पर है;
बिजली का हर्फ
सिर्फ मुझ पर गिर
तहस-नहस करता है;
बहुत बहस करता है
5
मेरे प्रति उन्मुख हो स्फूर्तियाँ
कहती हैं –
तुम क्या हो?
पहचान न पाईं, सच!
क्या कहना! तुम्हारी आत्मा का
सौंदर्य अनिर्वच,
प्राण हैं प्रस्तर-त्वच।
मारकर ठहाका, वे मुझे हिला देती हैं
सोई हुई अग्नियाँ
उँगली से हिला-डुला
पुनः जिला देती हैं।
मुझे वे दुनिया की
किसी दवाई में डाल
गला देती हैं!!
उनके बोल हैं कि पत्थर की बारिश है
बहुत पुराने किसी
अन-चुकाए कर्ज की
खतरनाक नालिश है
फिर भी है रास्ता, रिआयत है,
मेरी मुरव्वत है।
क्षितिज के कोने पर गरजते जाने किस
तेज आँधी-नुमा गहरे हवाले से
बोलते जाते हैं स्फूर्ति-मुख।
देख यों हम सबको
चमचमा मंगल-ग्रह साक्षी बन जाता है
पृथ्वी के रत्न-विवर में से निकली हुई
बलवती जलधारा
नव-नवीन मणि-समूह
बहाती लिए जाय,
और उस स्थिति में, रत्न-मंडल की तीव्र दीप्ति
आग लगाय लहरों में
उसी तरह, स्फूर्तिमय भाषा-प्रवाह में
जगमगा उठते हैं भिन्न-भिन्न मर्म-केंद्र।
सत्य-वचन,
स्वप्न-दृग् कवियों के तेजस्वी उद्धरण,
संभावी युद्धों के भव्य-क्षण-आलोडन,
विराट चित्रों में
भविष्य – आस्फालन
जगमगा उठता है।
और तब हा-हा खा
दुनिया का अँधेरा रोता है।
ठहाका – आगामी देवों का।
काले समुंदर की अंधकार-जल-त्वचा
थरथरा उठती है!!
बंद करने की कोशिश होती है तो
मन का यह दरवाजा
करकरा उठता है;
विरोध में, खुल जाता धड्ड से
उसका सुदूर तक गूँजता धड़ाका
अँधेरी रातों में।
स्फूर्तियाँ
कहती हैं कि
मैं जो पुत्र उनका हूँ
अब नहीं पहचान में आता हूँ;
लौट विदेशों से
अपने ही घर पर मैं इस तरह नवीन हूँ
इतना अधिक मौलिक हूँ –
असल नहीं!!
मन में जो बात एक कराहती रहती है
उसकी तुष्टि करने का
साहस, संकल्प और बल नहीं।
मुझको वे स्फूर्ति-मुख
इस तरह देखते कि
मानो अजीब हूँ;
उन्हें छोड़ कष्टों में
उन्हें त्याग दुख की खोहों में
कहीं दूर निकल गया
कि मैं जो बहा किया
आंतरिक आरोहावरोहों में,
निर्णायक मुहूर्त जो कि
घपले में टल गया,
कि मैं ही क्यों इस तरह बदल गया!
इसीलिए, मेरी ये कविताएँ
भयानक हिडिंबा हैं,
वास्तव की विस्फारित प्रतिमाएँ
विकृताकृति-बिंबा हैं।
6
मुझे जेल देती हैं
दुश्मन हैं स्फूर्तियाँ
गुस्से में ढकेल ही देती हैं।
भयानक समुंदर के बीचोंबीच फेंक दिया जाता हूँ।
अपना सब वर्तमान, भूत भविष्य स्वाहा कर
पृथ्वी-रहित, नभ रहित होकर मैं
वीरान जलती हुई अकेली धड़कन…
सहसा पछाड़ खा
चारों ओर फैले उस भयानक समुद्र की
(काले संगमूसा-सी चिकनी व चमकदार)
सतहों पर छटपटा गिरता हूँ
कि माथे पर चोट जो लगती है
लहरें चूस लेती हैं रक्त को,
तैरने लगते-से हैं रुधिर के रेशे ये।
इतने में खयाल आता है कि
समुद्र के अतल तले
लुप्त महाद्वीपों में पहाड़ भी होंगे ही
उनकी जल खोहों तक जाना ही होगा अब।
भागती लहरों के कंधों के साथ-साथ
आगे कुछ बढ़ता हूँ कि
नाभि-नाल छूता हूँ अकस्मात्।
मृणाल, हाँ मृणाल
जल खोहों से ऊपर उठ
लहरों के ऊपर चढ़
बनकर वृहद् एक
काला सहस्र-दल सम्मुख उपस्थित है,
उसमें हैं कृष्ण रक्त।
गोता लगाऊँ और
नाभि-नाल-रेखा की समांतर राह से
नीचे जल-खोह तक पहुँचूँ तो
संभव है सागर का मूल सत्य
मुझे मिल जायगा।
अंधी जल-खोहों में
क्यों न हम घूमें और
सर्वेक्षण क्यों न करें
फिरें-तिरें।
चाहें तो दुर्घटनाघात से
बूढ़ी विकराल व्हेल-पंजर की काँख में फँसें-मरें।
इतने में, भुजाएँ ये व्यग्र हो
पानी को काटती उदग्र हो।
अचानक खयाल यह आता है कि
काले संगमूसा-सी भयानक लहरों के
कई मील नीचे एक
वृहद नगर
भव्य…
सागर के तिमिर-तले।
निराकार तमाकार पानी की
कई मील मोटी जो लगातार सतहें हैं
जहाँ मुझे जाना है।
इसीलिए, मुझे इस तमाकार पानी से
समझौता करना है
तैरते रहना सीमाहीन काल तक
मुझको तो मृत्यु तक
भयानक लहरों से मित्रता रखना है।
इतने में, हाय-हाय
सागर की जल-त्वचा थरथरा उठती है,
लहरों के दाँत दीख पड़ते हैं पीसते,
दल पर दल लहरें हैं कि
तर्कों की बहती हुई पंक्तियाँ, दिगवकाश-संबंधी थियोरम या
ऊर्ध्वोन्मुख भावों की अधःपतित
उठती निसैनियाँ !!
और,ये लहरें जिस सीमा तक दौड़तीं
जहाँ जिस सीमा पर खो-सी जाती हैं
वहीं, हाँ,
पीली और भूरी-सी धुंध है गीली सी
मद्धिम उजाले को मटमैला बादली परदा-सा
कि जिसके प्रसार पर
जुलूस चल पड़ते हैं
दिक्काल
7
स्तब्ध हूँ
विचित्र दृश्य
फुसफुसे पहाड़ों-सी पुरुषों की आकृतियाँ
भुसभुसे टीलों-सी नारी प्रकृतियाँ
ऊँचा उठाए सिर गरबीली चाल से
सरकती जाती हैं
चेहरों के चौखटे
अलग-अलग तरह के – अजीब हैं
मुश्किल है जानना;
पर, कई
निज के स्वयं के ही
पहचानवालों का भान हो आता है।
आसमान असीम, अछोरपन भूल,
तंग गुंबज, फिर,
क्रमशः संक्षिप्त हो
मात्र एक अँधेरी खोह बन जाता है।
और, मैं मन ही मन, टिप्पणी करता हूँ कि
हो न हो
कई मील मोटी जल-परतों के
नीचे ढँका हुआ शहर जो डूबा है
उसके सौ कमरों में
हलचलें गहरी हैं
कि उनकी कुछ झाइयाँ
ऊपर आ सिहरी हैं
सिहरती उभरी हैं…
साफ-साफ दीखतीं।
अकस्मात् मुझे ज्ञान होता है
कि मैं ही नहीं वरन्
अन्य अनेक जन
दुखों के द्रोहपूर्ण
शिखरों पर चढ़ करके
देखते
विराट उन दृश्यों को
कि ऐसा ही एक देव भयानक आकार का
अनंत चिंता से ग्रस्त हो
विद्रोही समीक्षण-सर्वेक्षण करता है
विराट् उन चित्रों का।
जुलूस में अनेक मुख
(नेता और विक्रेता, अफसर और कलाकार)
अनगिन चरित्र
पर, चरितव्य कहीं नहीं
अनगिनत श्रेष्ठों की रूप-आकृतियाँ
रिक्त प्रकृतियाँ
मात्र महत्ता की निराकार केवलता।
उस कृष्ण सागर की ऊँची तरंगों में,
उठता गिरता हुआ मेरा मन
अपनी दृष्टि-रेखाएँ प्रक्षेपित करता है
इतने में दीखता कि
सागर की थाहों में पैर टिका देता है पर्वत-आकार का
देव भयानक
उठ खड़ा होता है।
सागर का पानी सिर्फ उसके घुटनों तक है,
पर्वत-सा मुख-मंडल आसमान छूता है
अनगिनत ग्रह-तारे चमक रहे, कंधों पर।
लटक रहा एक ओर
चाँद
कंदील-सा।
मद्धिम प्रकाश-रहस्य
जिसमें, दूर, वहाँ, एक फैला-सा
चट्टानी चेहरा स्याह
नाजुक और सख्त (पर, धुँधला वह)
कहता वह –
… … …
कितनी ही गर्वमयी
सभ्यता-संस्कृतियाँ
डूब गईं।
काँपा है, थहरा है,
काल-जल गहरा है,
शोषण की अतिमात्रा,
स्वार्थों की सुख-यात्रा,
जब-जब संपन्न हुई
आत्मा से अर्थ गया, मर गई सभ्यता।
भीतर की मोरियाँ अकस्मात् खुल गईं।
जल की सतह मलिन
ऊँची होती गई,
अंदर सूराख से
अपने उस पाप से
शहरों के टॉवर सब मीनारें डूब गईं,
काला समुंदर ही लहराया, लहराया!
भयानक थर-थर है!! ग्लानिकर सागर में
मुझे गश आता है
विलक्षण स्पर्शों की अपरिचित पीड़ा में
परिप्रेक्ष्य गहरा हो,
तिमिर-दृश्य आता है
ठनकती रहती हैं,
आभ्यंतर ग्रंथियाँ, बहिःसमस्याएँ।
इतने अकस्मात् मुझे दीख पड़ता है
काले समुंदर के बीच चट्टानों पर
सूनी हवाओं को सूँघ रहा
फूटा हुआ बुर्ज या
रोशनी-मीनार
बुझी हुई –
पुर्तगीज, ओलंदेज, फिरंगी लुटेरों के
हाथों सधी हुई।
उस पर चढ़ अँधियारा
जाने क्या गाता है,
मुझको डराता है!! खयाल यह आता है कि
हो न हो
इस काले सागर का
सुदूर-स्थित पश्चिम-किनारे से
जरूर कुछ नाता है
इसीलिए, हमारे पास सुख नहीं आता है।
इतने मे अकस्मात् तैरता आता-सा
समुद्री अँधेरे में
जगमगाते अनगिनत तारों का उपनिवेश।
विविध रूप दीपों को अनगिनत पाँतों का
रहस्य-दृश्य!! सागर में प्रकाश-द्वीप तैरता!!
जहाज हाँ जहाज सर्च-लाइट फेंक घनीभूत अँधेरे में दूर-दूर
उछलती लहरों पर जाने क्या ढूँढ़ता।
सागर तरंगों पर भयानक लट्ठे-सा
डूबता उतराता दिखाई देता हूँ कि
चमकती चादर एक तेज फैल जाती है
मेरे सब अंगों पर।
एक हाथ आता है मेरे हाथ!!
वह जहाज
क्षोभ विद्रोह-भरे संगठित विरोध का
साहसी समाज है!! भीतर व बाहर के पूरे दलिद्दर से
मुक्ति की तलाश में
आगामी कल नहीं, आगत वह आज है!!
बेचैन चील
बेचैन चील!!
उस जैसा मैं पर्यटनशील
प्यासा-प्यासा,
देखता रहूँगा एक दमकती हुई झील
या पानी का कोरा झाँसा
जिसकी सफ़ेद चिलचिलाहटों में है अजीब
इनकार एक सूना!!
मैं तुम लोगों से इतना दूर हूँ
मैं तुम लोगों से इतना दूर हूँ
तुम्हारी प्रेरणाओं से मेरी प्रेरणा इतनी भिन्न है
कि जो तुम्हारे लिए विष है, मेरे लिए अन्न है।
मेरी असंग स्थिति में चलता-फिरता साथ है,
अकेले में साहचर्य का हाथ है,
उनका जो तुम्हारे द्वारा गर्हित हैं
किन्तु वे मेरी व्याकुल आत्मा में बिम्बित हैं, पुरस्कृत हैं
इसीलिए, तुम्हारा मुझ पर सतत आघात है !!
सबके सामने और अकेले में।
( मेरे रक्त-भरे महाकाव्यों के पन्ने उड़ते हैं
तुम्हारे-हमारे इस सारे झमेले में )
असफलता का धूल-कचरा ओढ़े हूँ
इसलिए कि वह चक्करदार ज़ीनों पर मिलती है
छल-छद्म धन की
किन्तु मैं सीधी-सादी पटरी-पटरी दौड़ा हूँ
जीवन की।
फिर भी मैं अपनी सार्थकता से खिन्न हूँ
विष से अप्रसन्न हूँ
इसलिए कि जो है उससे बेहतर चाहिए
पूरी दुनिया साफ़ करन के लिए मेहतर चाहिए
वह मेहतर मैं हो नहीं पाता
पर , रोज़ कोई भीतर चिल्लाता है
कि कोई काम बुरा नहीं
बशर्ते कि आदमी खरा हो
फिर भी मैं उस ओर अपने को ढो नहीं पाता।
रिफ्रिजरेटरों, विटैमिनों, रेडियोग्रेमों के बाहर की
गतियों की दुनिया में
मेरी वह भूखी बच्ची मुनिया है शून्यों में
पेटों की आँतों में न्यूनों की पीड़ा है
छाती के कोषों में रहितों की व्रीड़ा है
शून्यों से घिरी हुई पीड़ा ही सत्य है
शेष सब अवास्तव अयथार्थ मिथ्या है भ्रम है
सत्य केवल एक जो कि
दुःखों का क्रम है
मैं कनफटा हूँ हेठा हूँ
शेव्रलेट-डॉज के नीचे मैं लेटा हूँ
तेलिया लिबास में पुरज़े सुधारता हूँ
तुम्हारी आज्ञाएँ ढोता हूँ।
जब दुपहरी ज़िन्दगी पर
जब दुपहरी ज़िन्दगी पर रोज़ सूरज
एक जॉबर-सा
बराबर रौब अपना गाँठता-सा है
कि रोज़ी छूटने का डर हमें
फटकारता-सा काम दिन का बाँटता-सा है
अचानक ही हमें बेखौफ़ करती तब
हमारी भूख की मुस्तैद आँखें ही
थका-सा दिल बहादुर रहनुमाई
पास पा के भी
बुझा-सा ही रहा इस ज़िन्दगी के कारख़ाने में
उभरता भी रहा पर बैठता भी तो रहा
बेरुह इस काले ज़माने में
जब दुपहरी ज़िन्दगी को रोज़ सूरज
जिन्न-सा पीछे पड़ा
रोज़ की इस राह पर
यों सुबह-शाम ख़याल आते हैं…
आगाह करते से हमें… ?
या बेराह करते से हमें ?
यह सुबह की धूल सुबह के इरादों-सी
सुनहली होकर हवा में ख़्वाब लहराती
सिफ़त-से ज़िन्दगी में नई इज़्ज़त, आब लहराती
दिलों के गुम्बजों में
बन्द बासी हवाओं के बादलों को दूर करती-सी
सुबह की राह के केसरिया
गली का मुँह अचानक चूमती-सी है
कि पैरों में हमारे नई मस्ती झूमती-सी है
सुबह की राह पर हम सीखचों को भूल इठलाते
चले जाते मिलों में मदरसों में
फ़तह पाने के लिए
क्या फ़तह के ये ख़याल ख़याल हैं
क्या सिर्फ धोखा है ?…
सवाल है।
(संभावित रचनाकाल 1948-50, अप्रकाशित)
कल और आज
अभी कल तक गालियाँ
देते थे तुम्हें
हताश खेतिहर,
अभी कल तक
धूल में नहाते थे
गौरैयों के झुंड,
अभी कल तक
पथराई हुई थी
धनहर खेतों की माटी,
अभी कल तक
दुबके पड़े थे मेंढक,
उदास बदतंग था आसमान !
और आज
ऊपर ही ऊपर तन गये हैं
तुम्हारे तंबू,
और आज
छमका रही है पावस रानी
बूंदा बूंदियों की अपनी पायल,
और आज
चालू हो गई है
झींगुरों की शहनाई अविराम,
और आज
जोर से कूक पड़े
नाचते थिरकते मोर,
और आज
आ गई वापस जान
दूब की झुलसी शिराओं के अंदर,
और आज
विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म
समेट कर अपने लाव-लश्कर ।
मैं उनका ही होता
मैं उनका ही होता जिनसे
मैंने रूप भाव पाए हैं।
वे मेरे ही हिये बंधे हैं
जो मर्यादाएँ लाए हैं।
मेरे शब्द, भाव उनके हैं
मेरे पैर और पथ मेरा,
मेरा अंत और अथ मेरा,
ऐसे किंतु चाव उनके हैं।
मैं ऊँचा होता चलता हूँ
उनके ओछेपन से गिर-गिर,
उनके छिछलेपन से खुद-खुद,
मैं गहरा होता चलता हूँ।
लकड़ी का रावण
दीखता
त्रिकोण इस पर्वत-शिखर से
अनाम, अरूप और अनाकार
असीम एक कुहरा,
भस्मीला अन्धकार
फैला है कटे-पिटे पहाड़ी प्रसारों पर;
लटकती हैं मटमैली
ऊँची-ऊँची लहरें
मैदानों पर सभी ओर
लेकिन उस कुहरे से बहुत दूर
ऊपर उठ
पर्वतीय ऊर्ध्वमुखी नोक एक
मुक्त और समुत्तुंग !!
उस शैल-शिखर पर
खड़ा हुआ दीखता है एक द्योः पिता भव्य
निःसंग
ध्यान-मग्न ब्रह्म…
मैं ही वह विराट् पुरुष हूँ
सर्व-तन्त्र, स्वतन्त्र, सत्-चित् !
मेरे इन अनाकार कन्धों पर विराजमान
खड़ा है सुनील
शून्य
रवि-चन्द्र-तारा-द्युति-मण्डलों के परे तक ।
दोनों हम
अर्थात्
मैं व शून्य
देख रहे…दूर…दूर…दूर तक
फैला हुआ
मटमैली जड़ीभूत परतों का
लहरीला कम्बल ओर-छोर-हीन
रहा ढाँक
कन्दरा-गुहाओं को, तालों को
वृक्षों के मैदानी दृश्यों के प्रसार को
अकस्मात्
दोनों हम
मैं वह शून्य
देखते कि कम्बल की कुहरीली लहरें
हिल रही, मुड़ रही !!
क्या यह सच,
कम्बल के भीतर है कोई जो
करवट बदलता-सा लग रहा ?
आन्दोलन ?
नहीं, नहीं मेरी ही आँखों का भ्रम है
फिर भी उस आर-पार फैले हुए
कुहरे में लहरीला असंयम !!
हाय ! हाय !
क्या है यह !! मेरी ही गहरी उसाँस में
कौन-सा है नया भाव ?
क्रमशः
कुहरे की लहरीली सलवटें
मुड़ रही, जुड़ रही,
आपस में गुँथ रही !!
क्या है यह !!
यर क्या मज़ाक है,
अरूर अनाम इस
कुहरे की लहरों से अगनित
कइ आकृति-रूप
बन रहे, बनते-से दीखते !!
कुहरीले भाफ भरे चहरे
अशंक, असंख्य व उग्र…
अजीब है,
अजीबोगरीब है
घटना का मोड़ यह ।
अचानक
भीतर के अपने से गिरा कुछ,
खसा कुछ,
नसें ढीली पड़ रही
कमज़ोरी बढ़ रही; सहसा
आतंकित हम सब
अभी तक
समुत्तुंग शिखरों पर रहकर
सुरक्षित हम थे
जीवन की प्रकाशित कीर्ति के क्रम थे,
अहं-हुंकृति के ही…यम-नियम थे,
अब क्या हुआ यह
दुःसह !!
सामने हमारे
घनीभूत कुहरे के लक्ष-मुख
लक्ष-वक्ष, शत-लक्ष-बाहु ये रूप, अरे
लगते हैं घोरतर ।
जी नहीं,
वे सिर्फ कुहरा ही नहीं है,
काले-काले पत्थर
व काले-काले लोहे के लगते वे लोग ।
हाय, हाय, कुहरे की घनीभूत प्रतिमा या
भरमाया मेरा मन,
उनके वे स्थूल हाथ
मनमाने बलशाली
लगते हैं ख़तरनाक;
जाने-पहचाने-से लगते हैं मुख वे ।
डरता हूँ,
उनमें से कोई, हाय
सहसा न चढ़ जाय
उत्तुंग शिखर की सर्वोच्च स्थिति पर,
पत्थर व लोहे के रंग का यह कुहरा !
बढ़ न जायँ
छा न जायँ
मेरी इस अद्वितीय
सत्ता के शिखरों पर स्वर्णाभ,
हमला न कर बैठे ख़तरनाक
कुहरे के जनतन्त्री
वानर ये, नर ये !!
समुदाय, भीड़
डार्क मासेज़ ये मॉब हैं,
हलचलें गड़बड़,
नीचे थे तब तक
फ़ासलों में खोये हुए कहीं दूर, पार थे;
कुहरे के घने-घने श्याम प्रसार थे ।
अब यह लंगूर हैं
हाय हाय
शिखरस्थ मुझको ये छू न जायँ !!
आसमानी शमशीरी, बिजलियों,
मेरी इन भुजाओं में बन जाओ
ब्रह्म-शक्ति !
पुच्छल ताराओं,
टूट पड़ो बरसो
कुहरे के रंग वाले वानरों के चहरे
विकृत, असभ्य और भ्रष्ट हैं…
प्रहार करो उन पर,
कर डालो संहार !!
अरे, अरे !
नभचुम्बी शिखरों पर हमारे
बढ़ते ही जा रहे
जा रहे चढ़ते
हाय, हाय,
सब ओर से घिरा हूँ ।
सब तरफ़ अकेला,
शिखर पर खड़ा हूँ ।
लक्ष-मुख दानव-सा, लक्ष-हस्त देव सा ।
परन्तु, यह क्या
आत्म-प्रतीति भी धोखा ही दे रही !!
स्वयं को ही लगता हूँ
बाँस के व कागज़ के पुट्ठे के बने हुए
महाकाय रावण-सा हास्यप्रद
भयंकर !!
हाय, हाय,
उग्रतर हो रहा चेहरों का समुदाय
और कि भाग नहीं पाता मैं
हिल नहीं पाता हूँ
मैं मन्त्र-कीलि-सा, भूमि में गड़ा-सा,
जड़ खड़ा हूँ
अब गिरा, तब गिरा
इसी पल कि उल पल…
रात, चलते हैं अकेले ही सितारे
रात, चलते हैं अकेले ही सितारे।
एक निर्जन रिक्त नाले के पास
मैंने एक स्थल को खोद
मिट्टी के हरे ढेले निकाले दूर
खोदा और
खोदा और
दोनों हाथ चलते जा रहे थे शक्ति से भरपूर।
सुनाई दे रहे थे स्वर –
बड़े अपस्वर
घृणित रात्रिचरों के क्रूर।
काले-से सुरों में बोलता, सुनसान था मैदान।
जलती थी हमारी लालटैन उदास,
एक निर्जन रिक्त नाले के पास।
खुद चुका बिस्तर बहुत गहरा
न देखा खोलकर चेहरा
कि जो अपने हृदय-सा
प्यार का टुकड़ा
हमारी ज़िंदगी का एक टुकड़ा,
प्राण का परिचय,
हमारी आँख-सा अपना
वही चेहरा ज़रा सिकुड़ा
पड़ा था पीत,
अपनी मृत्यु में अविभीत।
वह निर्जीव,
पर उस पर हमारे प्राण का अधिकार;
यहाँ भी मोह है अनिवार,
यहाँ भी स्नेह का अधिकार।
बिस्तर खूब गहरा खोद,
अपनी गोद से,
रक्खा उसे नरम धरती-गोद।
फिर मिट्टी,
कि फिर मिट्टी,
रखे फिर एक-दो पत्थर
उढ़ा दी मृत्तिका की साँवली चादर
हम चल पड़े
लेकिन बहुत ही फ़िक्र से फिरकर,
कि पीछे देखकर
मन कर लिया था शांत।
अपना धैर्य पृथ्वी के हृदय में रख दिया था।
धैर्य पृथ्वी का हृदय में रख लिया था।
उतनी भूमि है चिरंतन अधिकार मेरा,
जिसकी गोद में मैंने सुलाया प्यार मेरा।
आगे लालटैन उदास,
पीछे, दो हमारे पास साथी।
केवल पैर की ध्वनि के सहारे
राह चलती जा रही थी।
मृत्यु और कवि
घनी रात, बादल रिमझिम हैं, दिशा मूक, निस्तब्ध वनंतर
व्यापक अंधकार में सिकुड़ी सोयी नर की बस्ती भयकर
है निस्तब्ध गगन, रोती-सी सरिता-धार चली गहराती,
जीवन-लीला को समाप्त कर मरण-सेज पर है कोई नर
बहुत संकुचित छोटा घर है, दीपालोकित फिर भी धुंधला,
वधू मूर्छिता, पिता अर्ध-मृत, दुखिता माता स्पंदन-हीन
घनी रात, बादल रिमझिम हैं, दिशा मूक, कवि का मन गीला
“ये सब क्षनिक, क्षनिक जीवन है, मानव जीवन है क्षण-भंगुर” ।
ऐसा मत कह मेरे कवि, इस क्षण संवेदन से हो आतुर
जीवन चिंतन में निर्णय पर अकस्मात मत आ, ओ निर्मल !
इस वीभत्स प्रसंग में रहो तुम अत्यंत स्वतंत्र निराकुल
भ्रष्ट ना होने दो युग-युग की सतत साधना महाआराधना
इस क्षण-भर के दुख-भार से, रहो अविचिलित, रहो अचंचल
अंतरदीपक के प्रकाश में विणत-प्रणत आत्मस्य रहो तुम
जीवन के इस गहन अटल के लिये मृत्यु का अर्थ कहो तुम ।
क्षण-भंगुरता के इस क्षण में जीवन की गति, जीवन का स्वर
दो सौ वर्ष आयु होती तो क्या अधिक सुखी होता नर?
इसी अमर धारा के आगे बहने के हित ये सब नश्वर,
सृजनशील जीवन के स्वर में गाओ मरण-गीत तुम सुंदर
तुम कवि हो, यह फैल चले मृदु गीत निर्बल मानव के घर-घर
ज्योतित हों मुख नवम आशा से, जीवन की गति, जीवन का स्वर ।